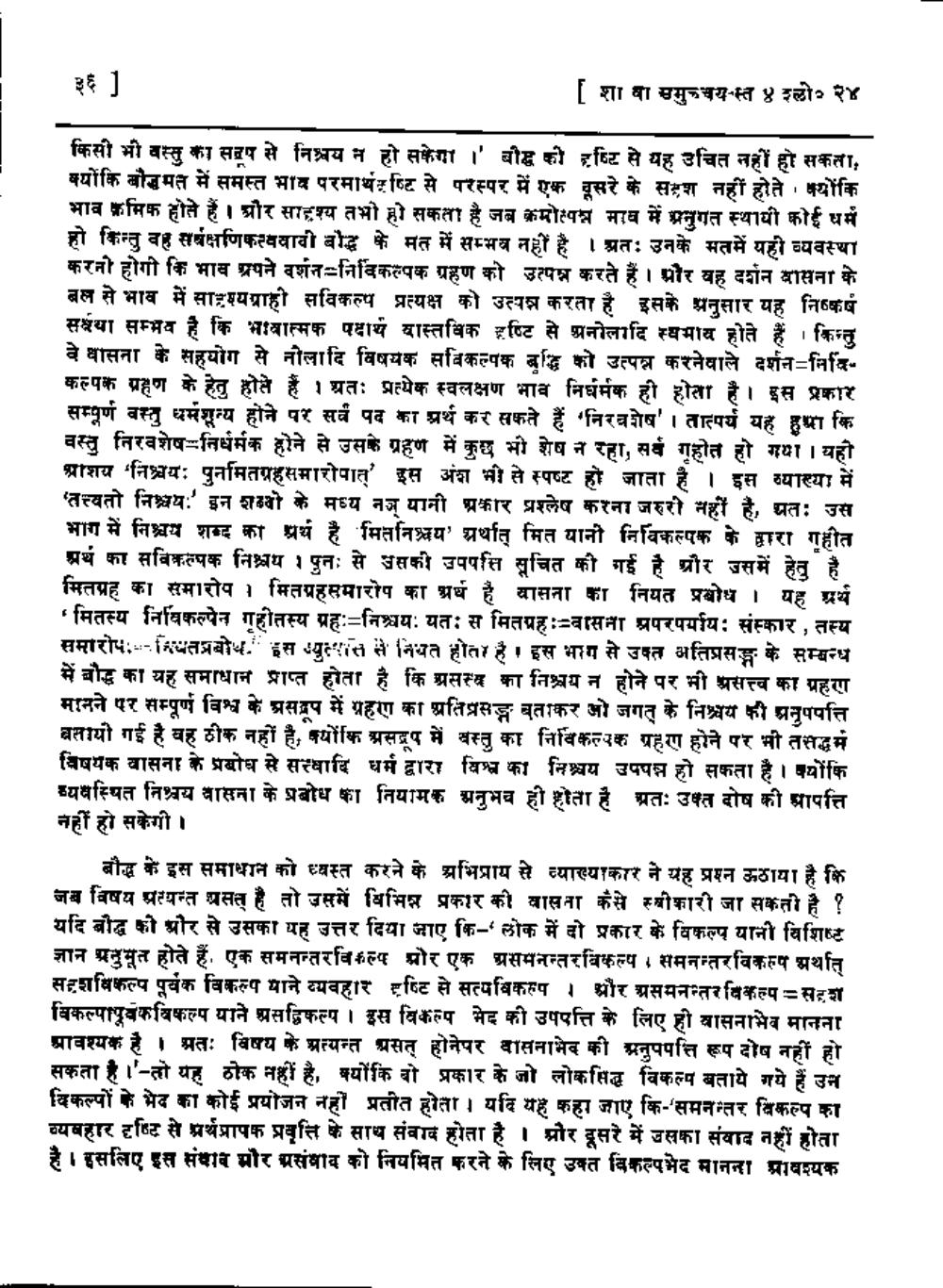________________
[ शा वा समुच्चय-स्त ४ श्लो० २४
किसी भी वस्तु का सत्य से निश्चय न हो सकेगा ।' बौद्ध की दृष्टि से यह उचित नहीं हो सकता, क्योंकि बौजमत में समस्त भाव परमार्थ ष्टि से परस्पर में एक दूसरे के सहश नहीं होते । क्योंकि भाव क्रमिक होते हैं । और सादृश्य तभी हो सकता है जब क्रमोत्पन्न माव में अनुगत स्थायी कोई धर्म हो किन्तु वह सर्वक्षणिकरववावी बौद्ध के मत में सम्भव नहीं है । अतः उनके मतमें यही व्यवस्था करनी होगी कि भाव अपने वर्शन-निर्विकल्पक ग्रहण को उत्पन्न करते हैं। और यह दर्शन वासना के बल से भाव में सादृश्यग्राही सविकल्प प्रत्यक्ष को उत्पन्न करता है इसके अनुसार यह निष्कर्ष सर्वया सम्भव है कि भावात्मक पदार्थ वास्तविक दृष्टि से अनोलादि स्वभाव होते हैं । किन्तु वे वासना के सहयोग से नौलादि विषयक सविकल्पक बुद्धि को उत्पन्न करनेवाले दर्शन निविकल्पक ग्रहण के हेतु होते हैं । अतः प्रत्येक स्वलक्षण भाव निर्मक ही होता है। इस प्रकार सम्पूर्ण वस्तु धर्मशून्य होने पर सर्व पद का अर्थ कर सकते हैं "निरवशेष' । तात्पर्य यह हुमा कि वस्तु निरवशेष-निर्धर्मक होने से उसके ग्रहण में कुछ भी शेष न रहा, सर्व गृहोत हो गया । यही प्राशय 'निश्चयः पुनमितग्रहसमारोपात्' इस अंश भी से स्पष्ट हो जाता है । इस व्याख्या में 'तत्त्वतो निश्चयः उन शब्दो के मध्य नजयानी प्रकार प्रश्लेष करना जरूरी नहीं है, अतः उस भाग में निश्चय शम्द का अर्थ है मितनिश्चय' अर्थात् मित यानी निर्विकल्पक के द्वारा गृहीत अर्थ का सविकल्पक निश्चय । पुनः से उसकी उपपत्ति सूचित की गई है और उसमें हेतु है मित्तग्रह का समारोप । मितग्रहसमारोप का अर्थ है वासना का नियत प्रबोध । यह प्रर्थ 'मितस्य निर्विकल्पेन गृहीतस्य ग्रहः निश्चयः यतः स मितग्रहः वासना अपरपर्याय: संस्कार , तस्य समारोप:--नियतप्रबोथ. इस प्युलात से नियत होता है। इस भाग से उक्त अतिप्रसन के सम्बन्ध में बौद्ध का यह समाधान प्राप्त होता है कि प्रसस्व का निश्चय न होने पर भी असत्त्व का ग्रहण मानने पर सम्पूर्ण विश्व के प्रसदप में ग्रहण का प्रतिप्रसङ्ग बताकर ओ जगत् के निश्चय की अनुपपत्ति बतायी गई है वह ठीक नहीं है, क्योंकि असद्रूप में वस्तु का निर्विकल्पक ग्रहण होने पर भी तसद्धर्म विषयक वासना के प्रबोध से सरवादि धर्म द्वारा विश्व का निश्चय उपपन्न हो सकता है। क्योंकि व्यवस्थित निश्चय वासना के प्रबोध का नियामक अनुभव ही होता है अतः उक्त दोष की प्रापत्ति नहीं हो सकेगी।
बौद्ध के इस समाधान को ध्वस्त करने के अभिप्राय से व्याख्याकार ने यह प्रश्न ऊठाया है कि जब विषय प्रत्यन्त असत् है तो उसमें विभिन्न प्रकार की वासना कैसे स्वीकारी जा सकती है ? यदि बौद्ध को और से उसका यह उत्तर दिया जाए कि-'लोक में दो प्रकार के विकल्प यानी विशिष्ट ज्ञान अनुमूत होते हैं, एक समनन्तरविकल्प प्रोर एक असमनन्तरविकल्प । समनन्तरविकरूप अर्थात् सदशविकल्प पूर्वक विकल्प याने व्यवहार दृष्टि से सत्यविकल्प । और असमनन्तर विकल्प सहश विकल्पापूर्वकविकल्प याने असद्विकल्प । इस विकल्प भेद की उपपत्ति के लिए ही वासनाभव मानना आवश्यक है । अतः विषय के अत्यन्त असत् होनेपर वासनाभेद की अनुपपत्ति रूप दोष नहीं हो सकता है।'-तो यह ठोक नहीं है, क्योंकि वो प्रकार के जो लोकसिद्ध विकल्प बताये गये हैं उन विकल्पों के भेद का कोई प्रयोजन नहीं प्रतीत होता। यदि यह कहा जाए कि-'समनन्तर विकल्प का व्यबहार दृष्टि से अर्थप्रापक प्रवृत्ति के साथ संवाद होता है । और दूसरे में उसका संवाद नहीं होता है। इसलिए इस संवाव भोर असंवाद को नियमित करने के लिए उक्त विकल्पभेद मानना प्रावश्यक