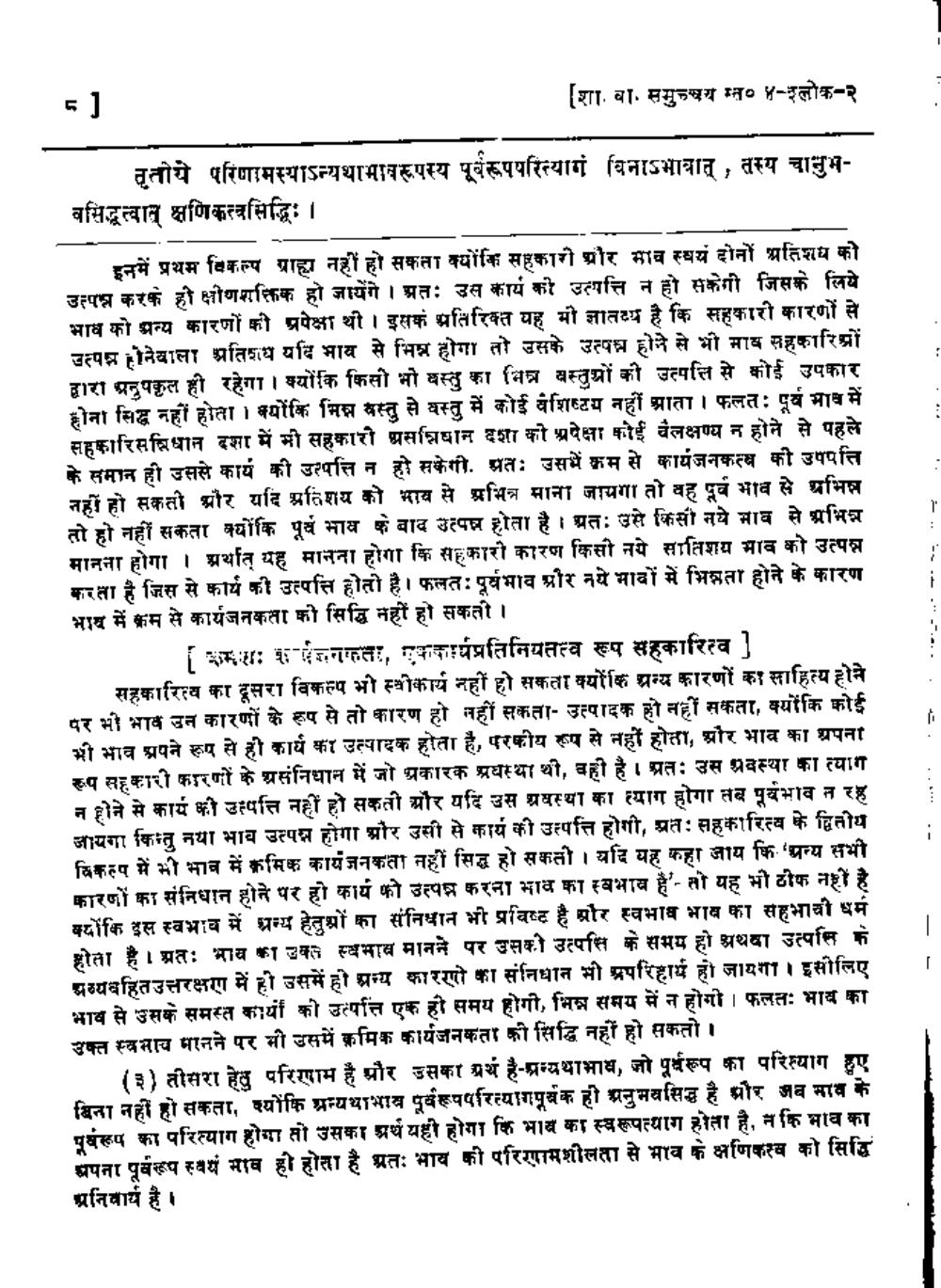________________
[शा. वा. समुच्चय म्न०४-श्लोक-२
तृतीये परिणामस्याऽन्यथामावरूपस्य पूर्वरूपपरित्यागं बिनाऽभावात् , तस्य चानुभवसिद्भूत्वात् क्षणिकत्वसिद्धिः ।
इनमें प्रथम विकल्प ग्राहा नहीं हो सकता क्योंकि सहकारी और माव स्वयं दोनों अतिशय को उत्पन्न करके ही क्षीणशक्तिक हो जायेंगे । अतः उस कार्य को उत्पत्ति न हो सकेगी जिसके लिये भाव को अन्य कारणों को प्रपेक्षा थी। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि सहकारी कारणों से उत्पन्न होनेवाला अतिशय यदि भाव से भिन्न होगा तो उसके उत्पन्न होने से भी माय सहकारियों द्वारा अनुपकृल ही रहेगा। क्योंकि किसी भी वस्तु का निन्न वस्तुओं की उत्पत्ति से कोई उपकार होना सिद्ध नहीं होता । क्योंकि मिन्न वस्तु से वस्तु में कोई वशिष्टय नहीं पाता। फलत: पूर्व भाव में सहकारिस निधान दशा में भी सहकारी असन्निधान दशा को अपेक्षा कोई वैलक्षण्य न होने से पहले के समान ही उससे कार्य की उत्पत्ति न हो सकेगी. प्रतः उसमें कम से कार्यजनकत्व की उपपत्ति नहीं हो सकती और यदि अतिशय को भाव से अभिन्न माना जायगा तो वह पूर्व भाव से अभिन्न तो हो नहीं सकता क्योंकि पूर्व भाव के बाद उत्पन्न होता है। अतः उसे किसी नये भाव से अभिन्न मानना होगा । अर्थात् यह मानना होगा कि सहकारी कारण किसी नये सातिशय भाव को उत्पन्न करता है जिस से कार्य की उत्पत्ति होती है। फलतः पूर्वभाव और नये भावों में भिन्नता होने के कारण भाव में क्रम से कार्यजनकता को सिद्धि नहीं हो सकती।
मिस कविगतता, एकाकार्यप्रतिनियतत्व रूप सहकारित्व] सहकारित्व का दूसरा विकल्प भी स्वीकार्य नहीं हो सकता क्योंकि अन्य कारणों का साहित्य होने पर भी भाव उन कारणों के रूप से तो कारण हो नहीं सकता- उत्पादक हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी भाव अपने रूप से ही कार्य का उत्पादक होता है, परकीय रूप से नहीं होता, और भाव का अपना रूप सहकारी कारणों के असंनिधान में जो प्रकारक अवस्था थी, वही है । अतः उस अवस्था का त्याग न होने से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती और यदि उस अवस्था का त्याग होगा तब पूर्वभाव न रह जायगा किन्तु नया भाव उत्पन्न होगा और उसी से कार्य की उत्पत्ति होगी, प्रतः सहकारित्व के द्वितीय विकल्प में भी भाव में क्रमिक कार्य जनकता नहीं सिद्ध हो सकती। यदि यह कहा जाय कि 'अन्य सभी कारणों का संनिधान होने पर हो कार्य को उत्पन्न करना भाव का स्वभाव है- तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि इस स्वभाव में अन्य हेतुत्रों का संनिधान भी प्रविष्ट है और स्वभाव भाव का सहभावी धर्म होता है। अतः भाव का उका स्वभाव मानने पर उसको उत्पत्ति के समय हो अथवा उत्पति के अव्यवहित उत्तरक्षण में ही उसमें ही अन्य कारणो का संनिधान भी अपरिहार्य हो जायगा। इसीलिए भाव से उसके समस्त कार्यों को उत्पत्ति एक ही समय होगी, भिन्न समय में न होगी। फलतः भाव का उक्त स्वभाव मानने पर भी उसमें क्रमिक कार्यजनकता की सिद्धि नहीं हो सकती।
(३) तीसरा हेतु परिणाम है और उसका अर्थ है-अन्यथाभाव, जो पूर्वरूप का परित्याग हुए बिना नहीं हो सकता, क्योंकि अन्यथाभाव पूर्वरूपपरित्यागपूर्वक ही अनुभवसिद्ध है और अब माव के पूर्वरूप का परित्याग होगा तो उसका अर्थ यही होगा कि भाव का स्वरूपत्याग होता है, न कि भाव का अपना पूर्वरूप स्वयं भाव ही होता है अतः भाव की परिणामशीलता से भाव के क्षणिकरव को सिद्धि अनिवार्य है।
।