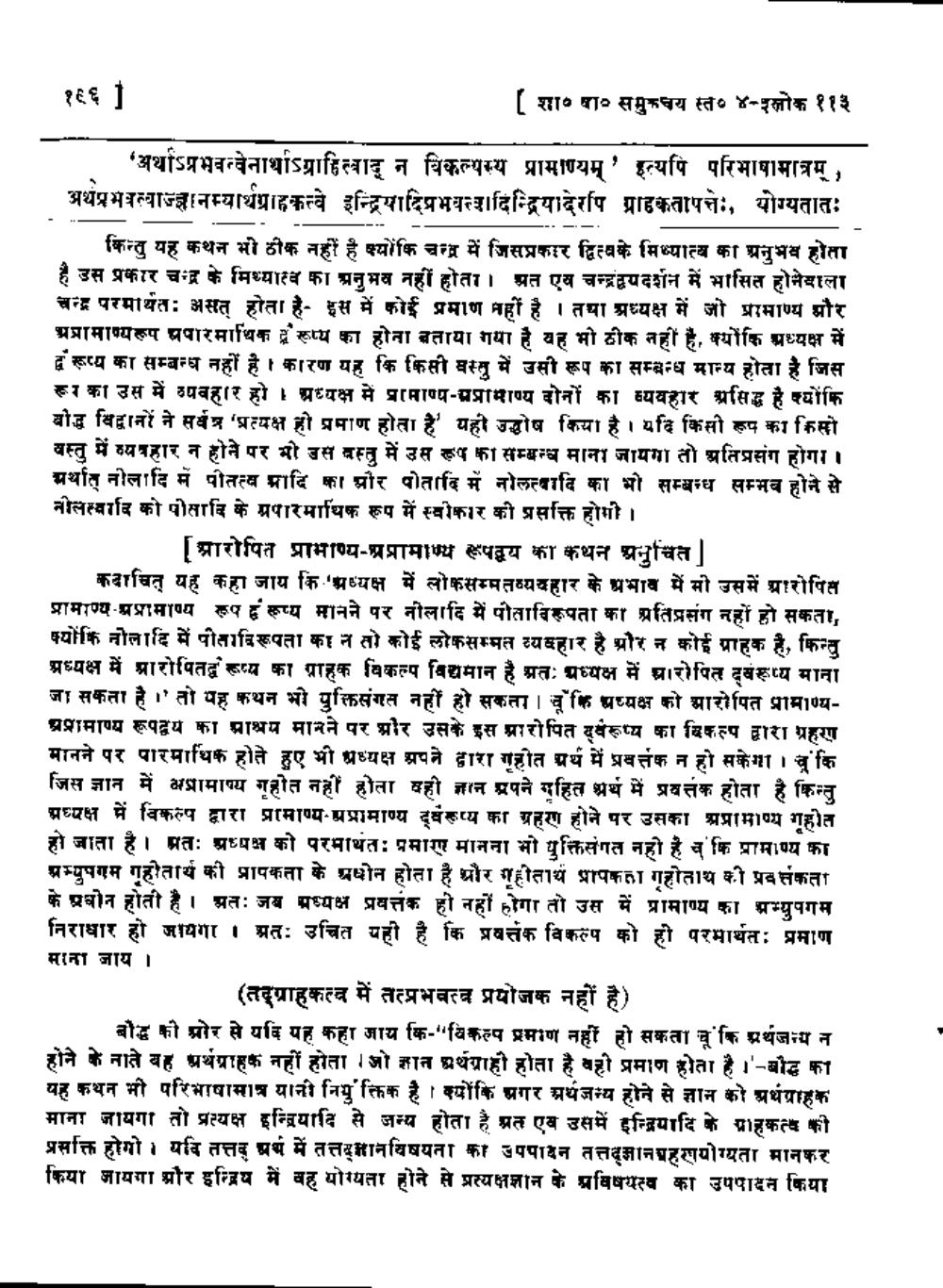________________
१६६ ]
[ शा.पा. समुरुषय स्त० ४-श्लोक ११३
___ 'अर्थाऽप्रभवत्वेनार्थाऽग्राहित्वाद् न विकल्पम्य प्रामाण्यम्' इत्यपि परिभाषामात्रम् , अर्थप्रभवल्याज्ञानम्यार्थग्राहकत्वे इन्द्रियादिप्रभवत्वादिन्द्रियादेपि ग्राहकतापत्तेः, योग्यतातः
किन्तु यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि चन्द्र में जिसप्रकार द्वित्वके मिथ्यात्व का अनुभव होता है उस प्रकार चन्द्र के मिथ्यात्व का अनमय नहीं होता। अत एव चन्द्रद्रयदर्शन में भासित होनेवाला चन्द्र परमार्थत: असत होता है. इस में कोई प्रमाण नहीं है । तथा अध्यक्ष में जो प्रामाण्य और अप्रामाण्यरूप अपारमाथिक रूप्य का होना बताया गया है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष में द्वं रूप्य का सम्बन्ध नहीं है। कारण यह कि किसी वस्तु में उसी रूप का सम्बन्ध मान्य होता है जिस रूर का उस में व्यवहार हो । अध्यक्ष में प्रामाण्य-प्रप्रामाण्य दोनों का व्यवहार प्रसिद्ध है क्योंकि बौद्ध विद्वानों ने सर्वत्र प्रत्यक्ष हो प्रमाण होता है यही उद्घोष किया है। यदि किसी रूप का किसो वस्तु में व्यवहार न होने पर भी उस वस्तु में उस रूप का सम्बन्ध माना जायगा तो अतिप्रसंग होगा। मर्थात् नीलादि में पीतत्व मादि का और पोतादि में नोलत्यादि का भी सम्बन्ध सम्भव होने से नीलस्वावि को पोसादि के अपारमाथिक रूप में स्वीकार की प्रसक्ति होगी।
[प्रारोपित प्रामाण्य-अप्रामाण्य रूपय का कथन अनुचित] कदाचित् यह कहा जाय कि अध्यक्ष में लोकसम्मतव्यवहार के प्रभाव में मी उसमें प्रारोपित प्रामाण्य-अप्रामाण्य रूप हंरूप्य मानने पर नीलादि में पोताविरूपता का प्रतिप्रसंग नहीं हो सकता, क्योंकि नोलादि में पीताविरूपता का न तो कोई लोकसम्मत व्यवहार है और न कोई ग्राहक है, किन्तु अध्यक्ष में प्रारोपितरूप्य का ग्राहक विकल्प विद्यमान है प्रतः अध्यक्ष में नारोक्ति दवरूप्य माना जा सकता है। तो यह कथन भी पक्तिसंगत नहीं हो सकता। किप्रध्यक्ष को आरोपित प्रामाण्यप्रामाण्य रूपद्वय का प्राश्रय मानने पर और उसके इस प्रारोपित स्वरूप्य का विकल्प द्वारा ग्रहरण मानने पर पारमार्थिक होते हुए भी अध्यक्ष अपने द्वारा गृहीत अर्थ में प्रवर्तक न हो सकेगा। चूंकि जिस ज्ञान में अप्रामाण्य गृहोत नहीं होता वही ज्ञान अपने माहित अर्थ में प्रवत्तंक होता है किन्तु अध्यक्ष में विकल्प द्वारा प्रामाण्य-प्रप्रामाण्य द्वरूप्य का ग्रहण होने पर उसका अप्रामाण्य गृहोत हो जाता है। प्रतः अध्यक्ष को परमार्थतः प्रमाण मानना भो युक्तिसंगत नहीं है कि प्रामाण्य का प्रभ्युपगम गहीतार्य की प्रापकता के अधीन होता है और महीतार्थ प्रापकता गहोताथ की प्रवर्तकता के प्रधान होती है। अतः जब अध्यक्ष प्रवत्तंक हो नहीं होगा तो उस में प्रामाण्य का अभ्युपगम निराधार हो जायगा । अतः उचित यही है कि प्रवत्तंक विकल्प को ही परमार्थतः प्रमाण माना जाय ।
(तद्ग्राहकत्व में तत्प्रभवत्व प्रयोजक नहीं है) बौद्ध को प्रोर से यदि यह कहा जाय कि-"विकल्प प्रमाण नहीं हो सकता कि प्रर्थजन्य न होने के नाते वह अर्थग्राहक नहीं होता । ओ ज्ञान प्रर्थनाही होता है वही प्रमाण होता है।'-बौद्ध का यह कथन भी परिभाषामात्र यानी नियुक्तिक है । क्योंकि अगर अर्थजन्य होने से ज्ञान को अथंग्राहक माना जायगा तो प्रत्यक्ष इन्द्रियादि से जन्य होता है प्रत एव उसमें इन्द्रियादि के ग्राहकत्व की प्रसक्ति होगी। यदि तत्तद् अर्थ में तत्तज्ञानविषयता का उपपादन तत्तझानग्रहणयोग्यता मानकर किया जायगा और इन्द्रिय में वह योग्यता होने से प्रत्यक्षज्ञान के प्रविषयत्व का उपपादन किया