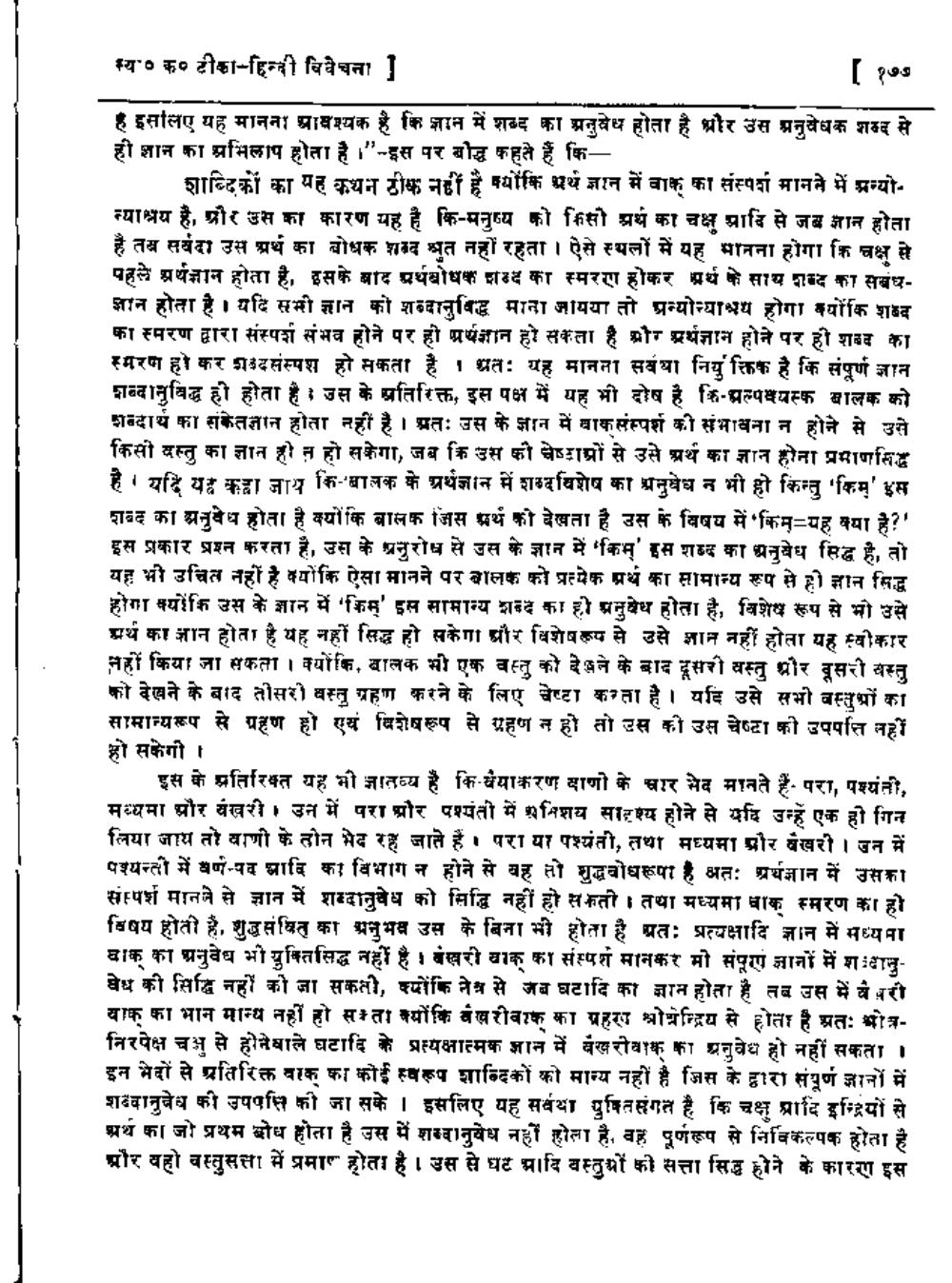________________
भ्यक० टीका-हिन्दी विवेचना ]
[ १७७ है इसलिए यह मानना प्रावश्यक है कि ज्ञान में शब्द का अनुवेध होता है और उस अनुवेधक शम्द से ही ज्ञान का प्रमिलाप होता है।"-इस पर बौद्ध कहते हैं कि
__ शाब्दिकों का यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि अर्थ ज्ञान में वाक का संस्पर्श मानने में अन्योन्याश्रय है, और उस का कारण यह है कि-मनुष्य को किसी प्रथं का चक्षु प्रादि से जब ज्ञान होता है तब सर्वदा उस अर्थ का बोधक शब्द श्रुत नहीं रहता। ऐसे स्थलों में यह मानना होगा कि चक्षु से पहले प्रर्थज्ञान होता है, इसके बाद प्रर्थबोधक शब्द का स्मरण होकर अर्थ के साय शब्द का सबंधज्ञान होता है। यदि समी ज्ञान को शब्दानुषिद्ध माना जायया तो प्रन्योन्याश्य होगा क्योंकि शब्द का स्मरण द्वारा संस्पर्श संभव होने पर ही अर्थज्ञान हो सकता है और प्रर्थज्ञान होने पर ही शब्द का स्मरण हो कर इद संस्पश हो सकता है । अत: यह मानना सर्वथा नियुक्तिक है कि संपूर्ण ज्ञान शब्दानुविद्ध ही होता है। उस के अतिरिक्त, इस पक्ष में यह भी दोष है कि-प्रल्पवयस्क बालक को शब्दार्थ का संकेतज्ञान होता नहीं है । प्रतः उस के ज्ञान में वाक संस्पर्श की संभावना न होने से उसे किसी वस्तु का ज्ञान हो न हो सकेगा, जब कि उस की चेष्टानों से उसे अर्थ का ज्ञान होना प्रमाणसिद्ध है । यदि यह कहा जाय कि-'बालक के अर्थज्ञान में शब्दविशेष का अनुषेध न भी हो किन्तु 'किम्' इस शब्द का अनुवेध होता है क्योंकि बालक जिस प्रर्थ को देखता है उस के विषय में किम्-यह क्या है?' इस प्रकार प्रश्न करता है, उस के अनुरोध से उस के ज्ञान में 'किम्' इस शब्द का अनुवेध सिद्ध है, तो यह भी उचित नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर बालक को प्रत्येक प्रथं का सामान्य रूप से हो ज्ञान सिद्ध होगा क्योंकि उस के ज्ञान में 'किम्' इस सामान्य शब्द का हो अनुवेध होता है, विशेष रूप से भी उसे मर्थ का ज्ञान होता है यह नहीं सिद्ध हो सकेगा और विशेष रूप से उसे ज्ञान नहीं होता यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि, बालक भी एक वस्तु को देखने के बाद दूसरी वस्तु और दूसरी वस्तु को देखने के बाद तीसरी वस्तु ग्रहण करने के लिए चेष्टा करता है। यदि उसे सभी वस्तुओं का सामान्यरूप से ग्रहण हो एवं विशेष रूप से ग्रहण न हो तो उस की उस चेष्टा को उपपत्ति नहीं हो सकेगी।
इस के प्रतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि-वैयाकरण दाणो के चार भेद मानते हैं. परा, पश्यंती, मध्यमा और यखरी। उन में परा प्रौर पश्यंती में शनिशय सादृश्य होने से यदि उन्हें एक ही गिन लिया जाय तो वाणी के तीन भेद रह जाते हैं। परा या पश्यंती, तथा मध्यमा और वैखरी । उन में पश्यन्ती में वर्ण-पद प्रादि का विभाग न होने से यह तो शुद्धबोधरूपा है अतः अर्थज्ञान में उसका सम्पर्श मानने से ज्ञान में शब्दानुवेष को सिद्धि नहीं हो सकती। तथा मध्यमा धाक स्मरण का हो विषय होती है, शुद्धसंचित का अनुभव उस के बिना भी होता है प्रतः प्रत्यक्षादि ज्ञान में मध्यमा वाक का अनुवेध भी युक्तिसिद्ध नहीं है। बखरी वाक् का संस्पर्श मानकर मो संपूर्ण ज्ञानों में शदानधेध की सिद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि नेत्र से जब घटादि का ज्ञान होता है तब उस में वैधरी वाक् का भान मान्य नहीं हो सकता क्योंकि बखरीवाक का ग्रहण श्रोग्रेन्द्रिय से होता है अतः भोत्रनिरपेक्ष चक्षु से होनेवाले घटादि के प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में बखरोवाक का अनुवेध हो नहीं सकता । इन भेदों से प्रतिरिक्त वाक का कोई स्वरूप शान्दिकों को मान्य नहीं है जिस के द्वारा संपूर्ण ज्ञानों में शब्वानुवेध की उपपत्ति की जा सके | इसलिए यह सर्वथा युक्तिसंगत है कि चक्षु प्रादि इन्द्रियों से अर्थ का जो प्रथम बोध होता है उस में शबानवेध नहीं होला है, वह पूर्ण रूप से निर्विकल्पक होता है और वहो वस्तुसत्ता में प्रमाण होता है । उस से घट प्रादि वस्तुओं को सत्ता सिद्ध होने के कारण इस