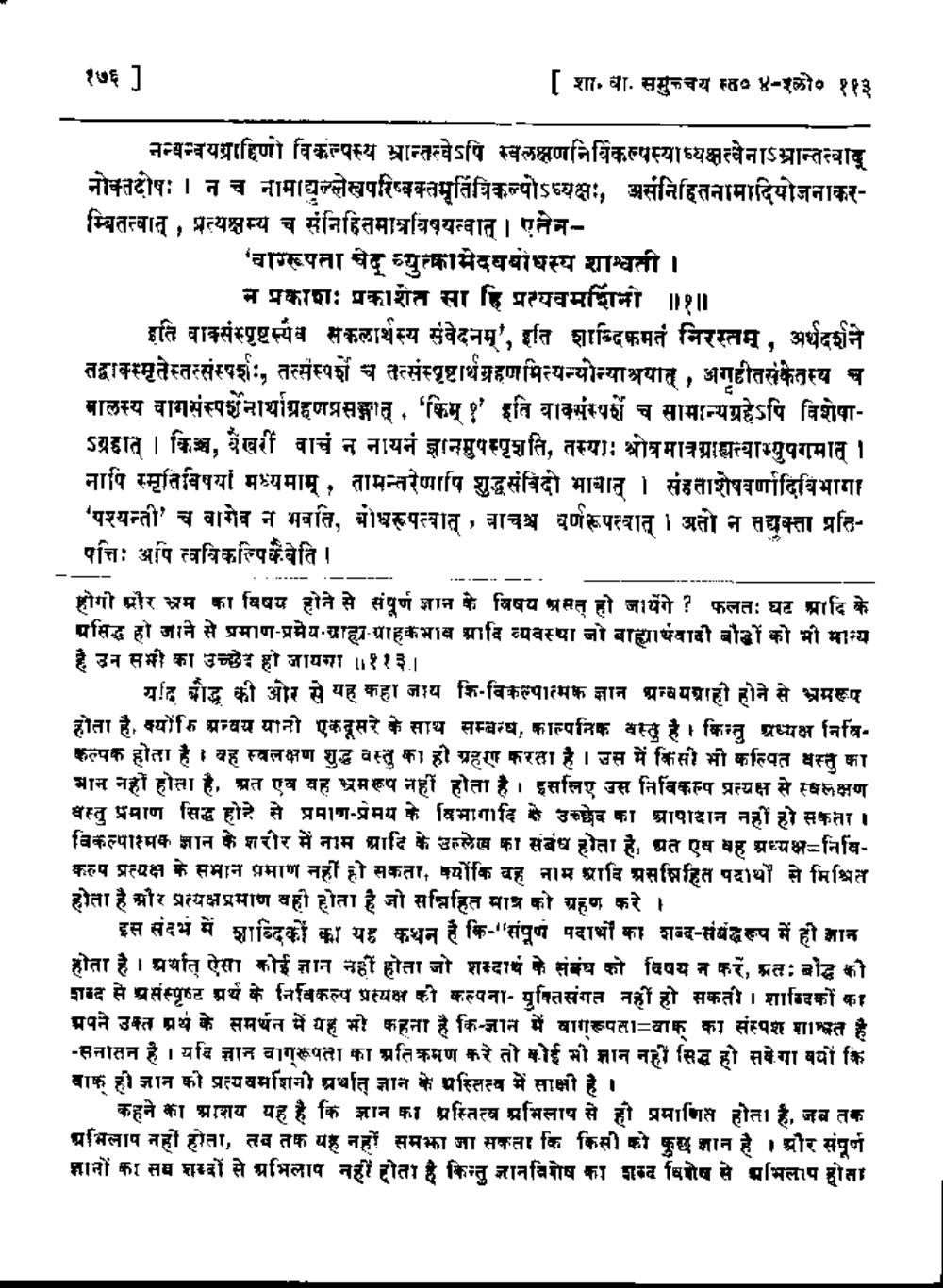________________
[ शा. वा. समुच्चय स्त० ४-श्लो० ११३
नन्यन्वयग्राहिणो विकल्पस्य भ्रान्तत्वेऽपि स्वलक्षणनिर्विकल्पस्याध्यक्षत्वेनाऽम्रान्तत्वाद् नोक्तदोषः । न च नामाद्युल्लेखपरिष्वक्तमूर्तिविकल्पोऽध्यक्षः, असंनिहितनामादियोजनाकरम्बितत्वात् , प्रत्यक्षम्य च संनिहितमात्रविषयत्वात् । एतेन
'वानरूपता घेदव्युत्कामेदवयोधस्य शाश्वती।
म प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनो ॥१॥ इति वासंस्पृष्टस्यैव सकलार्थस्य संवेदनम', इति शाब्दिकमतं निरस्तम् , अर्थदर्शने तद्वाक्स्मृतेस्तत्संस्पर्शः, तत्संस्पर्श च तत्संस्पृष्टार्थ ग्रहणमित्यन्योन्याश्रयात् , अगृहीतसंकेतस्य च पालस्य वागसंस्पर्शनार्थाग्रहणप्रसङ्गात् . 'किम् ?' इति वाक्मस्पर्श च सामान्यग्रहेऽपि विशेषाऽग्रहात् । किञ्च, खरी वाचं न नायनं ज्ञानमुपस्पृशति, तस्याः श्रोत्रमात्रायत्याभ्युपगमात् । नापि स्मृतिविषयां मध्यमाम् , तामन्तरेणापि शुद्धसंविदो भावान् । संहताशेषवर्णादिविभागा 'पश्यन्ती' च वागेव न भवति, बोधरूपत्वात् , बाचश्च वर्णरूपत्वात् । अतो न तक्ता प्रतिपत्तिः अपि त्वविकल्पिकैवेति । होगी और भ्रम का विषय होने से संपूर्ण ज्ञान के विषय असत् हो जायेंगे ? फलतः घट प्रादि के प्रसिद्ध हो जाने से प्रमाण-प्रमेय ग्राह्य ग्राहकभाव प्रादि व्यवस्था जो बाह्यार्थवादी बौद्धों को भी मान्य है उन सभी का उच्छेद हो जायगा ॥११३।।
यदि बौद्ध की ओर से यह कहा जाय कि-विकल्पात्मक ज्ञान अन्य यत्राही होने से भ्रमरूप होता है, क्योंकि अन्वय यानी एकदूसरे के साथ सम्बन्ध, काल्पनिक वस्तु है। किन्तु अध्यक्ष निविकल्पक होता है। यह स्वलक्षण शुद्ध वस्तु काही ग्रहण करता है । उस में किसी भी कल्पित वस्तु का भान नहीं होता है, अत एव वह भ्रमरूप नहीं होता है। इसलिए उस निर्विकल्प प्रत्यक्ष से स्थलक्षण वस्तु प्रमाण सिद्ध होने से प्रमाण-प्रेमय के विभागादि के उच्छेद का पापादान नहीं हो सकता। विकल्पास्मक ज्ञान के शरीर में नाम आदि के उल्लेख का संबंध होता है, प्रत एव बह अध्यक्ष-निविकल्प प्रत्यक्ष के समान प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वह नाम श्रादि प्रसन्निहित पदार्थों से मिश्रित होता है और प्रत्यक्षप्रमाण वही होता है जो सन्निहित मात्र को ग्रहण करे ।।
इस संदर्भ में शाब्दिकों का यह कथन है कि-"संपूर्ण पदार्थों का शब्द-संबंद्धरूप में ही शान होता है । अर्थात् ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता जो शम्दार्थ के संबंध को विषय न करें, अत: बौद्ध की शम्द से प्रसंस्पृष्ट अर्थ के निर्विकल्प प्रत्यक्ष की कल्पना- युक्तिसंगत नहीं हो सकती । शाग्रिकों का अपने उक्त प्रथ के समर्थन में यह भी कहना है कि-ज्ञान में वागरूपसा वाक् का संस्पश शाश्वत है -सनासन है । यदि ज्ञान बागरूपता का अतिक्रमण करे तो कोई भी शान नहीं सिद्ध हो सकेगा क्यों कि वाफ ही ज्ञान की प्रत्यवर्माशनी अर्थात् ज्ञान के अस्तित्व में साक्षी है।
कहने का प्राशय यह है कि ज्ञान का अस्तित्व प्रमिलाप से हो प्रमाणित होता है, जब तक अभिलाप नहीं होता, तब तक यह नहीं समझा जा सकता कि किसी को कुछ शान है । और संपूर्ण जानों का सब शम्बों से अभिलाप नहीं होता है किन्तु ज्ञानवियोष का शम्द विशोष से अभिलाप होता