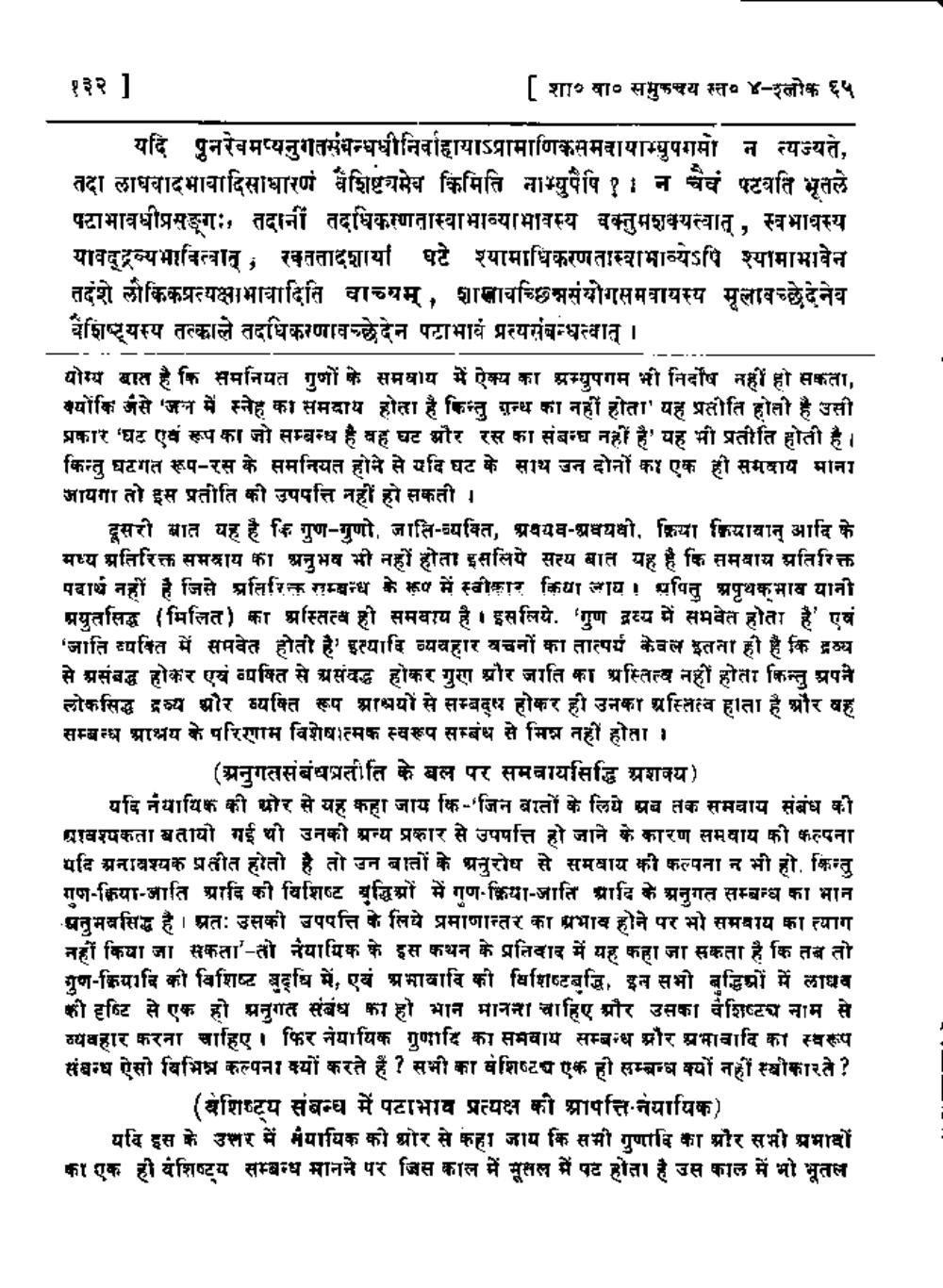________________
१३२ ]
[शा वा० समुकचय स्त० ४-श्लोक ६५
यदि पुनरेवमप्यनुगतसंबन्धधीनिर्वाहायाऽप्रामाणिकसमवायाभ्युपगमो न त्यज्यते, तदा लाघवादभावादिसाधारण वैशिष्टयमेव किमिति नाम्युपैपि । न चैवं पटवति भृतले पटाभावधीप्रसाः , तदानीं तदधिकरणतास्वाभाव्याभावस्य वक्तुमशक्यत्वात् , स्वभावस्य यावद्रव्यमादित्वात् ; रक्ततादशायाँ घटे श्यामाधिकरण तास्वामाव्येऽपि श्यामाभावेन तदेशे लोकिकप्रत्यक्षाभावादिति वाच्यम् , शाखाचच्छिन्नसंयोगसमवायस्य मृलावच्छेदेनेव वैशिष्ट्यस्य तत्काले तदधिकरणावच्छेदेन पटाभावं प्रत्यसंवन्धत्वात् । योग्य बात है कि समनिपत गुणों के समयाय में ऐक्य का अम्युपगम भी निर्दोष नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे 'जन में स्नेह का समदाय होता है किन्तु गन्ध का नहीं होता' यह प्रतीति होती है उसी प्रकार 'घट एवं रूप का जो सम्बन्ध है वह घट और रस का संबन्ध नहीं है' यह भी प्रतीति होती है। किन्तु घटगत रूप-रस के समनियत होने से यदि घट के साथ उन दोनों का एक ही समवाय माना आयगा तो इस प्रतीति को उपपत्ति नहीं हो सकती।
दूसरी बात यह है कि गुण-गुणो, जाति-व्यक्ति, अवयव-अधयक्षी, क्रिया कियावान् आदि के मध्य अतिरिक्त समवाय का अनुभव भी नहीं होता इसलिये सस्य बात यह है कि समवाय अतिरिक्त पदार्थ नहीं है जिसे अतिरिक्त सम्बन्ध के रूप में स्वीकार किया जाय। अपितु अपृथकभाव यानी प्रयुसिद्ध (मिलित) का अस्तित्व ही समवश्य है । इसलिये. 'गुण द्रव्य में समवेत होता है एवं 'जाति व्यक्ति में समवेत होती है' इत्यादि व्यवहार वचनों का तात्पर्य केवल इतना ही है कि द्रव्य से असंबद्ध होकर एवं व्यक्ति से असंबद्ध होकर गुण और जाति का अस्तित्व नहीं होता किन्तु अपने लोकसिद्ध द्रव्य और व्यक्ति रूप प्राश्रयों से सम्बद्ध होकर ही उनका अस्तित्व हाता है और वह सम्बन्ध प्राश्रय के परिणाम विशेषात्मक स्वरूप सम्बंध से मिन्न नहीं होता।
(अनुगतसंबंधाप्रतीति के बल पर समवायसिद्धि अशक्य) यदि नयायिक की अोर से यह कहा जाय कि-'जिन बातों के लिये अब तक समवाय संबंध की प्रावश्यकता बतायो गई थी उनकी अन्य प्रकार से उपपत्ति हो जाने के कारण समवाय की कल्पना पदि अनावश्यक प्रतीत होती है तो उन बातों के अनुरोध से समवाय की कल्पना न भी हो. किन्तु गण-किया-जाति आदि की विशिष्ट बुद्धिों में गुण-किया-जाति प्रादि के अनुगत सम्बन्ध का भान अनुभवसिद्ध है । प्रतः उसकी उपपत्ति के लिये प्रमाणान्तर का प्रभाव होने पर भो समवाय का त्याग नहीं किया जा सकता'-तो नैयायिक के इस कथन के प्रतिवाद में यह कहा जा सकता है कि तब तो गुण-क्रियानि की विशिष्ट बुद्धि में, एवं प्रभावावि की विशिष्टबुद्धि, इन सभी बुद्धिनों में लाधव की दृष्टि से एक हो अनुगत संबंध का हो भान मानना चाहिए और उसका वैशिष्टच नाम से व्यवहार करना चाहिए। फिर नेयायिक गुणादि का समवाय सम्बन्ध और प्रभावादि का स्वरूप संबन्ध ऐसो विभिन्न कल्पना क्यों करते हैं ? सभी का वैशिष्टय एक ही सम्बन्ध क्यों नहीं स्वीकारते?
(वशिष्ट्य संबन्ध में पटाभाव प्रत्यक्ष को प्रापत्ति नैयायिक) यदि इस के उत्तर में मंयायिक की ओर से कहा जाय कि सभी गुणादि का और सभी प्रभावों का एक ही वैशिष्ट्य सम्बन्ध मानने पर जिस काल में मूसल में पट होता है उस काल में भो भूतल