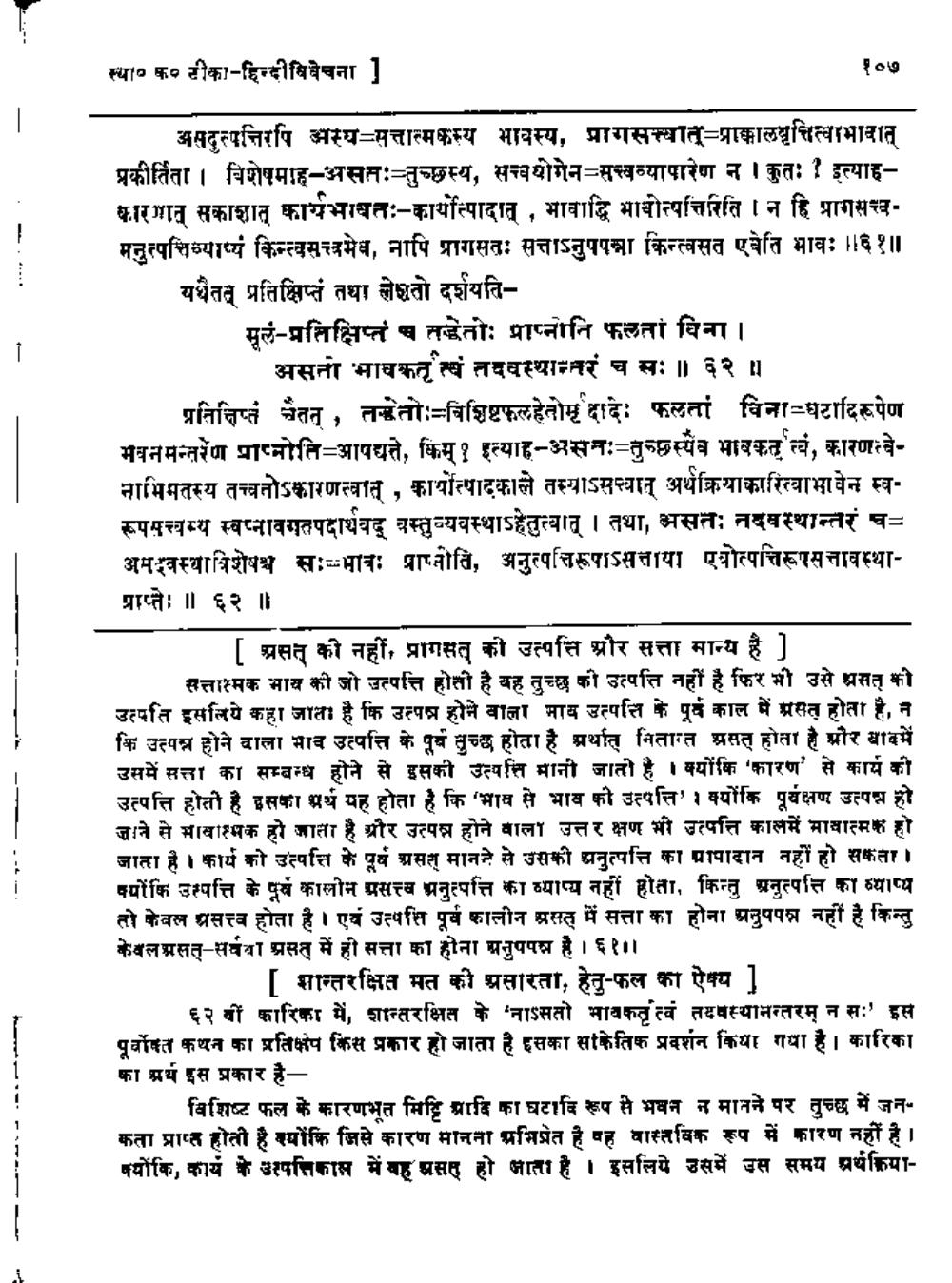________________
|
Î
---
स्था० क० टीका-हिन्दी विवेचना ]
असदुत्पत्तिरपि अस्य सत्तात्मकस्य भावस्य प्रागसत्त्वात् प्राक्कालवृत्तित्वाभावात् प्रकीर्तिता । विशेषमाह - असतः - तुच्छस्य, सच्च योगेन = सवव्यापारेण न । कुतः ? इत्याहकारणात् सकाशात् कार्यभावतः - कार्योत्पादात् भावादि भावोत्पत्तिरिति । न हि प्रागसवमनुत्पतिव्याप्यं किन्त्वसत्त्वमेव, नापि प्रागसतः सत्ताऽनुपपन्ना किन्त्वसव एवेति भावः ॥ ६१ ॥
यथैतत् प्रतिक्षिप्तं तथा लेशतो दर्शयति
1
१०७
सूर्य-प्रतिक्षिप्तं च तद्धेतोः प्राप्नोति फलतां विना ।
असतो भावकर्तृत्वं तववस्थान्तरं च सः ॥ ६२ ॥
,
प्रतिक्षिप्तं चैतत् ल तो: = विशिष्टफलहेतो दादेः फलतां विना घटादिरूपेण भवनमन्तरेण प्राप्नोति आपद्यते, किम् ? इत्याह- असन:- तुच्छस्यैव भावकर्तुं त्वं, कारणत्वेनाभिमतस्य तच्चतोऽकारणत्वात्, कार्योत्पादकाले तस्याऽसत्वात् अर्थक्रियाकारित्वाभावेन स्वरूपवस्य स्वप्नावगतपदार्थवद् वस्तुव्यवस्थाऽहेतुत्वात् । तथा, असतः नदवस्थान्तरं च = अमवस्थाविशेषश्च सः मात्रः प्राप्तोति, अनुत्पत्तिरूपाऽसत्ताया एवोत्पत्तिरूपसतावस्था - प्राप्तेः ॥ ६२ ॥
[ प्रसत् की नहीं, प्रागसत् की उत्पत्ति और सत्ता मान्य है ]
सत्तात्मक भाव की जो उत्पत्ति होती है यह तुच्छ की उत्पत्ति नहीं है फिर भी उसे असत् की उत्पति इसलिये कहा जाता है कि उत्पन्न होने वाला माव उत्पत्ति के पूर्व काल में प्रसत होता है, न कि उत्पन्न होने वाला भाव उत्पत्ति के पूर्व तुच्छ होता है अर्थात् नितान्त असत् होता है और बादमें उसमें सत्ता का सम्बन्ध होने से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है । क्योंकि 'कारण' से कार्य की उत्पत्ति होती है इसका अर्थ यह होता है कि 'भाव से भाव को उत्पत्ति' । क्योंकि पूर्वक्षण उत्पन्न हो जाने से भावात्मक हो जाता है और उत्पन्न होने वाला उत्तर क्षण भी उत्पत्ति कालमें मावात्मक हो जाता है। कार्य को उत्पत्ति के पूर्व असत् मानने से उसकी अनुत्पत्ति का प्रापादान नहीं हो सकता । क्योंकि उत्पत्ति के पूर्व कालीन प्रसत्त्व अनुत्पत्ति का व्याप्य नहीं होता, किन्तु अनुत्पत्ति का व्याप्य तो केवल सत्त्व होता है । एवं उत्पत्ति पूर्व कालीन असत् में सत्ता का होना अनुपपन्न नहीं है किन्तु केवल प्रसत्- सर्वत्रा श्रसत् में ही सत्ता का होना अनुपपन्न है । ६१ ।।
[ शान्तरक्षित मत की प्रसारता, हेतु-फल का ऐक्य ]
६२ वीं कारिका में, शान्तरक्षित के 'नाइसतो भावकर्तृत्वं तदवस्यानन्तरम् न स:' इस पूर्वोक्त कथन का प्रतिक्षेप किस प्रकार हो जाता है इसका सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है
विशिष्ट फल के कारणभूत मिट्टि श्रादि का घटादि रूप से भवन न मानने पर तुच्छ में जनकता प्राप्त होती है क्योंकि जिसे कारण मानना अभिप्रेत है वह वास्तविक रूप में कारण नहीं है। क्योंकि, कार्य के उत्पत्तिकाल में वह असत् हो जाता है । इसलिये उसमें उस समय अर्थक्रिया