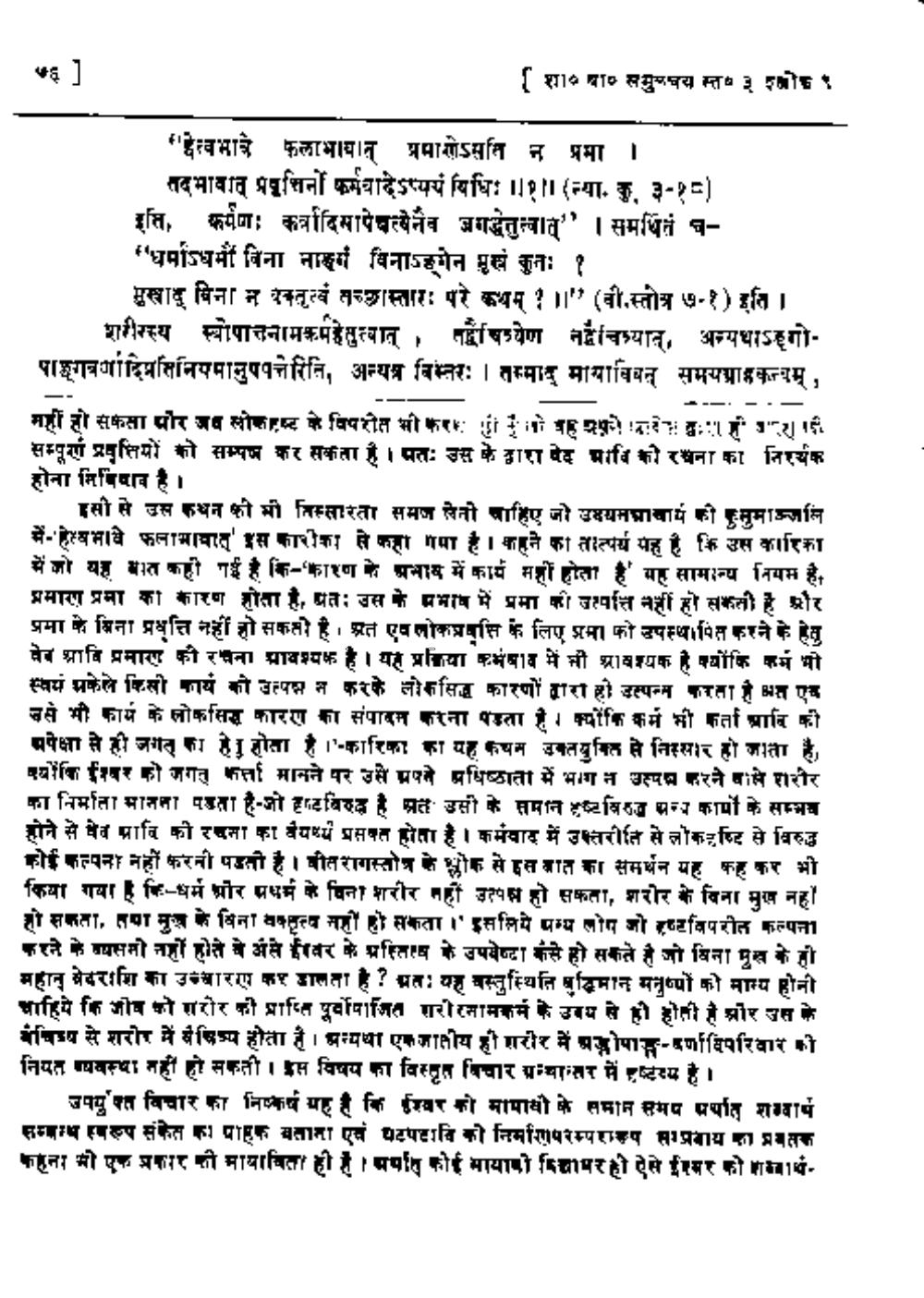________________
६]
[ शा० वा० समुच्चय स्त० ३९
फलाभावात् प्रमाऽसति न प्रभा ।
"त्वमा सदभावात् प्रसिन फर्मवादेऽप्ययं विधिः ॥ १ ॥ (न्या. कु. ३-१८) इसि कर्मणः कर्त्रादिसापेचत्वेनैव जगद्धेतुत्वात्" | समर्थितं च"धर्माधम विना नाहमं विनाऽङ्गेन मुखं कुतः १
खाद बिना न वक्तृत्वं तच्छास्तारः परे कथम् १ ||" (वी. स्तोत्र ७-१ ) इति । शरीरस्य स्पोपात्तनामक्रर्महेतुत्वात् तद्वैचित्रयेण नद्वैचित्र्याद, अन्यथाऽगोपात्रणां दिशि नियमानुपपत्तेरिति अन्यत्र विस्तरः । तस्माद मायाविधत् समयग्राहकत्वम्,
}
1
नहीं हो सका और जब लोकष्ट के विपरीत भी कर
सम्पूर्ण प्रवृत्तियों को सम्पन्न कर सकता है । मतः उस के द्वारा वेद मावि की रचना का निर्यक होना निविदा है।
इसी से उस कथन की भी विस्तारता समज सेतो चाहिए जो उदयनाचार्य की कुसुमाञ्जलि में हेयभावे फलाभावात्' इस कारीका से कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस कारिका में जो यह बात कही गई है कि कारण के अभाव में कार्य नहीं होता है' यह सामान्य नियम है, प्रमाण प्रभा का कारण होता है, अतः उस के प्रभाव में प्रभा की उत्पत्ति नहीं हो सकती है और प्रमा के बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। प्रत एव लोकप्रवृति के लिए प्रभा को उपस्थापित करने के हेतु वेब प्रावि प्रमाण की रचना श्रावश्यक है। यह प्रक्रिया कर्मभाव में भी श्रावश्यक है क्योंकि कर्म भो स्वयं अकेले किसी कार्य को उत्पन्न न करके लोकसिद्ध कारणों द्वारा हो उत्पन्न करता है अत एव उसे भी कार्य के लोकसि कारण का संपादन करना पडता है। क्योंकि कर्म भी कर्ता प्रावि की अपेक्षा से ही जगत् का हेतु होता है। कारिका का यह कथम उक्तयुक्ति से निस्सार हो जाता है, क्योंकि ईश्वर को जगत् कर्ता मानने पर उसे अपने अधिष्ठाता में भग्गन उत्पन करने वाले शरीर का निर्माता मानला पडता है जो हाटविरुद्ध है प्रत उसी के समान दृष्टविरुद्ध मन्त्र कार्यों के सम्भव होने से देव प्रावि की रचना का वैयथ्यं प्रसक्त होता है। कर्मवाद में उत्तरीति से लोकदृष्टि से विरुद्ध कोई कल्पना नहीं करनी पडती है। वीतरागस्तोत्र के श्लोक से इस बात का समर्थन यह कह कर भी किया गया है कि-धर्म और अधर्म के विना शरीर नहीं उत्पन्न हो सकता, शरीर के विना मुख नहीं हो सकता तथा मुख के बिना वक्तृत्व नहीं हो सकता। इसलिये अन्य लोग जो ष्टविपरीत कल्पना करने के व्यसनी नहीं होते वे अंसे ईश्वर के प्रति के उपवेष्टा कैसे हो सकते है जो बिना मुख के ही महान वेदराशि का उच्चारण कर डालता है ? अत: यह वस्तुस्थिति बुद्धिमान मनुष्यों को मान्य होनी चाहिये कि जीव को शरीर की प्राप्ति पूर्वोपार्जित शरीरसामकर्म के उदय से ही होती है और उस के यि से शरीर में वैषिष्य होता है। अन्यथा एकजातीय ही शरीर में अपाङ्ग वर्णादिपरिवार की नियत व्यवस्था नहीं हो सकती। इस विषय का विस्तृत विचार प्रन्यास में एष्टव्य है।
उपर्युक्त विचार का निष्कर्ष यह है कि ईश्वर को मायायों के समान समय अर्थात् सभ्यार्थ सम्बन्ध स्वरूप संकेत का ग्राहक बताना एवं घटपटादि को निर्माणपरम्पराप सम्प्रदाय का प्रयतक कहना भी एक प्रकार की मायाविता ही है। अर्थात् कोई मायाको विद्यामर ही ऐसे ईश्वर को