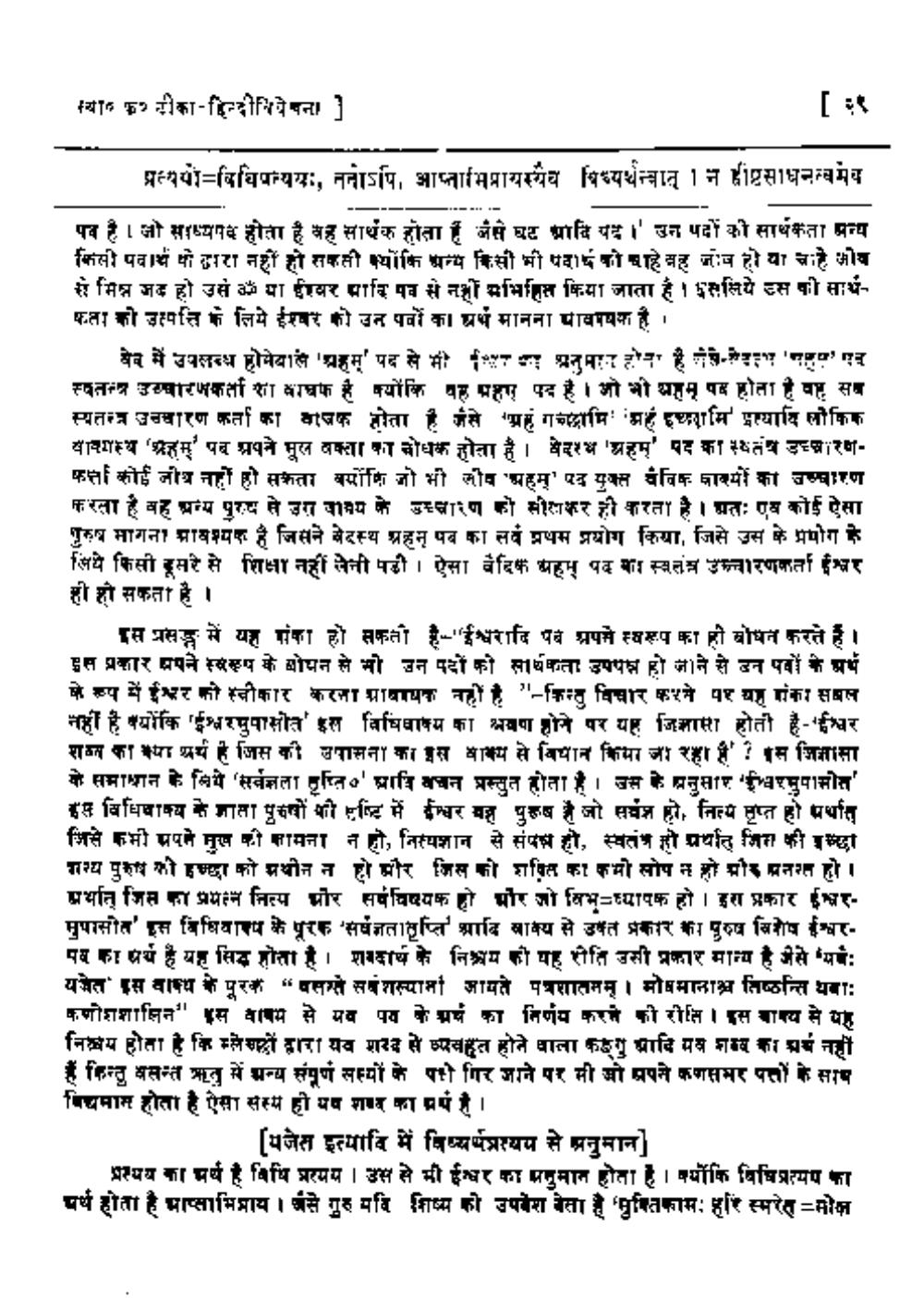________________
[:
प्रत्ययो विधिप्रत्ययः ननोऽपि आप्ताभिप्रायस्यैव विध्यर्थत्वात् । न ही साधनत्वमेव
पत्र है। जो साध्य होता है वह सार्थक होता है जैसे घट आदि पद । उन पदों की सार्थकता अन्य किसी पदार्थ के द्वारा नहीं हो सकती क्योंकि अन्य किसी भी पदार्थ को चाहे वह जीव हो या चाहे ओ सेमिन जब हो उसे या ईश्वर मावि पत्र से नहीं अभिहित किया जाता है। इसलिये उस की सार्थ पता को उत्पत्ति के लिये ईश्वर को उन पवों का प्रभं मानना बावमयका है.
1
स्वाद र टीका- हिन्दीविना ]
T
वेव में उपलब्ध होनेवाले 'ह' पद से
होता है
स्वतन्त्र उच्चारणकर्ता का वाचक है क्योंकि वह हर पद है। ओ भी अहम पद होता है वह सब स्वतन्त्र उच्चारण कर्ता का वाचक होता है जैसे "हं गच्छामि महं इच्छामि प्रत्यादि लौकिक वाक्यस्थ 'हम्' पर अपने मूल वक्ता का बोधक होता है । वेदश्य 'अहम्' पद का स्वतंत्र उच्चारणकर्ता कोई जी नहीं हो सकता क्योंकि जो भी सीब अहम्' पद युक्त वैविक वाक्यों का उच्चारण करता है वह अन्य पुरुष से उस वाक्य के उच्चारण को सोलकर ही करता है । धतः एवं कोई ऐसा माना आवश्यक है जिसने वेदस्य श्रहन् पब का सर्व प्रथम प्रयोग किया, जिसे उस के प्रयोग के लिये किसी दूसरे से शिक्षा नहीं लेनी पड़ी। ऐसा वैदिक अहम् पद का स्वतंत्र उच्चारणकर्ता ईश्वर ही हो सकता है ।
इस प्रसङ्ग में यह शंका हो सकती है- "ईश्वरादि पद श्रपसे स्वरूप का ही बोधन करते हैं। इस प्रकार पने स्वरूप के बोधन से भी उन पदों को सार्थकता उपपन्न हो जाने से उन पर्वो के अर्थ के रूप में ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है किन्तु विचार करने पर नहीं है क्योंकि श्वासोत' इस विधिवाक्य का श्रवण होने पर यह जिज्ञासा होती है- 'ईश्वर रात का क्या अर्थ है जिस की उपासना का इस वाक्य से विधान किया जा रहा है? इस जिज्ञासा के समाधान के लिये सर्वज्ञला तृप्ति०' प्रावि वचन प्रस्तुत होता है। उस के अनुसार 'राम' इस विधिवाक्य के जाता पुरुषों की दृष्टि में ईश्वर वह पुरुष है जो सर्वत्र हो, नित्य तृप्त हो अर्थात् जिसे कभी अपने मुख की कामना न हो, निस्पज्ञान से संपन हो, स्वतंत्र हो अर्थात् जिस की बा पुरुष की इच्छा को प्रथीन न हो और जिस को शति का कमी लोप न हो श्री प्रश्न हो । अर्थात् जिस का प्रयत्न नित्य और सर्वविषयक हो और जो विभु ध्यापक हो। इस प्रकार ईश्वरमुपासीत' इस विधिवाक्य के पूरक 'सर्वज्ञता तृप्ति श्रादि वाक्य से उक्त प्रकार का पुरुष विशेष ईश्वरकार्य है यह सिद्ध होता है। शब्दार्थ के निकाय की यह शैति उसी प्रकार मान्य है जैसे 'स यजेत इस वाक्य के पूरक "वससे सबंशस्याना जायते पत्र शातनम् । मोषमाना तिष्ठन्ति थबा कोशशालिन इस वाक्य से सब पय के अर्थ का निर्णय करने की रीति । इस वाक्य से यह निश्चय होता है कि मलेठों द्वारा यव शब्द से व्यवहुत होने वाला कगु आदि यत्र शब्द का अर्थ नहीं हैं किन्तु वसन्त ऋतु में अन्य संपूर्ण लक्ष्यों के पसे गिर जाने पर मी जो अपने कणसमर पत्तों के साथ विद्यमान होता है ऐसा सस्य ही यथ शब्द का प्रपं है ।
[भजेस इत्यादि में विध्यर्थप्रश्यम से अनुमान ]
प्रश्यय का अर्थ है विधि प्रत्यय। उस से भी ईश्वर का अनुमान होता है। क्योंकि विधिप्रत्यय का पर्थ होता है भासाभिप्राय । जैसे गुरु यदि शिष्य को उपवेश देता है 'मुक्तिकामः हरि स्मरेत मोक्ष
1