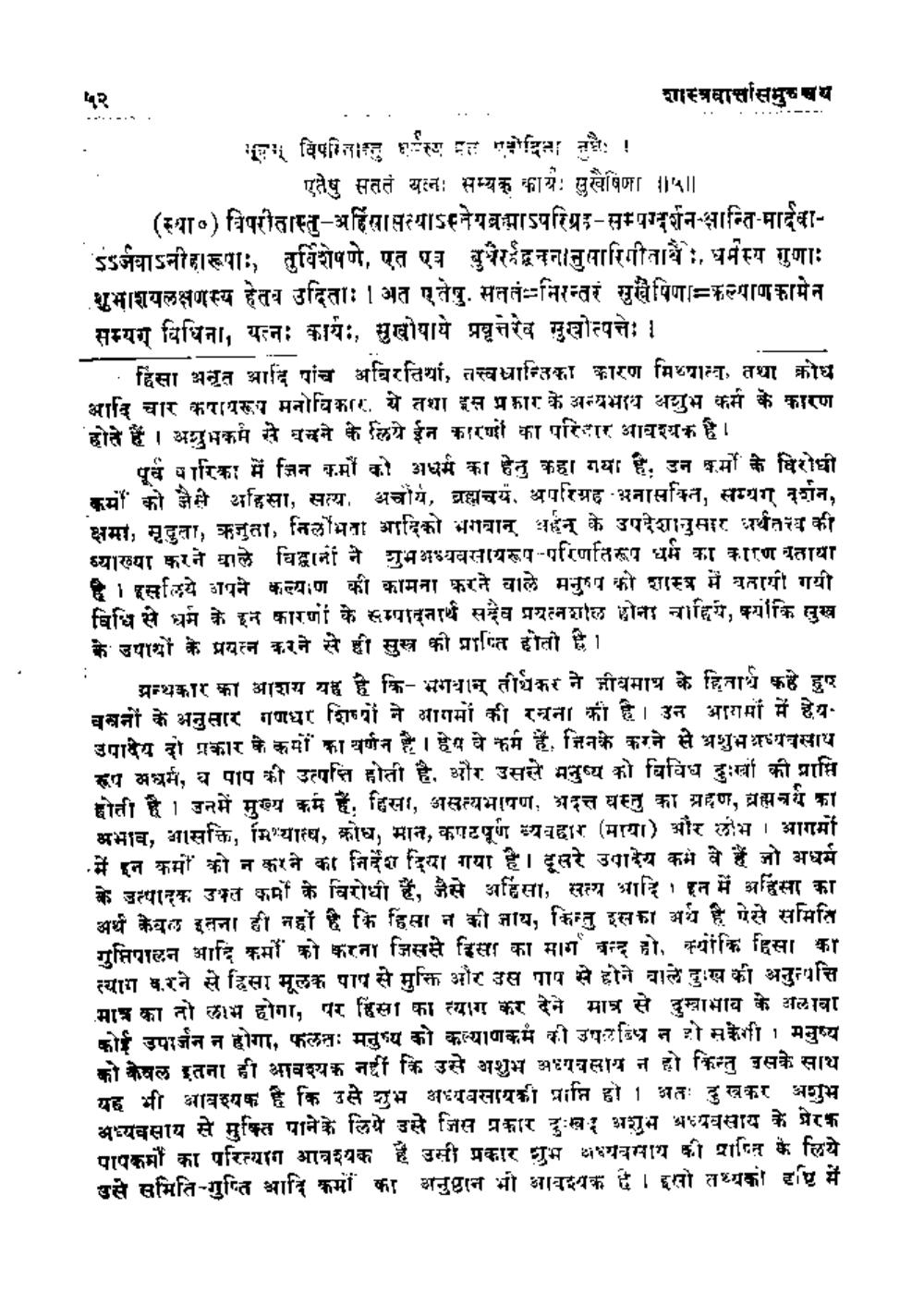________________
५२
शास्त्रवासिमुख चय र विपरिलानु पस्या मरा गोदिन नः !
एतेषु सततं यत्नः सम्यक् का यः सुखैषिणा ||५|| (स्था०) विपरीतास्तु-अहिंसातत्याऽस्नेयमाऽपरिग्रह-सम्पग्दर्शन-शान्ति-मार्दवाऽऽर्जबानीहारूपाः, तुर्विशेषणे, एत एष बुधरन नानुसारिगीताथै, धर्मस्य गुणाः शुभाशयलक्षणस्य हेतव उदिताः । अत एतेषु. सततं-निरन्तरं सुखैषिणा कल्याणकामेन सम्यग विधिना, यत्नः कार्यः, मुखोपाये प्रवृत्तरेव मुखोत्पत्तेः।
. हिंसा अनृत आदि पांच अबिरतियां, तत्वधान्तिका कारण मिथ्यात, तथा क्रोध आदि चार करायरूप मनोविकार. ये तथा इस प्रकार के अन्यभाष अशुभ कर्म के कारण होते हैं । अशुभकर्म से बचने के लिये इन कारणों का परिधार आवश्यक है।
पूर्व पारिका में जिन कमों को अधर्म का हेनु कहा गया है. उन कर्मों के विरोधी कर्मों को जैसे हिसा, सत्य, अचोय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह अनासक्नि, सम्यग दर्शन, क्षमा, मृदुता, ऋजुता, निर्लोभता आदिको भगवान् बहन के उपदेशानुसार अर्थतत्व की ध्याख्या करने वाले विद्वानों ने शुभअध्यवसायरूप-परिणतिरूप धर्म का कारण बताया है। इसलिये अपने कल्याण की कामना करने वाले मनुष्य को शास्त्र में बतायी गयी विधि से धर्म के इन कारणों के सम्पादनार्थ सदैव प्रयत्नशील होना चाहिये, क्योंकि सुख के उपायों के प्रयत्न करने से ही सुस्त्र की प्राप्ति होती है।
ग्रन्थकार का आशय यह है कि-भगवान् तीर्थकर ने जीवमात्र के हितार्थ फहे हुए वचनों के अनुसार गणधा शिष्यों ने आगमों की रचना की है। उन आरामों में हेय. उपादेय दो प्रकार के कर्मों का वर्णन है । हेय वे कर्म है, जिनके करने से अशुभअध्यवसाय रूप अधर्म, व पाप की उत्पत्ति होती है, और उसले मनुष्य को विविध दुग्यों की प्राप्ति होती है। उनमें मुख्य कर्म हैं, हिसा, असत्यभाषण, अदत्त घस्तु का ग्रहण, ब्रह्मचर्य का अभाव, आसक्ति, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, कपटपूर्ण व्यवहार (माया) और लोभ । आगमों में इन कमों को न करने का निर्देश दिया गया है। दूसरे उपादेय कमे वे हैं जो अधर्म के उत्पादक उक्त कर्मों के विरोधी हैं, जैसे अहिंसा, सत्य आदि। इन में अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि हिंसा न की जाय, किन्तु इसका अर्थ है ऐसे समिति गुप्तिगालन आदि कर्मों को करना जिससे दिसा का माग बन्द हो, क्योंकि हिसा का त्याग करने से हिसा मूलक पाप से मुक्ति और उस पाप से होने वाले दुःख की अनुत्पत्ति मात्र का तो लाभ होगा, पर हिंसा का त्याग कर देने मात्र से दुम्वाभाव के अलावा कोई उपार्जन न होगा, फलतः मनुष्य को कल्याणकर्म की उपट किंध न हो मकेगी । मनुष्य को केवल इतना ही आवश्यक नहीं कि उसे अशुभ अध्यवसाय न हो किन्तु उसके साथ यह भी आवश्यक है कि उसे शुभ अध्यबसायकी प्राप्ति हो । अतः दु ख कर अशुभ अध्यवसाय से मुक्ति पाने के लिये उसे जिस प्रकार दुःखद अशुभ अध्यवसाय के प्रेरक पापकर्मों का परित्याग आवश्यक है उसी प्रकार शुभ यवमाय की सानिन के लिये उसे समिति-गुप्ति आदि कर्मों का अनुष्ठान भी आवश्यक है। इसो तथ्यको दृष्टि में