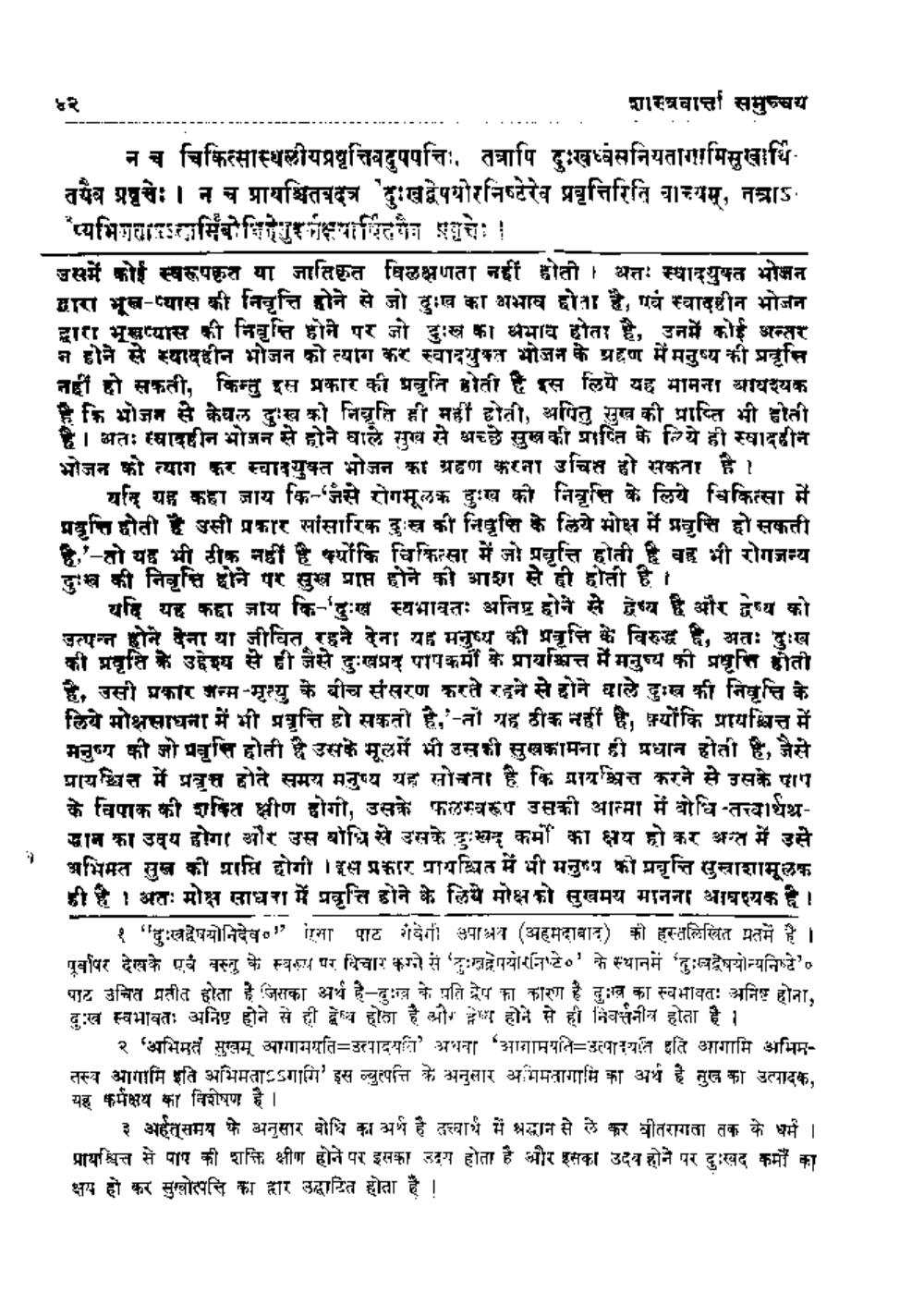________________
शास्त्रवार्ता समुच्चय न च चिकित्सास्थलीयप्रवृत्तिवदुपपत्तिः, तत्रापि दुःखध्वसनियतागामिमुखार्थितयैव प्रवृसेः । न च प्रायश्चितत्रदत्र 'दुःखद्वेषयोरनिष्टेरेव प्रवृत्तिरिति वाच्यम्, नत्राऽ. "प्यभिगमिबोशिशुपादित सारे जसमें कोई स्वरूपकृत या जातिकृत घिलक्षणता नहीं होती। अतः स्वादयुक्त भोजन मारा भूख-प्यास की निवृत्ति होने से जो दुःख का अभाव होता है, एवं स्वादष्ठीन भोजन द्वारा भूखप्यास की निवृत्ति होने पर जो दुःख का अभाव होता है, उनमें कोई अन्सर म होने से स्वादहीन भोजन को त्याग कर स्वादयुक्त भोजन के प्रहण में मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, किन्तु इस प्रकार की प्रवृति होती है इस लिये यह मामना आवश्यक है कि भोजन से केवल दुःख को निवृति ही नहीं होती, अपितु सुख की प्राप्ति भी होती है। अतः स्वादहीन भोजन से होने वाले सुख से अच्छे सुख की प्राप्ति के लिये ही स्वादहीन भोजन को त्याग कर स्वारयुक्त भोजन का ग्रहण करना उचित हो सकता है।
यान यह कहा जाय कि-'जैसे रोगमूलक दुःख की निवृति के लिये चिकित्सा में प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार सांसारिक दुःख की निवृत्ति के लिये भोक्ष में प्रवृत्ति हो सकती है, तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि चिकित्सा में जो प्रवृत्ति होती है वह भी रोगजन्य दुःख की निवृत्ति होने पर सुख प्राप्त होने की आशा से ही होती है।
यदि यह कहा जाय कि-'दुःख स्वभावतः अनिष्ट होने से द्वेष्य है और द्वेष्य को उत्पन्न होने देना या जीवित रहने देना यह मनुष्य की प्रवृत्ति के विरुद्ध है, अतः दुःख की प्रवृत्ति के उद्देश्य से ही जैसे दुःखप्रद पापकर्मों के प्रायश्चित्त में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार जन्म-मृत्यु के बीच संसरण करते रहने से होने वाले दुःख की निवृत्ति के लिये मोशसाधना में भी प्रवृत्ति हो सकती है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रायश्चित्त में मनुष्य की जो प्रवृति होती है उसके मूलमें भी उसकी सुखकामना ही प्रधान होती है, जैसे प्रायश्चित्त में प्रवृत्त होते समय मनुष्य यह सोचता है कि प्रायश्चित्त करने से उसके पाग के विपाक की शक्ति क्षीण होगी, उसके फलस्वरूप उसकी आन्मा में बोधि -तत्त्वार्थश्रखाम का उदय होगा और उस योधि से उसके दुःसन्द कर्मों का क्षय हो कर अन्त में उसे अभिमत सुख की प्राप्ति होगी । इस प्रकार प्रायश्चित में भी मनुष्य को प्रवृत्ति सुवाशामूलक ही है। अतः मोक्ष साधरा में प्रवृत्ति होने के लिये मोक्ष को सुखमय मानना आवश्यक है।
१ "दुःस्त्रद्वेषयोनिदेव." मा पाट गंवेगी अपाश्रय (अहमदाबाद) की हस्तलिखित प्रतमें है । पूर्वापर देखके एवं वस्तु के स्वरूप पर विचार कगो से 'दुन्नपयोरनिटे' के स्थानमें 'दुःस्वद्वेषयोन्यनिष्टे', पाट उचित प्रतीत होता है जिसका अर्थ है-दुश्व के पति द्रेप का कारण है दुःख का स्वभावतः अनिष्ट होना, दु:ख स्वभावतः अनिष्ट होने से ही द्वेध होता है और होने से ही निवसनीव होता है।
२ 'अभिमत सुखम् आगामयति उत्पादयति' अथवा 'आगामयति उत्पादयति इति आगामि अभिमतस्व आगामि इति अभिमताऽगागि' इस व्युत्पत्ति के अनुसार ममतागामि का अर्थ है सुख का उत्पादक, यह कर्मक्षय का विशेषण है।
३ अर्हत्समय के अनुसार बोधि का अर्थ है दरवार्थ में श्रद्धान से ले कर वीतरागता तक के धर्म । प्रायश्चित्त से पार की शक्ति क्षीण होने पर इसका उदय होता है और इसका उदव होने पर दुःखद कर्मों का क्षय हो कर सुखोत्पत्ति का द्वार उद्घाटित होता है ।