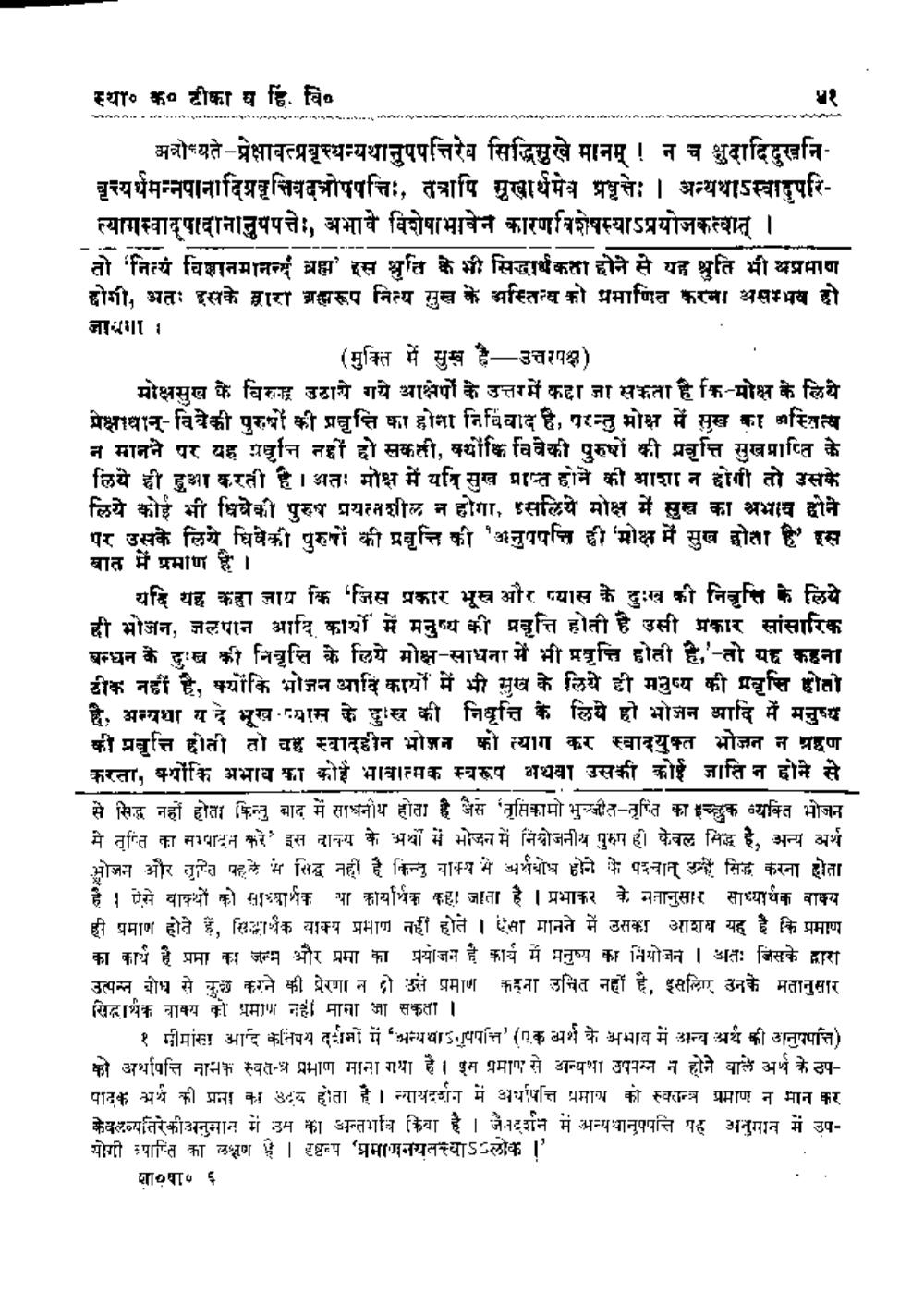________________
स्था० का टीका हि. वि०
अत्रोच्यते-प्रेक्षावत्प्रवृस्यन्यथानुपपत्तिरेव सिद्धिमुखे मानम् ! न च क्षुदादिदुखनिवृत्त्यर्थमन्नपानादिप्रकृत्तिवदत्रोपपत्तिः, तत्रापि मुखार्थमेव प्रवृत्तेः । अन्यथाऽस्वादुपरित्यागस्वादपादानानुपपत्तेः, अभावे विशेषाभावेन कारणविशेषस्याऽप्रयोजकत्वात् । तो 'नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इस श्रुति के भी सिद्धार्थकता होने से यह श्रुति भी प्रमाण होगी, अतः इसके द्वारा ब्रह्मरूप नित्य सुख के अस्तित्व को प्रमाणित करना असम्भव हो जायगा।
(मुक्ति में सुख है-उत्तरपक्ष) मोक्षसुख के विरूद्र उठाये गये आक्षेपों के उत्तरमें कहा जा सकता है कि-मोक्ष के लिये प्रेक्षाधान-विवेकी पुरुषों की प्रवृत्ति का होना निर्विवाद है, परन्तु मोक्ष में सुख का अस्तित्व न मानने पर यह प्रोन नहीं हो सकती, क्योंकि विवेकी पुरुषों की प्रवृत्ति सुख प्राप्ति के लिये ही हुआ करती है। अतः मोक्ष में यदि सुख प्राप्त होने की आशा न होगी तो उसके लिये कोई भी धिवेकी पुरुष प्रयत्नशील न होगा, इसलिये मोक्ष में सुख का अभाव होने पर उसके लिये विवेकी पुरुषों की प्रवृत्ति की 'अनुपपत्ति ही 'मोक्ष में सुख होता है इस बात में प्रमाण है।
यदि यह कहा जाय कि जिस प्रकार भूख और प्यास के दुःख की निवृत्ति के लिये ही भोजन, जलपान आदि कार्यो में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार सांसारिक बन्धन के दुःख की निवृत्ति के लिये मोक्ष-साधना में भी प्रवृत्ति होती है, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भोजन आदि कार्यों में भी सुख के लिये ही मनुष्य की प्रवृसि होतो है, अन्यथा य दे भूख-प्यास के दुःख की निवृत्ति के लिये हो भोजन आदि में मनुष्य की प्रवृत्ति होती तो वह स्वादहीन भोजन को त्याग कर स्वादयुक्त भोजन न ग्रहण करता, क्योंकि अभाव का कोई भावात्मक स्वरूप अथवा उसकी कोई जाति न होने से से सिद्ध नहीं होता किन्नु बाद में साधनीय होता है जैस 'तृप्तिकामो भुजीत-तृप्ति का इच्छुक व्यक्ति भोजन में तृप्ति का मम्पादन करे' इस वाक्य के अथों में भोजन में नियोजनीय पुरुप ही केवल सिद्ध है, अन्य अर्थ भोजन और तृप्ति पहले म सिद्ध नहीं है किन्तु वाक्य मे अर्थबोध होने के पश्चात् उसे सिद्ध करना होता है । ऐसे वाक्यों को साथ्यार्थक या कार्यार्थक कहा जाता है । प्रभाकर के मतानुसार साध्यार्थक वाक्य ही प्रमाण होते हैं, सिद्धार्थक वाक्य प्रमाण नहीं होते । ऐसा मानने में उसका आशय यह है कि प्रमाण का कार्य है प्रमा का जन्म और प्रमा का प्रयोजन है कार्य में मनुष्य का नियोजन । अतः जिसके द्वारा उत्पन्न बोध से कुछ करने की प्रेरणा न हो उसे प्रमाण कहना उचित नहीं है, इसलिए उनके मतानुसार सिदार्थक वाक्य को प्रमाण नहीं माना जा सकता ।
१ मीमांसा आद कतिपय दामों में अन्यथाऽपपत्ति' (एक अर्थ के अभाव में अन्व अर्थ की अनुपपत्ति) को अर्थापत्ति नानक स्वत-श्र प्रमाण माना गया है। इस प्रमाण से अन्यथा उपपन्न न होने वाले अर्थ के उपपादक अर्थ की प्राना का उदय होता है। न्यायदर्शन में अर्धापत्ति प्रमाग को स्वतन्त्र प्रमाण न मान कर केवलव्यतिरेकीअनुमान में उम का अन्तर्भाव किया है । जैनदर्शन में अन्यथानुपपत्ति यह अनुमान में उपयोगी पाप्ति का लक्षण | पृष्टम्प 'प्रमाणनयतत्त्वाऽ लोक ।'
शा०या०६