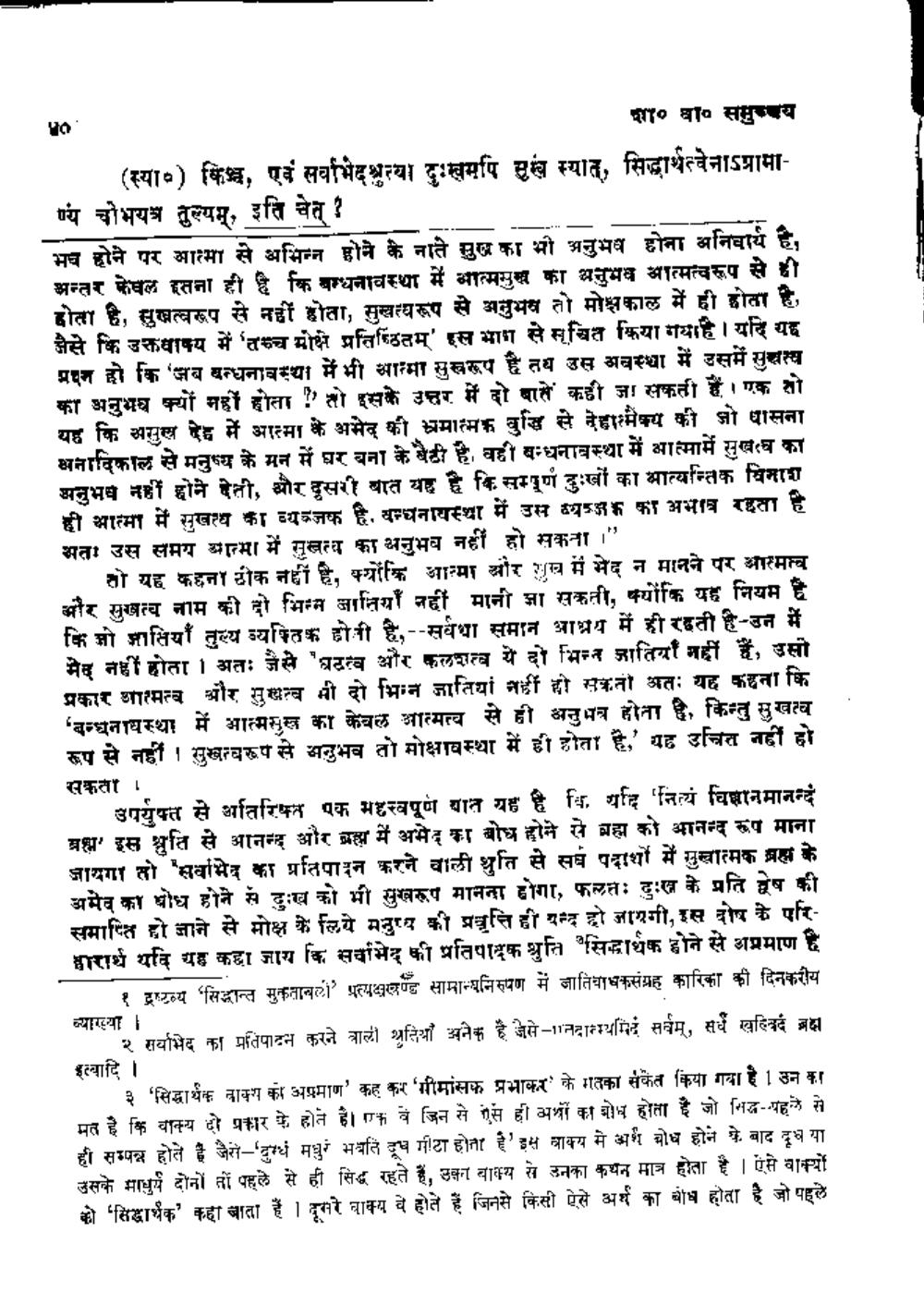________________
10.
शा. वा० समुपय (स्या०) किश्च, एवं सर्वाभेदश्रुत्या दुःखमपि सुख स्यात, सिद्धार्थत्वेनाऽप्रामाण्य चोभयत्र तुल्यम्, इति चेत् ? भव होने पर आत्मा से अभिन्न होने के नाते मुख का भी अनुभव होना अनिवार्य है, अन्तर फेवल इतना ही है कि बाधनावस्था में आत्मसुख का अनुभव आत्मत्वरूप से ही होता है, सुखत्वरूप से नहीं होता, सुखत्यरूप से अनुभव तो मोक्षकाल में ही होता है, जैसे कि उक्तवाक्य में 'तरुच मोक्षे प्रतिस्ठितम्' इस भाग से सूचित किया गया है। यदि यह प्रश्न हो कि 'जब बन्धनावस्था में भी आत्मा सुखरूप है तथ उस अवस्था में उसमें सुखस्व का अनुभव क्यों नहीं होता! तो इसके उत्तर में दो बातें कही जा सकती हैं। एक शो यह कि असुख देव में आत्मा के अमेद् की भ्रमात्मक बुद्धि से देहास्मैक्य की जो धासना अनादिकाल से मनुष्य के मन में घर बना के बैठी है. वही बन्धनावस्था में आत्मामें सुखत्व का अनुभव नहीं होने देती, और दूसरी बात यह है कि सम्पूर्ण दुःखों का आत्यन्तिक विनाश ही आत्मा में सुखत्य का व्यक्जक है. वचनावस्था में उस व्य क का अभाव रहता है अतः उस समय आत्मा में सुखत्य का अनुभव नहीं हो सकता ।"
तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा और स्त्र में भेद न मानने पर आरमन्च और सुखत्व नाम की दो भिन्म जातियों नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यह नियम है कि जो जातियाँ तुल्य व्यक्तिक होती है,--सर्वधा समान आश्रय में ही रहती है-उन में मेह नहीं होता । अतः जैसे पटव और कलश ये दो भिन्न जातियां नहीं है, उसी प्रकार आत्मत्व और सुखत्व मी दो भिन्न जातियां नहीं हो सकती अतः यह कहना कि 'बन्धनावस्था में आत्मसुख का केवल आत्मत्व से ही अनुभव होता है, किन्तु सुखत्व रूप से नहीं । सुखन्वरूप से अनुभव तो मोक्षावस्था में ही होता है, यह उचित नहीं हो सकता ।
उपर्युक्त से अतिरिक्त पक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि, यदि नित्यं विज्ञानमानन्द अश्ल' इस श्रुति से आनन्द और ब्रह्म में अमेद का बोध होने से ब्रह्म को आनन्द रूप माना जायगा तो सर्वाभेद का प्रतिपादन करने वाली श्रुति से सर्व पदार्थों में मुखात्मक ब्रह्म के अमेव का बोध होने से दुःख को भी सुखरूप मानना होगा, फलतः दुःख के प्रति वेष की समाप्ति हो जाने से मोक्ष के लिये मनुष्य की प्रवृत्ति ही यन्द हो जायगी, इस दोष के परिद्वारार्थ यदि यह कहा जाय कि सर्वाभेद की प्रतिपादक श्रुति सिद्धार्थक होने से अप्रमाण है
१ द्रष्टव्य सिद्धान्त मुकताबली' प्रत्यक्षपण्ड सामान्यनिरुपण में जातियाधकसंग्रह कारिका की दिनकरीय व्याख्या ।
२ सभेद का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों अनेक है जैसे-नदास्यमिदं सर्वम्, सधैं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि ।
३ 'सिद्धार्थक वाक्य को अप्रमाण' कह कर 'मीमांसफ प्रभाकर' के मतका संकेत किया गया है । उनका मत है कि वाक्य दो प्रकार के होते है। एक वे जिन से ऐसे ही अर्थों का बोध होता है जो सिद्ध-पहले से ही सम्पन्न होते है जैसे–'दुग्धं मधुरं भवति दूध मोटा होता है' इस वाक्य मे अर्थ बोध होने के बाद दूध या उसके माधुर्य दोनों तो पहले से ही सिद्ध रहते हैं, उन बाक्य से उनका कथन मात्र होता है । ऐसे वाक्यों को 'सिद्धार्थक' कहा जाता हैं । दूसरे वाक्य वे होते हैं जिनसे किसी ऐसे अर्थ का बोध होता है जो पहले