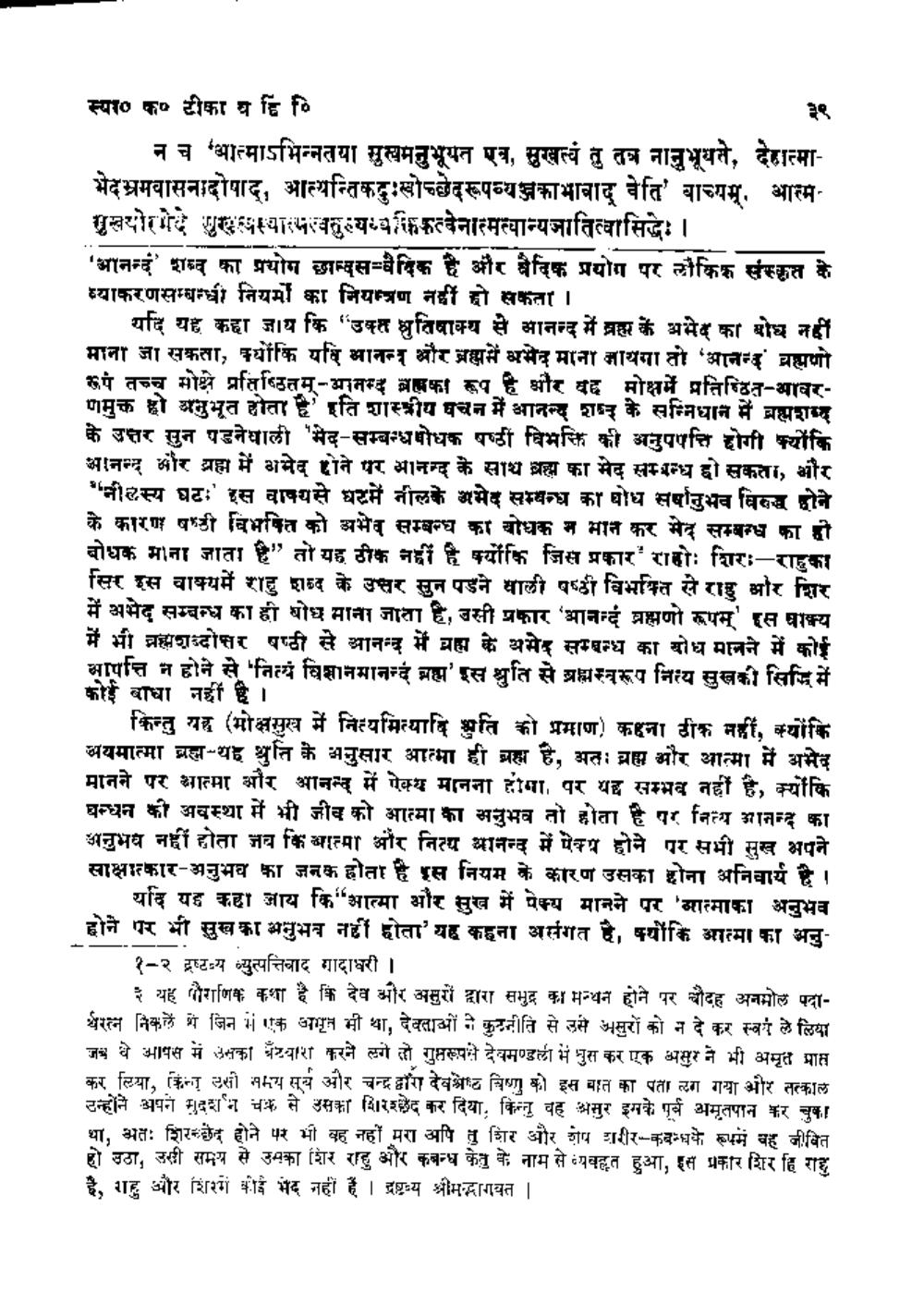________________
स्या० का टीका व हि
न च 'आत्माऽभिन्नतया मुखमनुभूयत एव, मुखत्यं तु तत्र नानुभूयते, देहात्माभेदभ्रमवासनादोपाद्, आत्यन्तिकदुःखोच्छेदरूपव्यञ्जकाभाना वेति' वाच्यम्. आत्ममुस्खयोरमेये सुरुवस्यात्मवतुल्य यक्षिकत्वेनात्मत्यान्यजातित्वासिद्धेः । 'आनन्द' शब्द का प्रयोग छाम्दस वैदिक है और वैदिक प्रयोग पर लौकिक संस्कृत के ध्याकरणसम्बन्धी नियमों का नियन्त्रण नहीं हो सकता।
यदि यह कहा जाय कि "उक्त श्रुतिवाक्य से आनन्द में ब्रह्म के अभेद का बोध नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि मानन्द और ब्रह्ममें अमेव माना जायगा तो 'आनन्द ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षे प्रतिष्ठित्तम्-आमम्द बलका रूप है और वह मोक्षमें प्रतिष्ठित-पावरणमुक्त हो अनुभूत होता है' इति शास्त्रीय वचन में आनन्द शब्द के सन्निधान में ब्रह्मशब्द के उत्तर सुन पडनेवाली 'मेद-सम्बन्धबोधक षष्ठी विभक्ति की अनुपपत्ति होगी क्योंकि आनन्द और ब्रह्म में अमेद होने पर आनन्द के साथ ब्रह्म का मेद सम्बन्ध हो सकता, और "नीरस्य घटः' इस वाक्यसे घटमें नीलके अमेद सम्बन्ध का घोध सर्षानुभव विरुद्ध होने के कारण षष्ठी विभक्ति को अभेव सम्बन्ध का बोधक म मान कर मेद सम्बन्ध का हो बोधक माना जाता है" तो यह ठीक नहीं है क्योंकि जिस प्रकार राहोः शिर:-राहुका सिर इस वाक्यमें राहु शब्द के उत्तर सुन पड़ने वाली षष्ठी विभक्ति से राहु और शिर में अभेद सम्बन्ध का ही बोध माना जाता है, उसी प्रकार 'आनन्दं ब्राह्मणो रूपम्' इस पाक्य में भी ब्रह्मशब्दोप्सर षष्ठी से आनन्द में ब्रह्म के अमेद सम्बन्ध का योध मालने में कोई
आपत्ति न होने से 'नित्यं विज्ञानमानन्द ब्रह्म' इस श्रुति से ब्रह्मस्वरूप नित्य सुखकी सिद्धि में कोई बाधा नहीं है।
किन्तु यह (मोक्षसुख में नित्यमित्यादि अति को प्रमाण) कहना ठीक नहीं, क्योंकि अयमात्मा ब्रह्म-यह श्रुति के अनुसार आत्मा ही ब्रह्म है, अतः ब्रह्म और आत्मा में अभेद मानने पर आत्मा और आनन्द में ऐक्य मानना होगा, पर यह सम्भव नहीं है, क्योंकि घन्धन की अवस्था में भी जीव को आत्मा का अनुभव तो होता है पर नित्य आनन्द का अनुभव नहीं होता जब कि बात्मा और नित्य मानन्द में ऐक्य होने पर सभी सुख अपने साक्षात्कार-अनुभव का जनक होता है इस नियम के कारण उसका होना अनिवार्य है।
यदि यह कहा जाय कि"आत्मा और सुख में पेश्य मानने पर 'मात्माका अनुभव होने पर भी सुख का अनुभव नहीं होता' यह कहना असंगत है, क्योंकि आत्मा का अनु
१-२ द्रष्टव्य व्युत्पत्तिवाद गादाधरी ।
३ यह पौणिक कशा है कि देव और असुरों द्वारा समुद्र का मन्थन होने पर चौदह अनमोल पदाथरत्न निकलें | जिन में एक अमृत भी था, देवताओं ने कुटनीति से उसे असुरों को न दे कर स्वयं ले लिया जब वे आपस में उसका अँट्यार करने लगे तो गुप्तरूपले देवमण्डली में घुस कर एक असुर ने भी अमृत प्राप्त कर लिया, किन्तु उसी समय सूर्य और चन्द्र द्वारा देवश्रेष्ठ विष्णु को इस बात का पता लग गया और तत्काल उन्होंने अपने मुदर्शन चक्र से उसका शिरश्छेद कर दिया, किन्तु वह असुर इसके पूर्व अमृतपान कर चुका था, अतः शिरच्छेद होने पर भी वह नहीं मरा अपि तु शिर और शेष शरीर-कबन्धके रूपमें वह जीवित हो उठा, उसी समय से उमका शिर राहु और कबन्ध केतु के नाम से व्यवहृत हुआ, इस प्रकार शिर हि राहु है, गहु और शिरमें कोई भेद नहीं हैं । द्रष्टव्य श्रीमद्भागवत ।