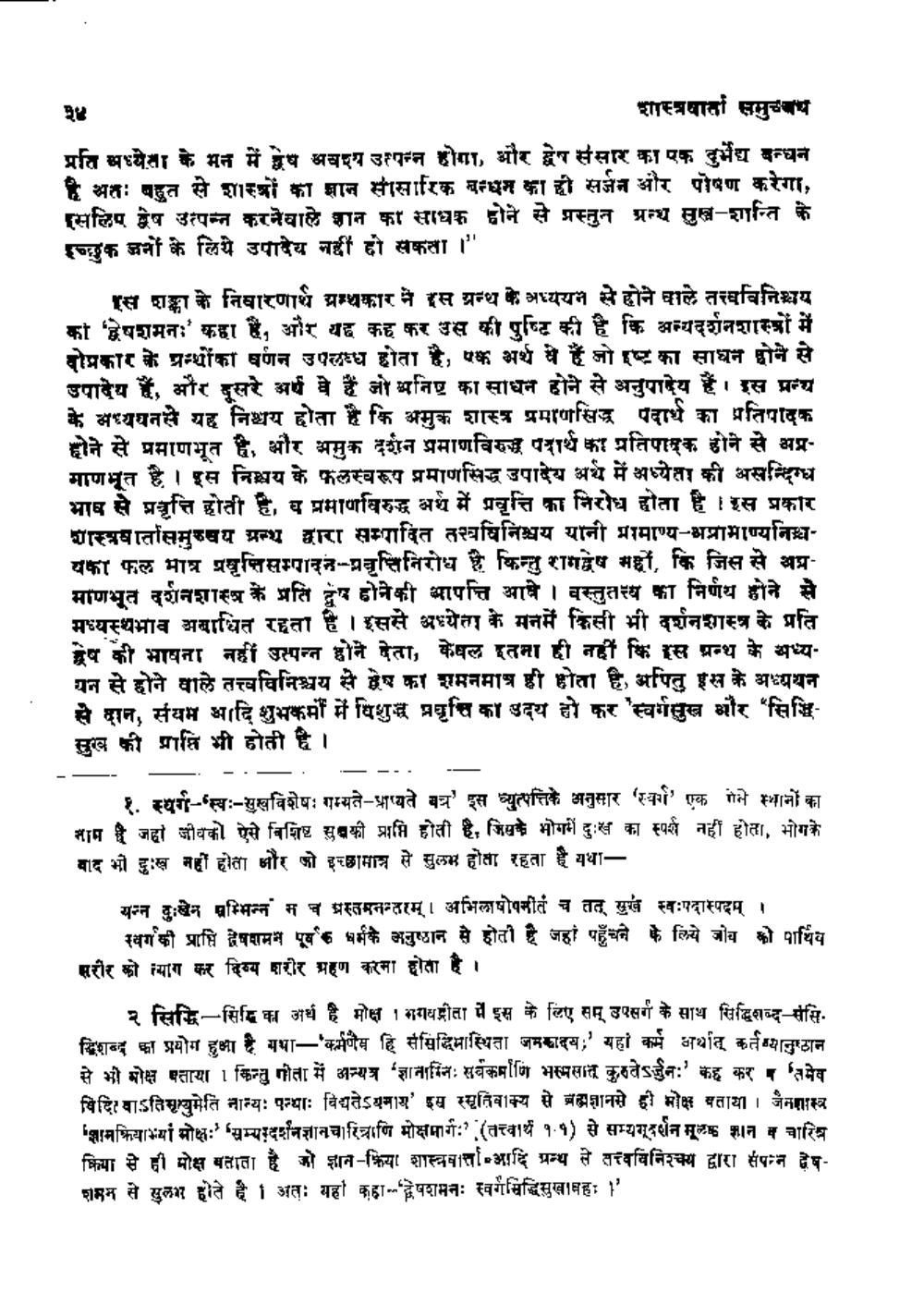________________
शास्त्रधाता समुच्चय प्रति अध्येता के मन में द्वेष अवश्य उत्पन्न होगा, और द्वेष संसार का एक दुर्भेद्य बन्धन है अतः बहुत से शास्त्रों का ज्ञान सांसारिक बन्धन का ही सर्जन और पोषण करेगा, इसलिए वेष उत्पन्न करनेवाले शान का साधक होने से प्रस्तुत ग्रन्थ सुख-शान्ति के इच्छुक जनों के लिये उपादेय नहीं हो सकता।"
इस शङ्का के निवारणार्थ ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ के अध्ययन से होने वाले तत्वविनिश्चय को 'द्वेषशमनः' कहा है, और यह कह कर उस की पुष्टि की है कि अन्यदर्शनशास्त्रों में दोप्रकार के प्राधोंका वर्णन उपलब्ध होता है, एक अर्थ वे हैं जो इष्ट का साधन होने से उपादेय है, और दूसरे अर्थ वे हैं जो अनिष्ट का साधन होने से अनुपादेय हैं। इस प्रन्य के अध्ययनसे यह निश्चय होता है कि अमुक शास्त्र प्रमाणसिद्ध पदार्थ का प्रतिपादक होने से प्रमाणभूत है, और अमुक दर्शन प्रमाणविरुद्ध पदार्थ का प्रतिपादक होने से अप्रमाणभूत है। इस निश्चय के फलस्वरूप प्रमाणसिद्ध उपादेय अर्थ में अध्येता की असन्दिग्ध भाष से प्रवृत्ति होती है, घ प्रमाविरुद्ध अर्थ में प्रवृत्ति का निरोध होता है । इस प्रकार शास्त्रषासमुरुखय ग्रन्थ द्वारा सम्पादित तस्वविनिश्चय यानी प्रामाण्य-अप्रामायनिश्चयका फल मात्र प्रवृत्तिसम्पादन-प्रवृत्तिनिरोध है किन्तु रागद्वेष महों, कि जिस से अप्रमाणभूत दर्शनशास्त्र के प्रति द्वप होनेकी आपत्ति आधे । वस्तुतत्य का निर्णय होने से मध्यस्थभाव अबाधित रहता है । इससे अध्येता के मनमें किसी भी दर्शनशास्त्र के प्रति द्वेष की भाषना नहीं उत्पन्न होने देता, केवल इतना ही नहीं कि इस प्रन्थ के अध्ययन से होने वाले तत्त्वविनिश्चय से देष का शमनमात्र ही होता है, अपितु इस के अध्ययन से दान, संयम आदि शुभकर्मों में विशुद्ध प्रवृत्ति का उदय हो कर 'स्वर्गसुख भौर "सिद्धिसुख की प्राप्ति भी होती है।
- -. -. . १. स्वर्ग-स्वः-सुखविशेषः गम्यते-प्राप्यते यत्र' इस ध्युत्पत्तिके अनुसार 'स्वर्ग' एक गेने स्थानों का भाम है जहाँ जीवको ऐसे विशिष्ट सुख की प्राप्ति होती है, जिसके भोगमें दुःख का स्पर्श नहीं होता, भोगके बाद भी दुःख नहीं होता और जो इच्छामात्र से सुलभ होता रहता है यथा
यन्न दुःखेन अम्मिन्न म च प्रस्तमनन्तरम् । अभिलाषोपमीतं च तत् सुख स्वःपदास्पदम् ।
स्वर्गकी प्राप्ति द्वेषशमन पूर्व धर्मक अनुष्ठान से होती है जहाँ पहुँचने के लिये जीव को पार्थिव सरीर को त्याग कर दिव्य शरीर ग्रहण करमा होता है।
२ सिद्धि-सिद्धि का अर्थ है मोक्ष । भगवडीता में इस के लिए सम् उपसर्ग के साथ सिद्धिशब्द-संसि. द्विशब्द का प्रयोग हुआ है यथा-'कर्मणैम हि संसिद्धिमास्थिता जमकादयः' यहां कर्म अर्थात् कर्तव्यानुष्ठान से भी मोक्ष पताया 1 किन्तु गीता में अन्यत्र 'ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुतेऽर्जुनः' कह कर नतिमेव विहिवाऽतिसायमेति नान्यः पन्थाः विद्यतेऽयमाय' इस स्मृतिवाक्य से ब्रह्मज्ञानसे ही मोक्ष बताया। जैनशास्त्र "ज्ञामक्रियाभ्यां मोक्षः' 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः (तत्त्वार्थ १.१) से सम्यग्दर्शन मूलक ज्ञान व चारित्र प्रिया से ही मोक्ष बताता है जो ज्ञान-क्रिया शास्त्रवाता आदि ग्रन्थ से तत्त्वविनिश्चय द्वारा संपन्न देषशमम से सुलर होते है । अतः यहाँ कहा--द्वेषशमनः स्वर्गसिद्धिसुखावहः ।'