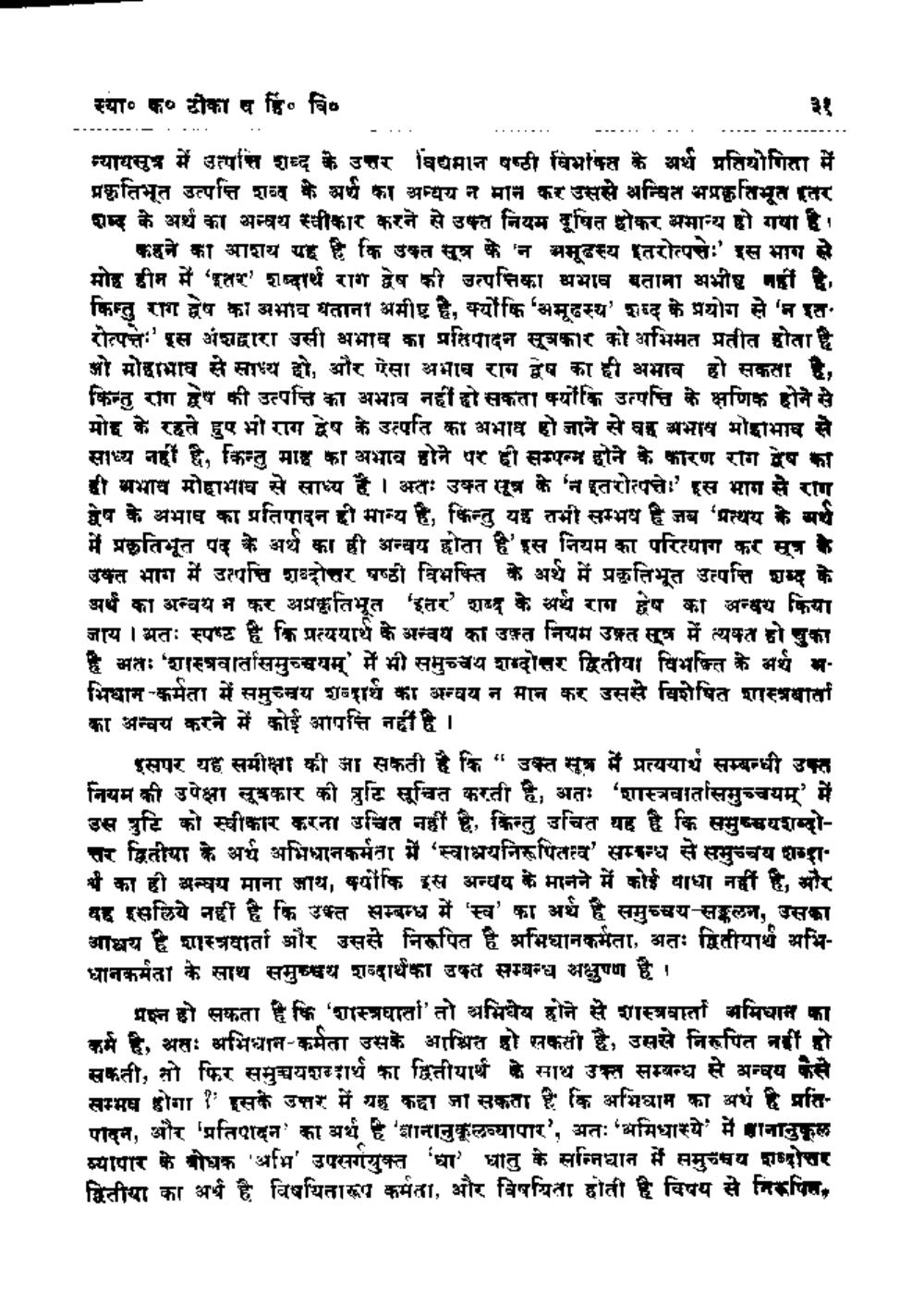________________
स्या० का टीका व हिं० वि०
३१
म्यायसूत्र में उत्पत्ति शब्द के उत्तर विद्यमान षष्ठी विभक्ति के अर्थ प्रतियोगिता में प्रकृतिभूत उत्पत्ति शब्द के अर्थ का अन्यय न मान कर उससे अन्धित भप्रकृतिभूत इतर शम्द के अर्थ का अन्वय स्वीकार करने से उक्त नियम दूषित होकर अमान्य हो गया है।
कहने का आशय यह है कि उक्त सूत्र के 'न अमूढस्य इतरोत्पतेः' इस भाग से मोह हीम में 'इतर' शब्दार्थ राग द्वेष की उत्पत्तिका अभाव बताना अभीष्ट नहीं है। किन्तु राग द्वेष का अभाव थताना अमीष्ट है, क्योंकि 'अमूहस्य' शब्द के प्रयोग से 'न इत. रोत्पत्तः' इस अंशद्वारा उसी अभाव का प्रतिपादन सूत्रकार को अभिमत प्रतीत होता है ओ मोहाभाव से साध्य हो, और ऐसा अभाव राग द्वेष का ही अभाव हो सकता है, किन्तु राग द्वेष की उत्पत्ति का अभाव नहीं हो सकता क्योंकि उत्पत्ति के क्षणिक होने से मोह के रहते हुए भी राग द्वेष के उत्पति का अभाव हो जाने से वह अभाव मोहाभाष से साध्य नहीं है, किन्तु माह का अभाव होने पर ही सम्पन्न होने के कारण राग देष का ही अभाव मोहाभाव से साध्य है । अतः उक्त सूत्र के 'न इतरोत्पत्तेइस भाग से राण वेष के अभाष का प्रतिपादन ही मान्य है, किन्तु यह तभी सम्भव है जब 'प्रत्यय के मार्थ में प्रकृतिभूत पद के अर्थ का ही अन्वय होता है' इस नियम का परित्याग कर सूत्र के उक्त भाग में उत्पत्ति शब्दोत्तर षष्ठी विभक्ति के अर्थ में प्रकृतिभूत उत्पत्ति शम्द के अर्थ का अन्वय भ कर अप्रकृतिभूत 'इत्तर' शब्द के अर्थ राग द्वेष का अन्वय किया जाय । अतः स्पष्ट है कि प्रत्ययार्थ के अन्वय का उक्त नियम उक्त सूत्र में त्यक्त हो चुका है अतः 'शास्त्रवार्तासमुच्चयम्' में भी समुच्चय शब्दोसर द्वितीया विभक्ति के मर्थ म. मिधाम कर्मता में समुच्चय शब्दार्थ का अन्वय न मान कर उससे विशेषित शास्त्रबार्ता का अन्वय करने में कोई आपत्ति नहीं है ।
इसपर यह समीक्षा की जा सकती है कि " उक्त सूत्र में प्रत्ययार्थ सम्बन्धी उक्त नियम की उपेक्षा सूत्रकार की त्रुटि सूचित करती है, अतः 'शास्त्रवातासमुच्चयम्' में उस त्रुटि को स्वीकार करना उचित नहीं है, किन्तु उचित यह है कि समुश्मयशदोतर द्वितीया के अर्थ अभिधानकर्मता में 'स्वाश्रयनिरूपितत्व' सम्बन्ध से समुच्चय शम्दा. 2 का ही अन्धय माना आय, क्योंकि इस अन्धय के मानने में कोई बाधा नहीं है, और वह इसलिये नहीं है कि उक्त सम्बन्ध में 'स्व' का अर्थ है समुच्चय-सङ्कलन, उसका आश्रय है शास्त्रवार्ता और उससे निरूपित है अभियानकर्मता, अतः द्वितीयार्थ अभिधानकर्मता के साथ समुच्चय शब्दार्थका उक्त सम्बन्ध अक्षुण्ण है।
प्रश्न हो सकता है कि 'शास्त्रघाता' तो अभिधेय होने से शास्त्रवार्ता अमिधान का कर्म है, अतः अभिधान-कर्मता उसके आश्रित हो सकती है, उससे निरूपित नहीं हो सकती, तो फिर समुच्चयशदार्थ का द्वितीयार्थ के साथ उक्त सम्बन्ध से अन्धय कैसे सम्भव होगा ?' इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि अभिधाम का अर्थ है प्रतिपादन, और 'प्रतिपादन' का अर्थ है 'ज्ञानानुकूलव्यापार', अतः 'अमिधास्ये में जानानुकल व्यापार के बोधक 'अभि' उपसर्गयुक्त 'धा' धातु के सान्निधान में समुच्चय शदोसर द्वितीया का अर्थ है विषयितारूप कर्मता, और विषयिता होती है विषय से निरूपित,