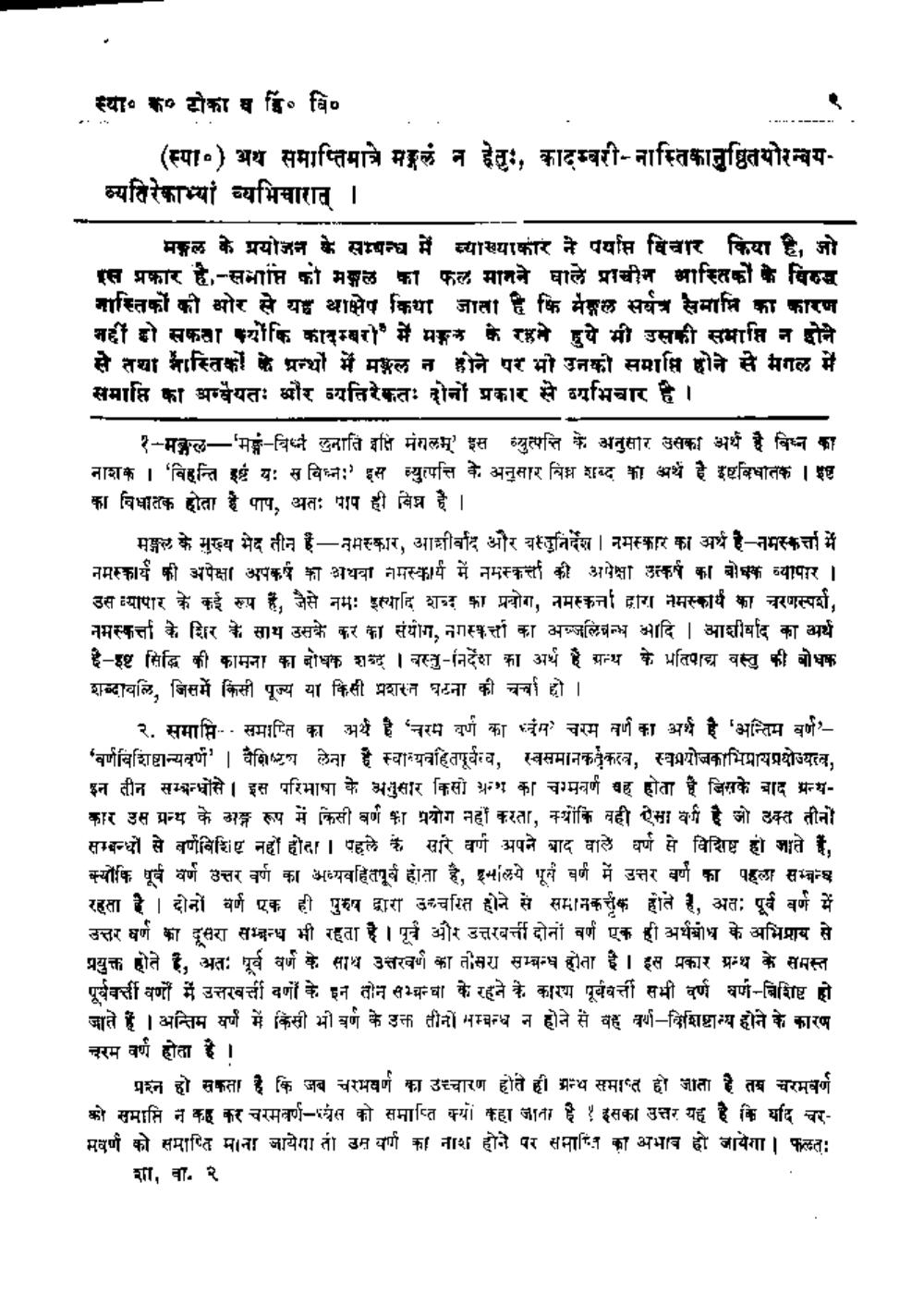________________
स्या० ० टोका व हिं० वि०
(स्पा.) अथ समाप्तिमात्रे मङ्गलं न हेतुः, कादम्बरी- नास्तिकानुष्ठितयोरन्बयव्यतिरेकाभ्यां व्यभिचारात् ।
माल के प्रयोजन के सम्बन्ध में व्याख्याकार ने पर्याप्त विचार किया है, जो इस प्रकार है,-समाप्ति को माल का फल मानने पाले प्राचीन आस्तिकों के विस नास्तिकों की ओर से यह थाक्षेप किया जाता है कि मैगल सर्वत्र समाप्ति का कारण नहीं हो सकता क्योंकि कादम्बरो' में मजल के रहने हुये भी उसकी समाप्ति न होने से तथा मास्तिकों के प्रन्यो में माल न होने पर भी उनकी समाप्ति होने से मगल में समाप्ति का अग्धयतः और व्यतिरेकातः दोनों प्रकार से व्यभिचार है।
१-मबल-मई-विन लुनाति इति मंगलम्' इस व्युत्पत्ति के अनुसार उसका अर्थ है विध्न का नाशक । 'विहन्ति इष्ट यः स विश्न: इस व्युत्पत्ति के अनुसार विन शब्द का अर्थ है इविधातक । इट का विधातक होता है पाप, अतः पाप ही विघ्न है ।
माल के मुख्य भेद तीन है-नमस्कार, आशीर्वाद और वस्तुनिर्देश | नमस्कार का अर्थ है-नमस्का में नमस्कार्य की अपेक्षा अपकर्ष का अथवा नमस्कार्य में नमस्कर्ता की अपेक्षा उत्कर्ष का बोरक व्यापार । उस व्यापार के कई रूप हैं, जैसे नमः इत्यादि शब्द का प्रयोग, नमस्का द्वारा नमस्कार्य का चरणस्पर्श, नमस्कर्ता के शिर के साथ उसके कर का संयोग, नगस्कर्ता का अञ्जलिबन्ध आदि | आशीर्वाद का अर्थ है-इष्ट सिद्धि की कामना का बोधक शब्द । वस्तु-निर्देश का अर्थ है ग्रन्थ के प्रतिपाद्य वस्तु की बोधक शब्दावलि, जिसमें किसी पूज्य या किसी प्रशस्त घटना की चर्चा हो ।
२. समाप्ति . समाप्ति का अर्थ है 'नरम वर्ण का दम' चरम वर्ण का अर्थ है 'अन्तिम वर्ण'वर्णविशिष्टान्यवर्ण' । वैशिष्टय लेना है स्वान्यवहितपूर्वस्व, स्वसमानक कल, स्वप्रयोजकाभिप्रायप्रयोज्यत्व, इन तीन सम्बन्धोंसे । इस परिभाषा के अनुसार किसो अन्ध का चम्मवर्ण बह होता है जिसके बाद अन्यकार उस ग्रन्थ के अङ्ग रूप में किसी वर्ण का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वही ऐसा वर्ग है जो उक्त तीनो सम्बन्धों से वर्णविशिष्ट नहीं होता। पहले के सारे वर्ण अपने बाद वाले वर्ण से विशिष्ट हो जाते है, स्योंकि पूर्व वर्ण उत्तर वर्ण का अव्यवहितपूर्व होता है, इसलिये पूर्व वर्ण में उत्तर वर्ण का पहला सम्बन्ध रहता है । दोनों वर्ण एक ही पुरुष द्वारा उचरित होने से समामकर्तृक होते हैं, अतः पूर्व वर्ग में उत्तर वर्ण का दूसरा सम्बन्ध भी रहता है। पूर्व और उत्तरवर्ती दोनों वर्ण एक ही अर्थबोध के अभिप्राय से प्रयुक्त होते है, अतः पूर्व वर्ण के साथ उत्तरवर्ण का तीसरा सम्बन्ध होता है । इस प्रकार ग्रन्थ के समस्त पूर्ववर्ती वर्गों में उत्तरवर्ती वर्गों के इन तीन सम्बन्चा के रहने के कारण पूर्ववर्ती सभी वर्ण वर्ण-विशिष्ट हो जाते हैं । अन्तिम वर्ण में किसी भी वर्ण के उक्त तीनो सम्बन्ध न होने से वह वर्ग-विशिष्टान्य होने के कारण चरम वर्ण होता है।
प्रश्न हो सकता है कि जब चरमवर्ण का उच्चारण होते ही अन्य समाप्त हो जाता है तब चरमवर्ण को समाप्ति न कह कर चरमवर्ण-वस को समाप्ति क्यों कहा जाता है इसका उत्तर यह है कि यदि चरमवर्ण को समाप्ति माना जायेगा तो उस वर्ण का नाश होने पर समाप्ति का अभाव हो जायेगा। फलतः
शा, वा. २