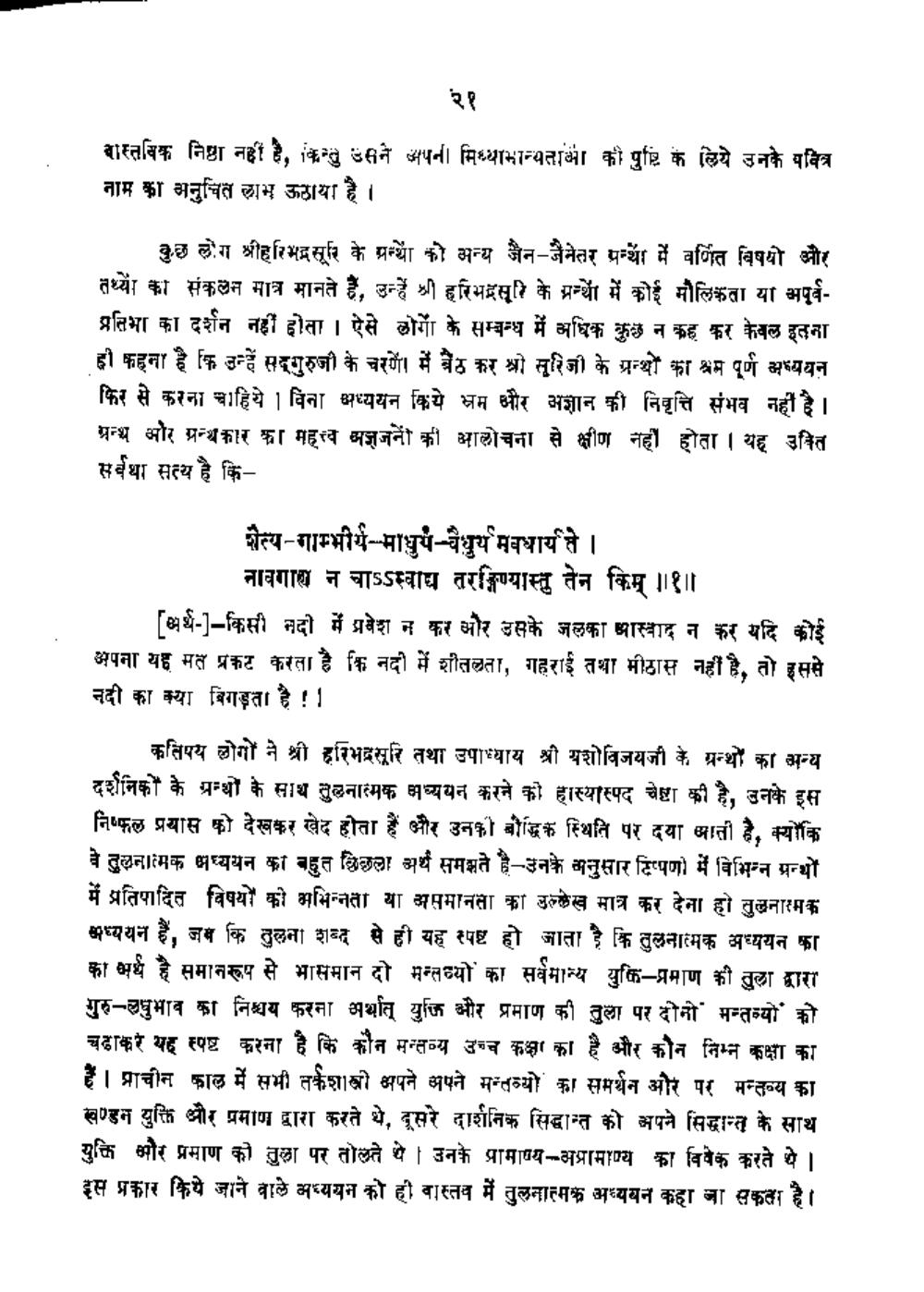________________
शास्तविक निष्ठा नहीं है, किन्तु उसने अपना मिथ्यामान्यतामा की पुष्टि के लिये उनके पवित्र नाम का अनुचित लाभ ऊठाया है।
कुछ लोग श्रीहरिभद्रसूरि के ग्रन्थों को अन्य जैन-जैनेतर अन्यों में वर्णित विषयो और तथ्यों का संकलन मात्र मानते हैं, उन्हें श्री हरिभद्रसूरि के ग्रन्थों में कोई मौलिकता या अपूर्वप्रतिभा का दर्शन नहीं होता । ऐसे लोगों के सम्बन्ध में अधिक कुछ न कह कर केवल इतना ही कहना है कि उन्हें सद्गुरुजी के चरणें। में बैठ कर श्री सरिजी के ग्रन्थों का श्रम पूर्ण अध्ययन फिर से करना चाहिये । विना अध्ययन किये भ्रम और अज्ञान की निवृत्ति संभव नहीं है । प्रन्थ और ग्रन्थकार का महत्व अज्ञजनों की आलोचना से क्षीण नहीं होता । यह उक्ति सर्वथा सत्य है कि
शैत्य-गाम्भीर्य-माधुप-चैधुर्य मवधार्यते ।
नावगाथ न चाऽऽस्वाध तरङ्गिण्यास्तु तेन किम् ॥१॥ [अर्थ-]-किसी नदी में प्रवेश न कर और उसके जलका पास्वाद न कर यदि कोई अपना यह मत प्रकट करता है कि नदी में शीतलता, गहराई तथा मीठास नहीं है, तो इससे नदी का क्या बिगड़ता है !!
कतिपय लोगों ने श्री हरिभद्रसूरि तथा उपाध्याय श्री यशोविजयजी के ग्रन्थों का अन्य दर्शनिको के ग्रन्थों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने को हास्यास्पद चेष्टा की है, उनके इस निष्फल प्रयास को देखकर खेद होता हैं और उनकी बौद्धिक स्थिति पर दया पाती है, क्योंकि वे तुलनात्मक अध्ययन का बहुत छिछला अर्थ समझते है-उनके अनुसार टिप्पणो में विभिन्न ग्रन्थों में प्रतिपादित विषयों को भभिन्नता या असमानता का उल्लेख मात्र कर देना हो तुलनात्मक अध्ययन हैं, जब कि तुलना शब्द से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलनात्मक अध्ययन का का अर्थ है समानरूप से भासमान दो मन्तव्यों का सर्वमान्य युकि-प्रमाण की तुला द्वारा गुरु-लघुभाव का निश्चय करना अर्थात् युक्ति और प्रमाण की तुला पर दोनो मन्तव्यों को चढाकरे यह स्पष्ट करना है कि कौन मन्तव्य उच्च कक्षा का है और कौन निम्न कक्षा का हैं। प्राचीन काल में सभी तर्कशास्त्री अपने अपने मन्तव्यों का समर्थन और पर मन्तव्य का खण्डन युक्ति और प्रमाण द्वारा करते थे, दूसरे दार्शनिक सिद्धान्त को अपने सिद्धान्त के साथ युक्ति और प्रमाण को तुला पर तोलते थे । उनके प्रामाण्य-अप्रामाण्य का विवेक करते थे । इस प्रकार किये जाने वाले अध्ययन को ही वास्तव में तुलनात्मक अध्ययन कहा जा सकता है।