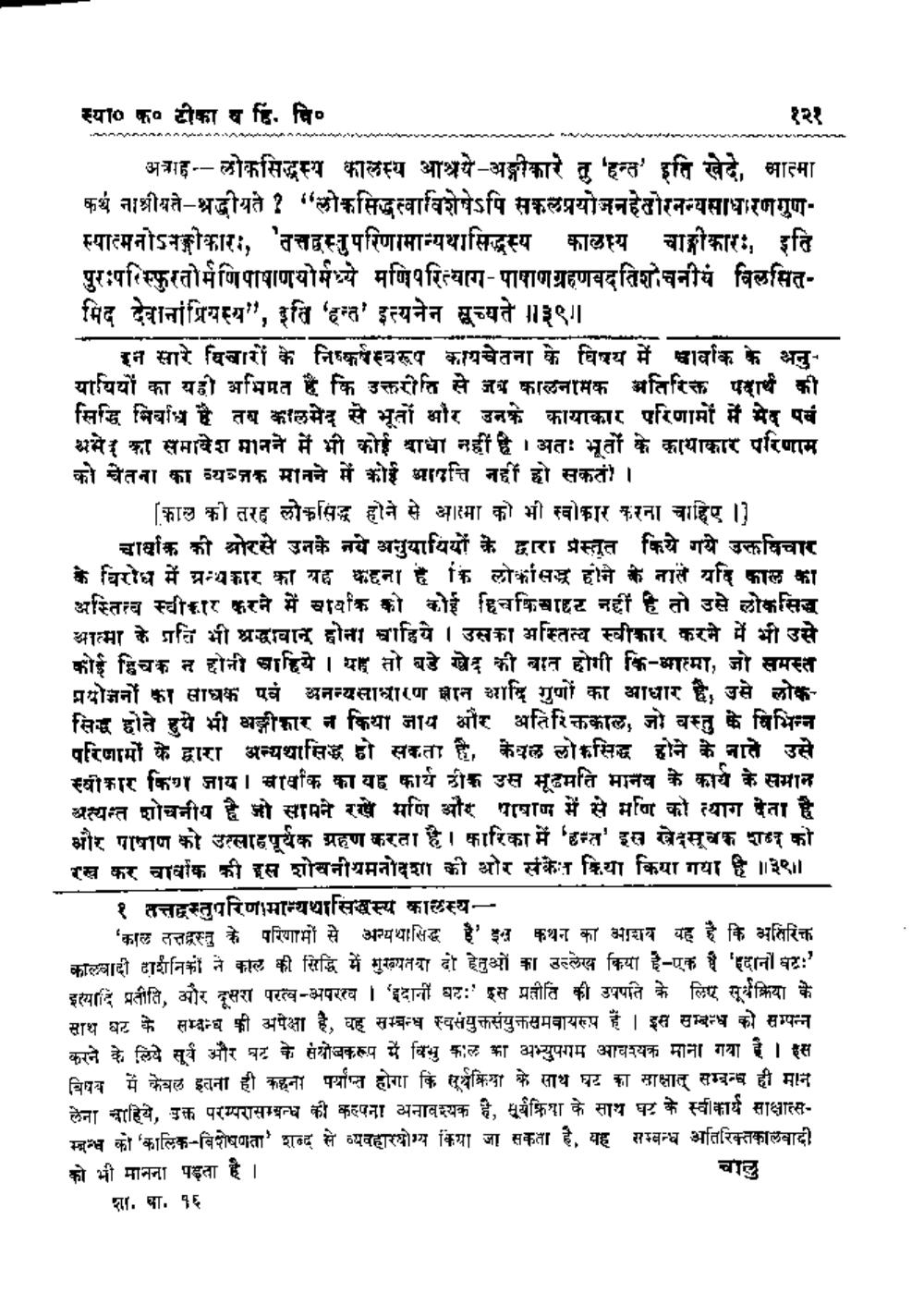________________
ma
स्या० का टीका वहि. वि.
१२१ __ अत्राह-- लोकसिद्धस्य कालस्य आश्रये -अङ्गीकारे तु 'हन्त' इति खेदे, मात्मा कथं नाश्रीयते-श्रद्धीयते ? "लोकसिद्धत्वाविशेषेऽपि सकलप्रयोजनहेतोरनन्यसाधारणगुणस्यात्मनोऽनङ्गोकारस, 'तत्सद्वस्तुपरिणामान्यथासिद्धस्य कालाय चाङ्गीकारः, इति पुर:परिस्फुरतोमणिपाषाणयोर्मध्ये मणिपरित्याग-पाषाणग्रहणवदतिशोचनीयं विलसितमिद देवानांप्रियस्य", इति 'हन्त' इत्यनेन सूच्यते ॥३९॥
इन सारे विचारों के निष्कर्षस्वरूप कायचेतना के विषय में चार्वाक के अनु यायियों का यही अभिमत है कि उक्तरीति से जब कालनामक अतिरिक्त पदार्थ की सिद्धि मिधि है तब कालमेद से भूतों और उनके कायाकार परिणामों में मेव पर्व अमेई का समावेश मानने में भी कोई बाधा नहीं है। अतः भूतों के कायाकार परिणाम को चेतना का व्यन्जक मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती।
काल की तरह लोकसिद्ध होने से आत्मा को भी स्वीकार करना चाहिए । चार्वाक की ओर से उनके नये अनुयायियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्तविचार के विरोध में ग्रन्थकार का यह कहना है कि लोकांस होने के नासे यदि काल का अस्तित्व स्वीकार करने में वार्याक को कोई हिचकिचाहट नहीं है तो उसे लोकसिद्ध आत्मा के प्रति भी श्रद्धावान होना चाहिये । उसका अस्तित्व स्वीकार करने में भी उसे कोई हिचक न होनी चाहिये । यह तो बडे खेद की बात होगी कि-यात्मा, जो समस्त प्रयोजनों का साधक पवं अनन्यसाधारण शान आदि गुणों का आधार है, उसे लोकसिद्ध होते हुये भी अङ्गीकार न किया जाय और अतिरिक्तकाल, जो वस्तु के विभिन्न परिणामों के द्वारा अन्यथासिद्ध हो सकता है, केवल लोकसिद्ध होने के नाते उसे स्वीकार किए जाय । चार्वाक का यह कार्य ठीक उस मूढमति मानव के कार्य के समान अत्यन्त शोचनीय है जो सामने रखे मणि और पाषाण में से मणि को त्याग देता है और पाषाण को उत्साहपूर्वक ग्रहण करता है। कारिका में 'हन्त' इस खेदसूचक शहन को रख कर चार्वाक की इस शोचनीयमनोदशा की ओर संकेत क्रिया किया गया है ॥३९॥
१ तत्तद्वस्तुपरिणामान्यथासिसस्य कालस्य
'काल तत्तद्रस्तु के परिणामों से अन्यथा सिद्ध है' इस कथन का आशय यह है कि अतिरिक्त कालवादी दार्शनिकों ने काल की सिद्धि में मुख्यतया दो हेतुओं का उल्लेख किया है-एक है 'हदानी घटः' इत्यादि प्रतीति, और दूसरा परत्व-अपररव । इदानी घटः' इस प्रतीति की उपपत्ति के लिए सूर्यक्रिया के साथ घट के सम्बन्ध की अपेक्षा है, वह सम्बन्ध स्वसंयुक्तसंयुक्तसमवायरूप हैं । इस सम्बन्ध को सम्पन्न करने के लिये सूर्य और घट के संयोजकरूप में विभु काल का अभ्युपगम आवश्यक माना गया है । इस विषय में केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि सूर्यक्रिया के साथ घट का साक्षात् सम्बन्ध ही मान लेना चाहिये, उक्त परम्परासम्बन्ध की कल्पना अनावश्यक है, सूर्यक्रिया के साथ घर के स्वीकार्य साक्षात्सम्बन्ध को 'कालिक-विशेषणता' शब्द से व्यवहारयोग्य किया जा सकता है, यह सम्बन्ध अतिरिक्तकालवादी को भी मानना पड़ता है।
चालु शा. पा. १६