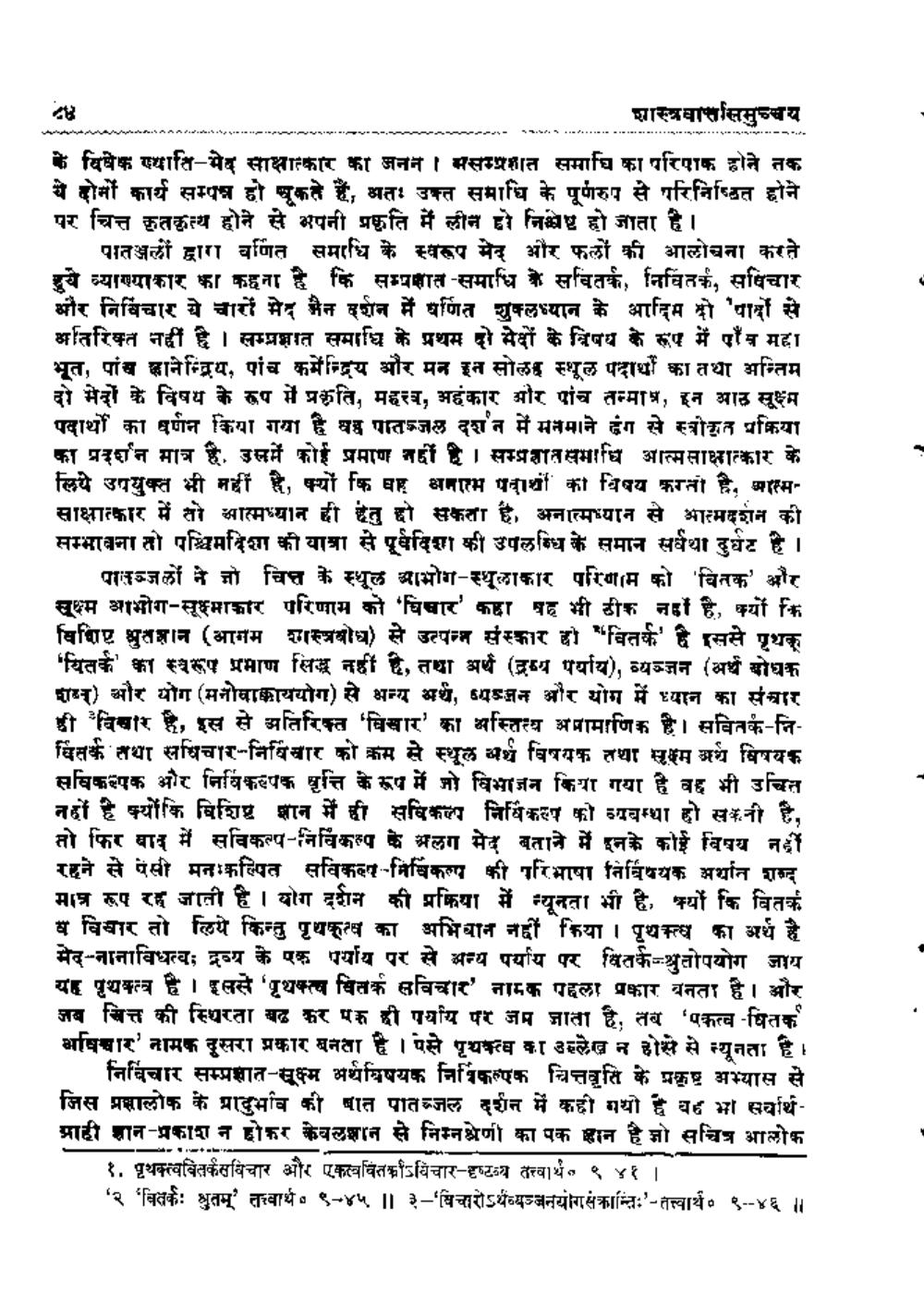________________
शास्त्रवातासमुच्चय के विधेक पथाति-मेव साक्षात्कार का जनन । मसम्मात समाधि का परिपाक होने तक ये दोनों कार्य सम्पन्न हो चूकते हैं, अतः उक्त समाधि के पूर्णरुप से परिनिष्ठित होने पर चित्त कृतकृत्य होने से अपनी प्रकृति में लीन हो निश्चेष्ट हो जाता है।
पातालों द्वारा वर्णित समाधि के स्वरूप मेद और फलों की आलोचना करते हुये व्याण्याकार का कहना है कि सम्पज्ञात-समाधि के सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार ये चारों मेद मैन दर्शन में धर्णित शुक्लध्यान के आदिम को 'पार्यों से अतिरिक्त नहीं है। सम्प्रभात समाधि के प्रथम दो मेदों के विषय के रूप में पात्र महा भूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कमेंन्द्रिय और मन इन सोलह स्थूल पदार्थों का तथा अन्तिम दो भेदों के विषय के रूप में प्रकृति, महत्व, अहंकार और पांच तन्मात्र, इन आठ सूक्ष्म पदार्थों का वर्णन किया गया है वह पातजल दर्शन में मनमाने ढंग से स्त्रोक्त प्रक्रिया का प्रदर्शन मात्र है, उसमें कोई प्रमाण नहीं है। सम्प्रशातसमाधि आत्मसाक्षात्कार के लिये उपयुक्त भी महीं है, क्यों कि वह अनारम पदार्थो को विषय करती है, मास्मसाक्षात्कार में तो आरमध्यान ही हेतु हो सकता है, अनात्मध्यान से आत्मदर्शन की सम्भावना तो पश्चिमदिशा की यात्रा से पूर्व दिशा की उपलब्धि के समान सर्वथा दुर्धट है।
पातञ्जलों ने जो चित्त के स्थूल आभोग-स्थूलाकार परिणाम को 'विनक' और सूक्ष्म आभोग-सूक्ष्माकार परिणाम को 'विचार' कहा यह भी ठीक नहीं है, क्यों कि विशिष्ट श्रुतशान (आगम शास्त्रबोध) से उत्पन्न संस्कार हो “वितर्क' है इससे पृथक "यितर्क' का स्वरूप प्रमाण सिद्ध नहीं है, तथा अर्थ (द्रव्य पर्याय), व्यञ्जन (अर्थ बोधक शान) और योग (मनोवाकाययोग) से अन्य अर्थ, ध्यजन और योग में ध्यान का संचार ही विचार है, इस से अतिरिक्त 'विसार' का अस्तित्व अप्रामाणिक है। सवितर्क-निवितर्क तथा सधिचार-निर्विचार को क्रम से स्थूल अर्थ विषयक तथा सूक्ष्म अर्थ विषयक सविकल्पक और निर्विकल्पक वृत्ति के रूप में जो विभाजन किया गया है वह भी उचित नहीं है क्योंकि विशिष्ट शान में ही सविकल्प निर्विकल्प को व्यवस्था हो सकती है, तो फिर बाद में सविकल्प-निर्विकल्प के अलग मेद बताने में इनके कोई विषय नहीं रहने से पसी मनःकल्पित सविकल्प-निर्विकल्प की परिभाषा निविषयक अर्थात शब्द मात्र रूप रह जाती है । योग दर्शन की प्रक्रिया में न्यूनता भी है, क्यों कि वितर्क व विचार तो लिये किन्तु पृथक्व का अभियान नहीं किया । पृथक्त्व का अर्थ है मेद-नानाविधत्वः द्रव्य के एक पर्याय पर से अन्य पर्याय पर वितर्क-श्रुतोपयोग जाय यह पृथक्त्व है। इससे 'पृथक्त्व वितर्क सविचार' नामक पहला प्रकार बनता है। और जब मित्त की स्थिरता बढ़ कर एक ही पर्याय पर जम जाता है, तब 'पकत्व -षितर्क भषिचार' नामक दूसरा प्रकार बनता है। पसे पृथक्त्व का उल्लेख न होसे से न्यूनता है।
निर्विचार सम्प्रज्ञात-सूक्ष्म अर्थविषयक निर्विकल्पक चित्तवृति के प्रकृष्ट अभ्यास से जिस प्रशालोक के प्रादुर्भाव की बात पातजल दर्शन में कही गयो हैयह भी सर्वार्थग्राही शान-प्रकाश न होकर केवलशान से निम्नश्रेणी का पक हान है जो सचित्र आलोक
१. पृथक्त्ववितर्कसविचार और एकत्ववितोऽविचार-दृष्टव्य तत्त्वार्थ० ९ ४१ । '२ "वितर्कः श्रुतम् तत्वार्थ ः ९-४५. ॥ ३-'विचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः'- तत्त्वार्थ० ९--४६ ।।