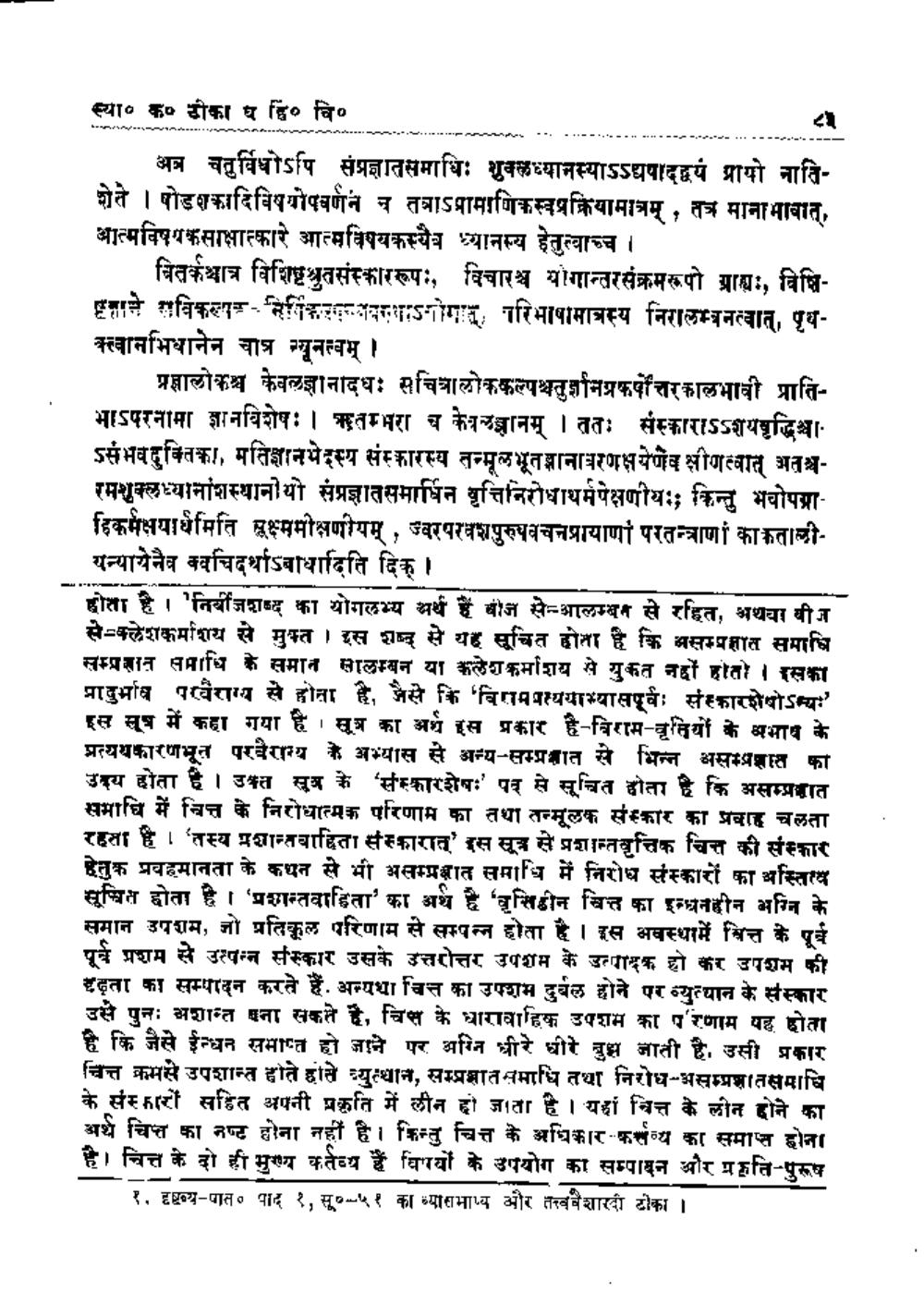________________
स्या० क. टीका घहिं० वि०
___ अत्र चतुर्विधोऽपि संप्रज्ञातसमाधिः शुक्लध्यानस्याऽऽद्यपादद्वयं प्रायो नातिशेते । पोडशकादिविषयोपवर्णन च तत्राऽप्रामाणिकस्वप्रक्रियामात्रम् , तत्र मानामावात, आत्मविषयकसाक्षात्कारे आत्मविषयकस्यैव ध्यानस्य हेतुत्वाच्च ।
वितर्कश्चात्र विशिष्टश्रुतसंस्काररूपः, विचारश्च योगान्तरसंक्रमरूपो प्रायः, विधिशाने विकलानिकलवायोगात, परिभाषामात्रस्य निरालम्बनत्वात्, पृथक्वाभिधानेन चार न्यूनत्वम् ।।
प्रज्ञालोकश्च केवलज्ञानादधः सचित्रालोककल्पश्चतुनिग्रकोत्तरकालभावी प्रातिभाऽपरनामा ज्ञानविशेषः । ऋतम्भरा च केवलज्ञानम् । ततः संस्काराऽऽशयवृद्धिश्चाऽसंभवदुक्तिका, मतिज्ञानदस्य संस्कारस्य तन्मूलभूतमानावरणक्षयेणेव क्षीणत्वात् अतश्चरमशुक्लध्यानांशस्थानोयो संप्रज्ञातसमार्धिन वृत्तिनिरोधाथमपेक्षणीयः; किन्तु भवोपनाहिकर्मक्षयामिति पूक्ष्ममोक्षणीयम् , ज्वरपरवशपुरुषवचनप्रायाणां परतन्त्राणां काकतालीयन्यायेनैव क्वचिदर्थाऽवाधादिति दिक् । होता है । 'नि:जशब्द का योगलभ्य अर्थ है बीज से-आलम्बन से रहित, अथवा वीज से-क्लेशकर्माशय से मुक्त । इस शब्द से यह सूचित होता है कि असम्प्रहात समाधि सम्प्रमात समाधि के समान सालम्बन या कलेशकर्माशय से युकत नहीं होतो । इसका प्रादुर्भाव परखैराग्य से होता है, जैसे कि 'विरामवस्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽभ्य' इस सूत्र में कहा गया है। सूत्र का अर्थ इस प्रकार है-विराम-वृतियों के प्रभाव के प्रत्ययकारणभूत परवैराग्य के अभ्यास से अन्य-सम्प्रभात से भिन्न असम्प्रशात का उदय होता है। उक्त सूत्र के संस्कारशेषः' पद से सूचित होता है कि असम्प्रशात समाधि में वित्त के निरोधात्मक परिणाम का तथा तन्मूलक संस्कार का प्रवाह चलता रहता है । 'तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्' इस सूत्र से प्रशान्तवृत्तिक चित्त की संस्कार हेतुक प्रवहमानता के कथन से भी असम्प्रक्षात समाधि में निरोध संस्कारों का अस्तित्व सूचित होता है। प्रशान्तवाहिता' का अर्थ है 'वृसिडीन वित्त का इन्धनहीन अग्नि के समान उपशम, जो प्रतिकूल परिणाम से सम्पन्न होता है । इस अवस्थामें वित्त के पूर्व पूर्व प्रशम से उत्पन्न संस्कार उसके उत्तरोत्तर उपशम के उत्पादक हो कर उपशम की दृढ़ता का सम्पादन करते हैं. अन्यथा चित्त का उपशम दुर्बल होने पर व्युत्थान के संस्कार उसे पुनः अशान्त बना सकते है, चिस के धारावाहिक उपशम का परिणाम यह होता है कि जैसे ईन्धन समाप्त हो जाने पर अग्नि धीरे धीरे बुझ जाती है, उसी प्रकार चित्त क्रमसे उपशान्त होते होते ब्युस्थान, सम्प्रभातसमाधि तथा निरोध-असम्प्रशातसमाधि के संस्कारों सहित अपनी प्रकृति में लीन हो जाता है। यहां चित्त के लीन होने का अर्थ चित्त का नष्ट होना नहीं है। किन्तु चित्त के अधिकार कर्तव्य का समाप्त होना है। चित्त के दो ही मुख्य कतव्य हैं विषयों के उपयोग का सम्पायन और प्रकृति-पुरूष
१. दृष्टव्य-पात ० पाद १, सू०.५१ का ध्यासमाप्य और तत्ववैशारदी टोका ।