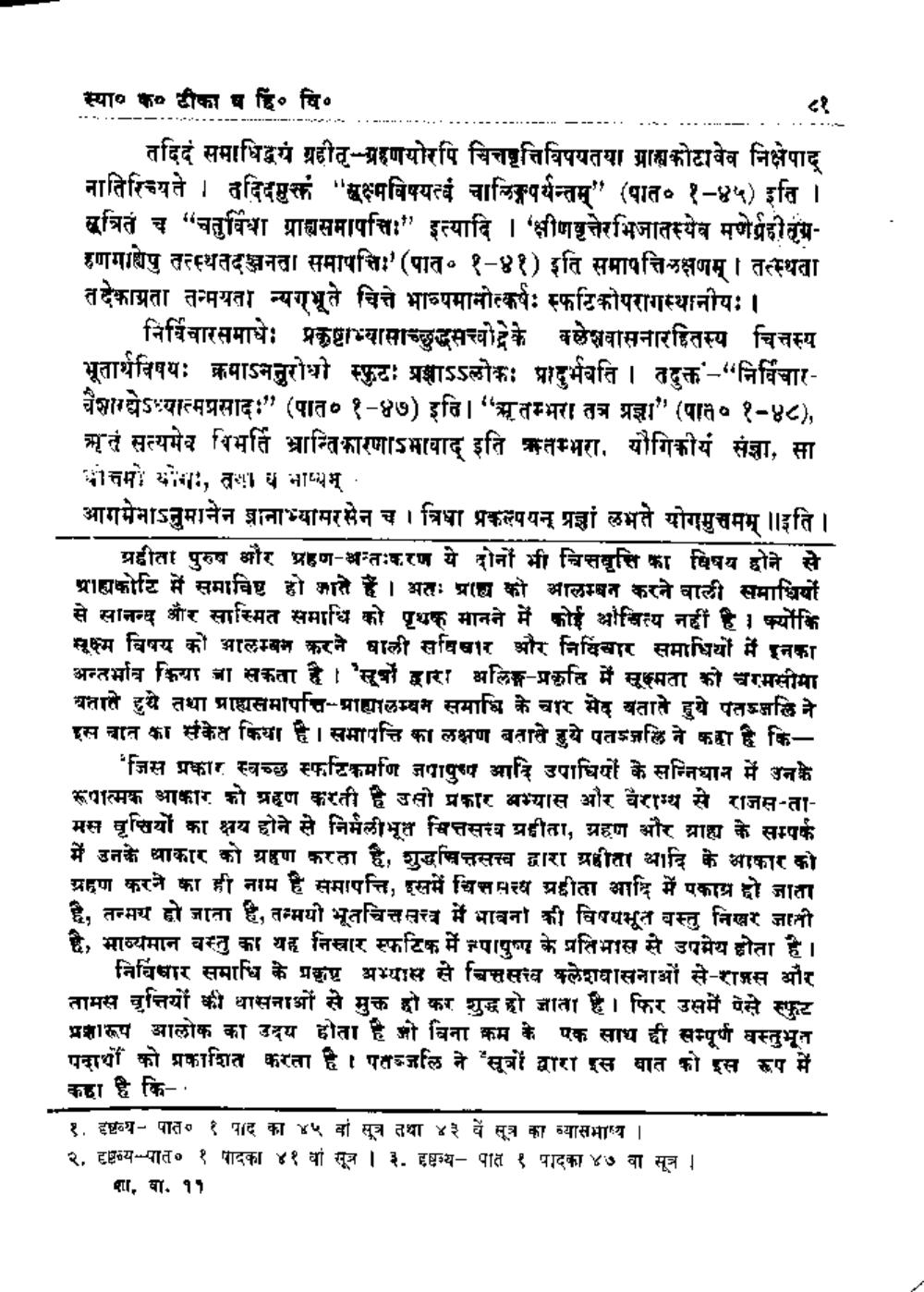________________
स्या० क० टीका बहि. वि.
___ तदिदं समाधिद्वयं ग्रहीत ग्रहणयोरपि वित्तवृत्तिविषयतया ग्राहकोटावेव निक्षेपाद् नातिरिच्यते । तदिदमुक्तं "सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यन्तम्" (पात. १-४५) इति । सूत्रितं च "चतुर्विधा ग्राह्यसमापत्ति" इत्यादि । क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेही तनहणगापु तत्स्थतदानता समापत्तिः (पात. १-४१) इति समापत्तिलक्षणम् । तत्स्थता तदेकाग्रता तन्मयता न्यगभूते चित्ते भाव्यमानोत्कर्षः स्फटिकोपरागस्थानीयः।।
__ निर्विचारसमाधेः प्रकृष्टाभ्यासाच्छुद्धसत्वोनेके क्लेशवासनारहितस्य चित्तस्य भूतार्थविषयः क्रमाऽननुरोधो स्फुटः प्रज्ञाऽऽलोकः प्रादुर्भवति । तदुक्त'-"निर्विचारचैशारोऽध्यात्मप्रसाद:" (पात०१-४७) इति । "ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा" (पात ०१-४८), अतं सत्यमेव बिभर्ति भ्रान्तिकारणाऽभावाद् इति ऋतम्भरा. यौगिकीयं संज्ञा, सा पोत्तमो योगः, तथा व नाप्यम् । आगमेनाऽनुमानेन बानाभ्यामरसेन च । त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम् ।।इति ।
प्रहीता पुरुष और ग्रहण-अन्तःकरण ये दोनों भी चिप्सवृत्ति का विषय होने से प्राह्यकोटि में समाविष्ट हो जाते हैं। अतः प्राख को आलम्बन करने वाली समाधियों से सानन्द और सास्मित समाधि को पृथक मानने में कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि सूक्ष्म विषय को आलम्बन करने वाली सविखार और निर्विचार समाधियों में इनका अन्तर्भाव किया जा सकता है। सूत्रों द्वारा अलिस-प्रकृति में सूक्ष्मता को चरमसीमा बताते हुये तथा प्राह्यसमात्ति-प्राह्मालम्बम समाधि के चार मेद बताते हुये पतञ्जलि ने इस बात का संकेत किया है। समापत्ति का लक्षण बताते हुये पतझजलि ने कहा है कि
_ 'जिस प्रकार स्वच्छ स्फटिकर्माण जपापुष्प आदि उपाधियों के सन्निधान में उनके रूपात्मक आकार को ग्रहण करती है उसी प्रकार अभ्यास और वैराग्य से राजस-तामस वृसियों का क्षय होने से निर्मलीभूत पित्तसत्त्व प्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य के सम्पर्क में उनके आकार को ग्रहण करता है, शुद्धचित्तसत्व द्वारा ग्रहीता आदि के आकार को ग्रहण करने का ही नाम है समापत्ति, इसमें चिसय ग्रहीता आदि में पकान हो जाता है, तन्मय हो जाता है, तन्मयो भूतचित्त सत्व में भावना की विषयभूत वस्तु निखर जाती है, भाव्यमान वस्तु का यह निसार स्फटिक में उपायुष्ण के प्रतिभास से उपमेय होता है।
निर्विधार समाधि के प्रकृष्ट अभ्यास से चिप्ससत्व कलेशवासनाओं से-राजस और तामस वृत्तियों की धासनाओं से मुक्त हो कर शुद्ध हो जाता है। फिर उसमें पेसे स्फुट प्रशारूप आलोक का उदय होता है जो विना क्रम के पक साथ ही सम्पूर्ण वस्तुभूत पदार्थों को प्रकाशित करता है । पतञ्जलि ने सूत्रों द्वारा इस बात को इस रूप में कहा है कि१. दृष्टव्य- पातर १ पाद का ४५ वां सूत्र तथा ४३ वे सूत्र का व्यासभाष्य । २. दृष्टस्य पात० १ पादका ४१ वां सूत्र । ३. दृष्टश्य- पात १ पादका ४७ वा सूत्र ।
शा, वा. "