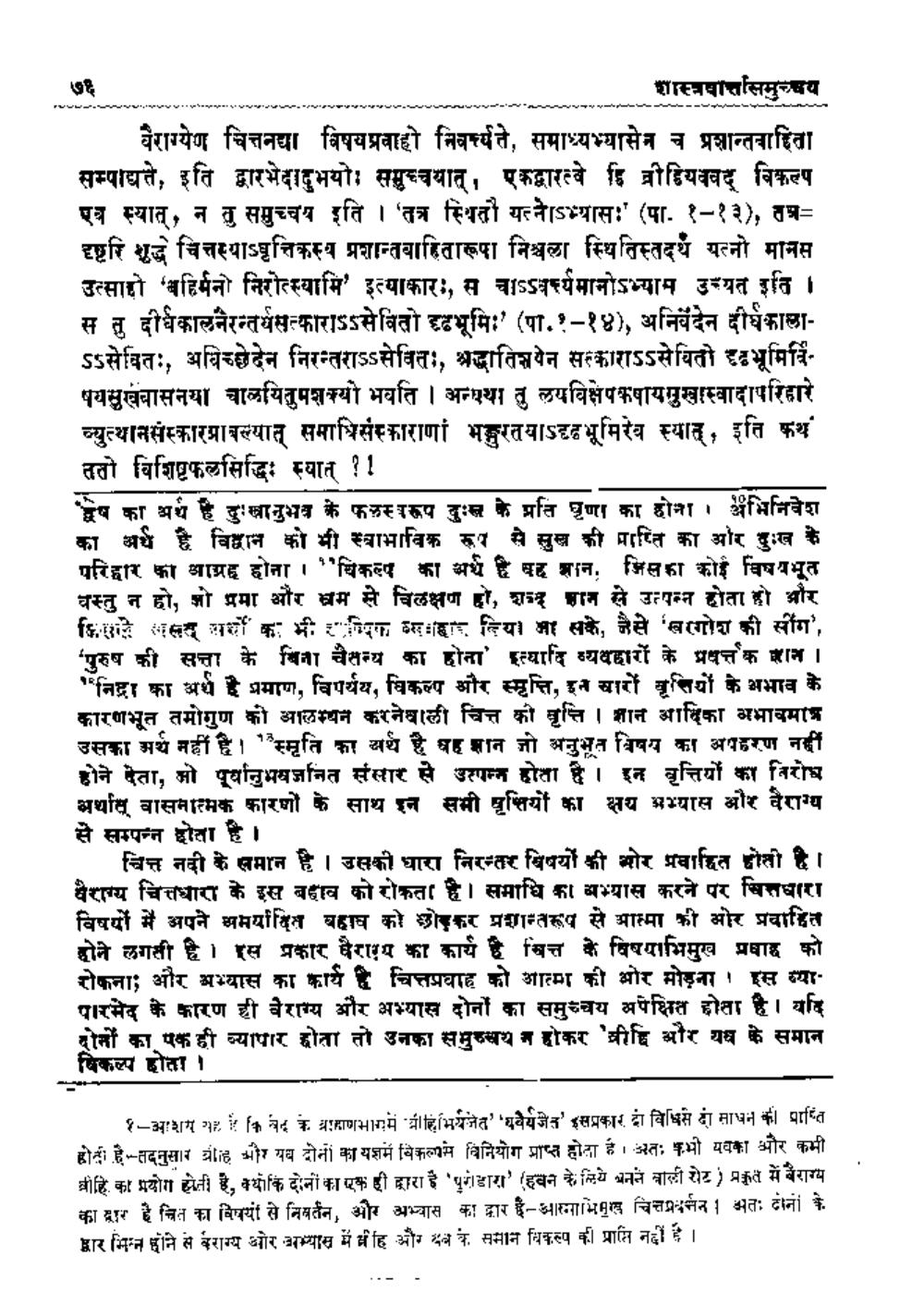________________
७६
शास्त्रवासिमुच्चय वैराग्येण चित्तनद्या विषयप्रवाहो निवर्य ते, समाध्यभ्यासेन च प्रशान्तवाहिता सम्पाद्यते, इति द्वारभेदादुभयोः समुच्चयात् । एकद्वारत्वे हि वीडियववद् विकल्प एवं स्यात्, न तु समुच्चय इति । 'तत्र स्थितौ यत्नेोऽभ्यासः' (पा. १-१३), तत्र दृष्टरि शुद्ध चित्तस्याऽवृत्तिकस्य प्रशान्तवाहितारूपा निश्चला स्थितिस्तदर्थ यत्नो मानस उत्साहो 'बहिर्मनो निरोत्स्यामि' इत्याकारः, स चाऽऽवय॑मानोऽभ्याम उच्यत इति । स तू दीर्घकालनरन्तयसत्काराऽऽसेवितो दृढभूमिः' (पा.१-१४), अनिदेन दीर्घकालाऽऽसेवितः, अविच्छेदेन निरन्तराऽऽसेवितः, श्रद्धातिशयेन सत्काराऽऽसेवितो दृढभूमिर्विषयसुखवासनया चालयितुमशक्यो भवति । अन्श्या तु लयविक्षेपकषायमुखास्वादापरिहारे व्युत्थानसंस्कारप्राबल्यात् समाधिसंस्काराणां भरतयाऽदृढभूमिरेव स्यात्, इति कथं ततो विशिष्टफलसिद्धिः स्यात् ? ! द्वष का अर्थ है दुःखानुभव के फलस्वरूप दुःस्त्र के प्रति घृणा का होना । अभिनिवेश का अर्थ है विज्ञान को भी स्वाभाविक रूप से सुख की प्राप्ति का और इसके परिहार का आग्रह होना । "विकल्प का अर्थ है यह शान, जिसका कोई विषयभूत वस्तु न हो, जो प्रमा और भ्रम से विलक्षण हो, शमशान से उत्पन्न होता हो और किराने मला माझे का भी कि साहाय लिया जा सके, जैसे खरगोश की सींग', 'पुरुष की सत्ता के बिना चैतन्य का होना इत्यादि व्यवहारों के प्रवर्तक हान | "निद्रा का अर्थ है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और स्मृत्ति, इन चारों वृत्तियों के अभाव के कारणभूत तमोगुण को आलम्थन करनेवाली चित्त की वृत्ति । शान आदिका अभावमात्र उसका अर्थ नहीं है। स्मृति का अर्थ है यह मान जो अनुभत विषय का अपहरण नहीं होने देता, जो पूर्वानुभवजनित संसार से उत्पन्न होता है। इन वृत्तियों का विरोध अर्थात् वासनात्मक कारणों के साथ इन समी पृत्तियों का क्षय अभ्यास और वैराग्य से सम्पन्न होता है।।
चित्त नदी के समान है। उसकी धारा निरन्तर विषयों की भोर प्रवाहित होती है। वैराग्य चित्तधारा के इस बहाव को रोकता है। समाधि का अभ्यास करने पर चिसधारा विषयों में अपने अमर्यादित बहाथ को छोड़कर प्रशान्तरूप से आस्मा की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार बैराश्य का कार्य है बित्त के विषयाभिमुख प्रवाह को रोकना; और अभ्यास का कार्य है चित्तप्रवाह को आत्मा की ओर मोड़ना । इस व्या. पारमेद के कारण ही वैराग्य और अभ्यास दोनों का समुच्चय अपेक्षित होता है। यदि दोनों का एक ही व्यापार होता तो उनका समुच्चयन होकर 'बीहि और यव के समान विकल्प होता।
१-आशय किवद के बाहाणभागमें बाहिभिर्यजेत' 'यवैर्यजेत' इसप्रकार दा विधिसे दो माधन की प्राप्ति होती है तदनुसार बौह और यब दोनों का यज्ञमें विकलामे विनियोग प्राप्त होता है। अतः कभी यवका और कभी व्रीहि. का प्रयोग होती है, क्योंकि दोनों का एक ही द्वारा है 'घुरोडारा हवन के लिये बनने वाली रोट) प्रकृत में वैराग्य । का दार है चित का विषयों से निवर्तन, और अभ्यास का द्वार ई-आगाममुख चित्तप्रवनन । अतः दोनों के द्वार भिन्न होने से वैराग्य ओर अभ्यास में हि और व कं. समान विकल्प की प्राप्ति नहीं है।