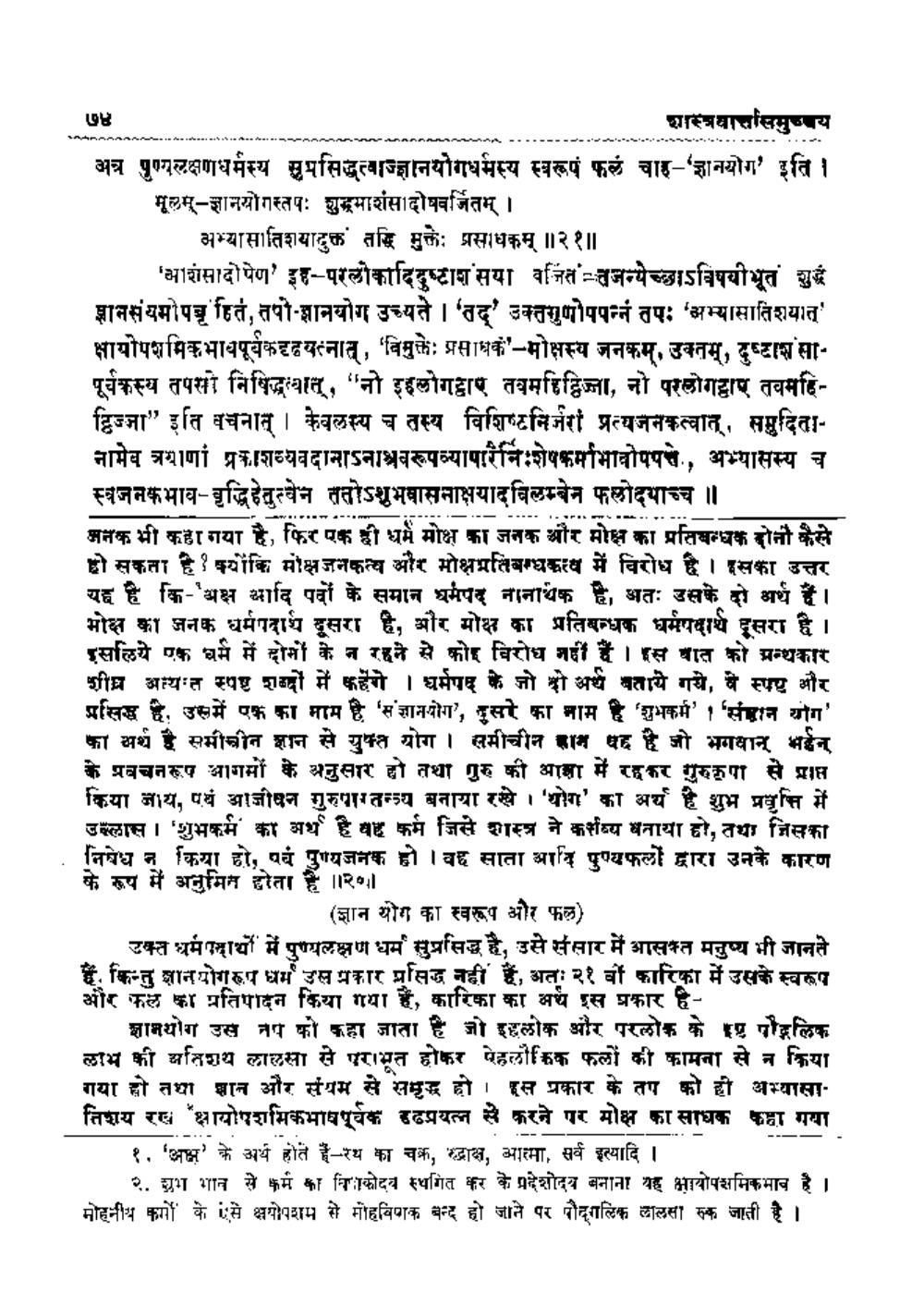________________
७४
अत्र पुण्यलक्षणधर्मस्य
शास्त्रवातसमुच्चय
प्रसिद्धत्वाज्ज्ञानयोगधर्मस्य स्वरूपं फलं चाह - 'ज्ञानयोग' इति ।
मूलम् - ज्ञानयोगस्तपः शुद्धमाशंसा दोषवर्जितम् ।
अभ्यासातिशयदुक्तं तद्धि मुक्तेः प्रसाधकम् ॥ २१॥
'आशंसादोपेण' इह-परलोकादिदुष्टाशंसया वजित राजन्येच्छाऽविषयीभूतं शुद्धं ज्ञानसंयमोपच हितं तपो ज्ञानयोग उच्यते । 'तद्' उक्तगुणोपपन्नं तपः 'अभ्यासातिशयात्' क्षायोपशमिकभावपूर्वक दृढ यत्नात्, 'विमुक्तेः प्रसाधक' - मोक्षस्य जनकम्, उक्तम्, दुष्टाशंसापूर्वकस्य तपसो निषिद्धत्वात्, "नो इहलोगद्वार तवमहिद्विज्जा, नो परलोगहाए तवमहिहिज्जा" इति वचनात् । केवलस्य च तस्य विशिष्ट निर्जरां प्रत्यजनकत्वात्, समुदितानामेव त्रयाणां प्रकाशव्यवदानाऽनाश्रवरूपव्यापारैर्निःशेषकर्माभावोपपते, अभ्यासस्य च स्वजनकभाव- वृद्धिहेतुत्वेन ततोऽशुभवासनाक्षयाद विलम्बेन फलोदयाच्च ॥
अनक भी कहा गया है, फिर एक ही धर्मे मोक्ष का जनक और मोक्ष का प्रतिबन्धक दोनों कैसे हो सकता है? क्योंकि मोक्षजनकत्व और मोक्षप्रतिबन्धकत्व में विरोध है । इसका उत्तर यह है कि- 'अक्ष आदि पदों के समान धर्मपद नानार्थक है, अतः उसके दो अर्थ हैं । मोक्ष का जनक धर्मार्थ दूसरा है, और मोक्ष का प्रतिबन्धक धर्मपदार्थ दूसरा है । इसलिये एक धर्म में दोनों के न रहने से कोई विरोध नहीं हैं। इस बात को ग्रन्थकार शीघ्र अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कहेंगे । धर्मपद के जो दो अर्थ बताये गये, वे स्पष्ट और प्रसिद्ध है, उसमें एक का नाम है 'संज्ञानयोग', दुसरे का नाम है 'शुभकर्म' ' 'संज्ञान योग' का अर्थ है समीचीन ज्ञान से युक्त योग । समीचीन हाथ वह है जो भगवान् भईन् के प्रवचनरूप आगमों के अनुसार हो तथा गुरु की आज्ञा में रहकर गुरुकृपा से प्राप्त किया जाय, पथं आजीवन गुरुप्राग्तव्य बनाया रखे । 'योग' का अर्थ है शुभ प्रवृति में उक्लास | 'शुभकर्म का अर्थ है वह कर्म जिसे शास्त्र ने कर्तव्य बनाया हो, तथा जिसका निषेध न किया हो, पवं पुण्यजनक हो । वह साता आदि पुण्यफलों द्वारा उनके कारण के रूप में अनुमित होता है ॥२॥
(ज्ञान योग का स्वरूप और फल )
उक्त धर्मार्थों में पुण्यलक्षण धर्म सुप्रसिद्ध है, उसे संसार में आसक्त मनुष्य भी जानते हैं. किन्तु ज्ञानयोगरूप धर्म इस प्रकार प्रसिद्ध नहीं हैं, अतः २१ वीं कारिका में उसके स्वरूप और फल का प्रतिपादन किया गया हैं, कारिका का अर्थ इस प्रकार है
ज्ञानयोग उस नप को कहा जाता है जो इहलोक और परलोक के
पौलिक
लाभ की अतिशय लालसा से पराभूत होकर ऐहलौकिक फलों की कामना से न किया गया हो तथा ज्ञान और संयम से समृद्ध हो । इस प्रकार के तप को ही अभ्यासातिशय रख क्षायोपशमिकभावपूर्वक उढप्रयत्न से करने पर मोक्ष का साधक कहा गया
१. 'अम' के अर्थ होते हैं - रथ का चक्र, द्राक्ष, आत्मा, सर्व इत्यादि ।
२. शुभ भाव से कर्म का विकोदव स्थगित कर के प्रदेशोदय बनाना यह भायोपशमिकभाव है । मोहनीय कर्मों के ऐसे क्षयोपशम से मोहविक बन्द हो जाने पर बौद्गलिक लालसा रुक जाती है ।