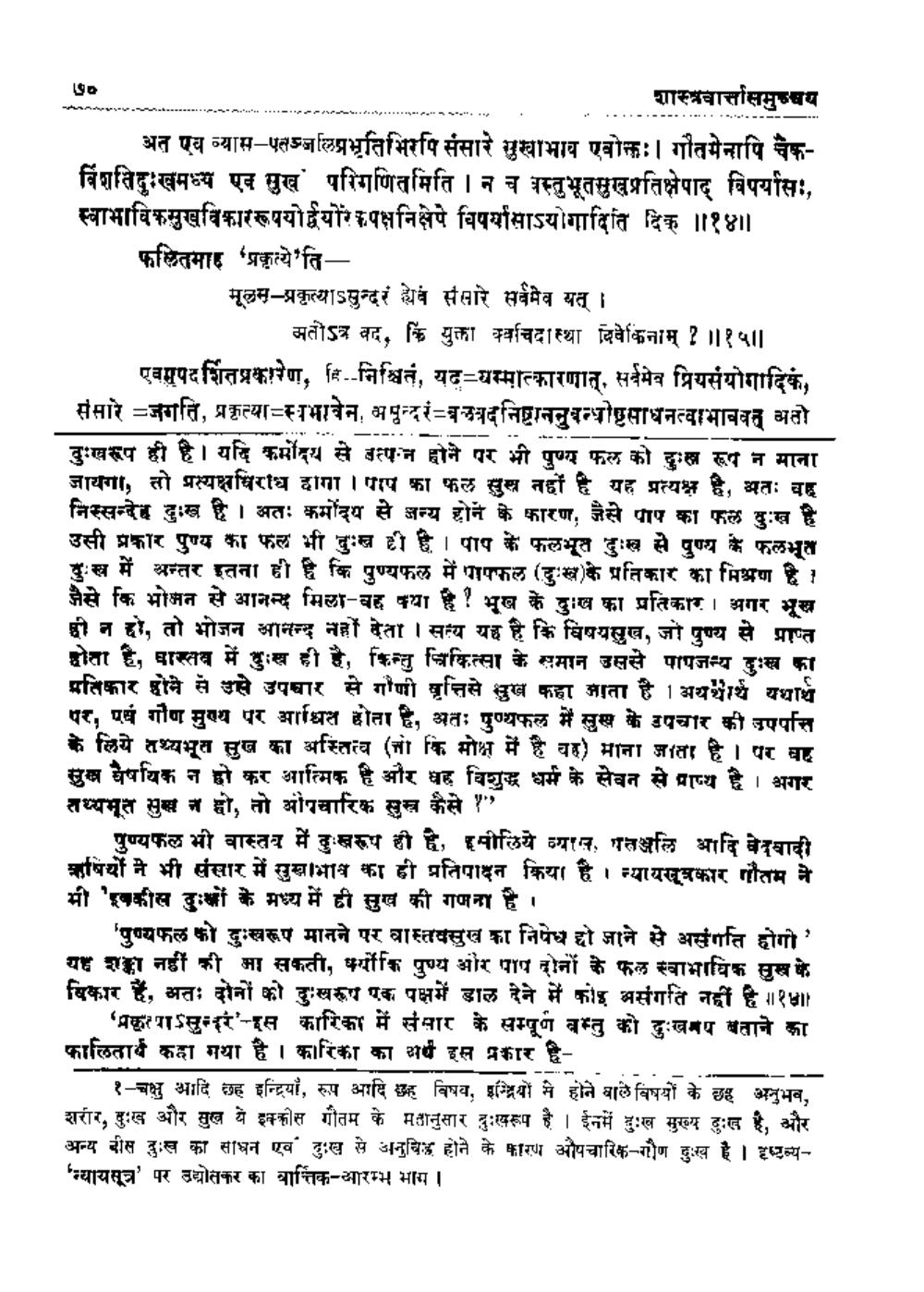________________
शास्त्रवार्तासमुच्चय अत एव व्यास–पतञ्जलिप्रभृतिभिरपि संसारे सुखाभाव एवोक्तः। गौतमेनापि चैकविंशतिदुःखमध्य एव सुख परिगणितमिति | न च वस्तुभूतमुखप्रतिक्षेपाद् विपर्यासः, स्वाभाविकमुखविकाररूपयोईयों कपक्षनिक्षेपे विपर्यासाऽयोगादिति दिक् ॥१४॥ फलितमाह 'प्रकृत्ये'ति__मूलम-प्रकृत्याऽसुन्दरं ह्येवं संसारे सर्वमेव यत् ।
मतोऽत्र वद, किं युक्ता क्वचिदास्था दिकिनाम् ? |१५|| एवमुपदर्शितप्रकारेण, हि-निश्चितं, यद-यस्मात्कारणात्, सर्वमेव प्रियसंयोगादिक, संसारे =जगति, प्रकृत्या स्वभावेन. अ पुन्दरं-बलबदनिष्टाननुबन्धोष्टसाधनत्वाभाववत् अतो दुःखरूप ही है। यदि कर्मोदय से उत्पन होने पर भी पुण्य फल को दुःस्त्र रूप न माना जायगा, तो प्रत्यक्षविरोध दागा । पाप का फल सुत्र नहीं है यह प्रत्यक्ष है, अतः वह निस्सन्देह दुःख है। अतः कमोदय से जन्य होने के कारण, जैसे पाप का फल दुःख है उसी प्रकार पुण्य का फल भी 'दुःख ही है। पाप के फलभूत दुःख से पुण्य के फलभूत दुःख में अन्तर इतना ही है कि पुण्यफल में फ्फल (दुःख)के प्रतिकार का मिश्रण है। जैसे कि भोजन से आनन्द मिला-वह क्या है। भूख के दुःख का प्रतिकार । अगर भूख छी न हो, तो भोजन आनन्द नहीं देता । सत्य यह है कि विषयसुख, जो पुण्य से प्राप्त होता है, पास्तव में दुःख ही है, किन्तु चिकित्सा के समान उससे पापजन्य दुःस्त्र का प्रतिकार होने से उसे उपचार से गौणी वृत्तिसे सुख कहा आता है 1 अयथार्थ यथार्थ पर, पथं गौण मुख्य पर आश्रित होता है, अतः पुण्यफल में सुख के उपचार की उपास के लिये तथ्यभूत सुख का अस्तित्व (जो कि मोक्ष में है वह) माना जाता है। पर वह सुख वैषयिक न हो कर आत्मिक है और वह विशुद्ध धर्म के सेवन से प्राप्य है। अगर तथ्यभूत सुख न हो, तो औपचारिक सुख कैसे ?"
पुण्यफल भी वास्तव में दुःखरूप ही है, इसीलिये व्यास, पतञ्जलि आदि वेदवादी ऋषियों ने भी संसार में सुस्वाभाव का ही प्रतिपादन किया है। न्यायसूत्रकार गौतम ने भी 'इक्कीस दुःखों के मध्य में ही सुख की गणना है ।
'पुण्यफल को दुःखरूप मानने पर वास्तवसुख का निषेध हो जाने से असंगति होगी' यह शक नहीं की मा सकती, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों के फल स्वाभाविक सुख के विकार हैं, अतः दोनों को दुःखरूप एक पक्षमें डाल देने में कोइ असंगति नहीं है ॥१४॥
'प्रकरयाऽसुन्दरं' इस कारिका में संसार के सम्पूर्ण वस्तु को दुःखमय बताने का फालितार्थ कहा गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है
१-चक्षु आदि छह इन्द्रियाँ, रुप अगदि छह विषव, इन्द्रियों मे होने वाले विषयों के छह अनुभव, शरीर, दुःख और सुख ये इसकोस गौतम के मतानुसार दुःरयरूप है । ईनमें दुःख मुख्य दुःख है, और अन्य चीस दुःख का साधन एवं दुःख से अनुचित होने के कारण औपचारिक-गौण दुःख है । दृष्टव्य'न्यायसूत्र' पर उद्योतकर का बार्तिक-आरम्भ भाय ।