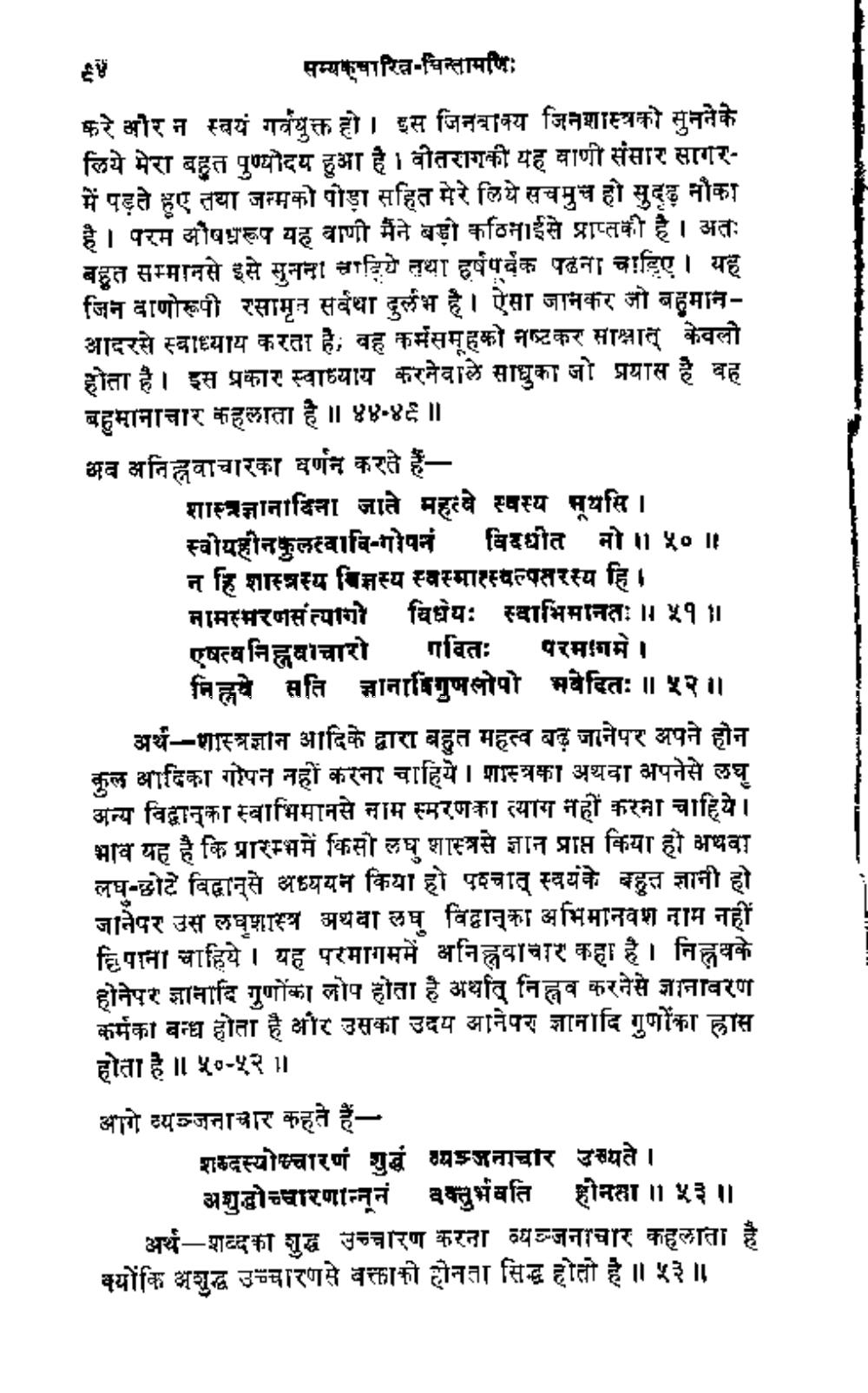________________
सम्यक्चारित्र-चिन्तामणिः
करे और न स्वयं गर्वयुक्त हो। इस जिनवाक्य जिनशास्त्रको सुनने के लिये मेरा बहुत पुण्योदय हुआ है। वीतरागकी यह वाणी संसार सागरमें पढ़ते हुए तथा जन्मको पोड़ा सहित मेरे लिये सचमुच हो सुदृढ नौका है । परम औषधरूप यह वाणी मैंने बड़ी कठिनाईसे प्राप्तकी है। अतः बहुत सम्मान से इसे सुनना चाहिये तथा हर्षपूर्वक पढना चाहिए। यह जिन दाणोरूपी रसामृत सर्वथा दुर्लभ है। ऐसा जानकर जो बहुमानआदरसे स्वाध्याय करता है; वह कर्मसमूहको नष्टकर साक्षात् केवली होता है । इस प्रकार स्वाध्याय करनेवाले साधुका जो प्रयास है वह बहुमानाचार कहलाता है ॥ ४४-४६ ॥
अव अह्निवाचारका वर्णन करते हैं
शास्त्रज्ञानादिना जाते महत्वे स्वस्य सूयसि । स्वयहीन कुलस्वावि-गोपनं विदधीत नो ॥ ५० ॥
न हि शास्त्रस्य विज्ञस्य स्वस्मात्स्वल्पतरस्य हि । नामस्मरणसं त्यागी विधेयः स्वाभिमानतः ॥ ५१ ॥
गवितः परमागमे ।
एषत्व निवाचारो मिलये सति जानादिगुणलोपो भवेदितः ।। ५२ ।। अर्थ - शास्त्रज्ञान आदिके द्वारा बहुत महत्व बढ़ जानेपर अपने होन कुल आदिका गोपन नहीं करना चाहिये । शास्त्रका अथवा अपनेसे लघु अन्य विद्वानका स्वाभिमानसे नाम स्मरणका त्याग नहीं करना चाहिये । भाव यह है कि प्रारम्भ में किसी लघु शास्त्रसे ज्ञान प्राप्त किया हो अथवा लघु-छोटे विद्वान् से अध्ययन किया हो पश्चात् स्वयंके बहुत ज्ञानी हो जानेपर उस लघुशास्त्र अथवा लघु विद्वान्का अभिमानवश नाम नहीं छिपाना चाहिये। यह परमागममें अनिवाचार कहा है । निह्नवके होनेपर ज्ञानादि गुणोंका लोप होता है अर्थात् निह्नव करनेसे ज्ञानावरण कर्मका बन्ध होता है और उसका उदय आनेपर ज्ञानादि गुणोंका ह्रास होता है ।। ५०-५२ ॥
आगे व्यञ्जनाचार कहते हैं
शब्दस्योच्चारणं शुद्धं व्यञ्जनाचार उच्यते । अशुद्धोच्चारणान्नूनं वक्तुर्भवति होनता ॥ ५३ ॥
अर्थ - शब्दका शुद्ध उच्चारण करना व्यञ्जनाचार कहलाता क्योंकि अशुद्ध उच्चारणसे वक्ता की होनता सिद्ध होतो है ॥ ५३ ॥