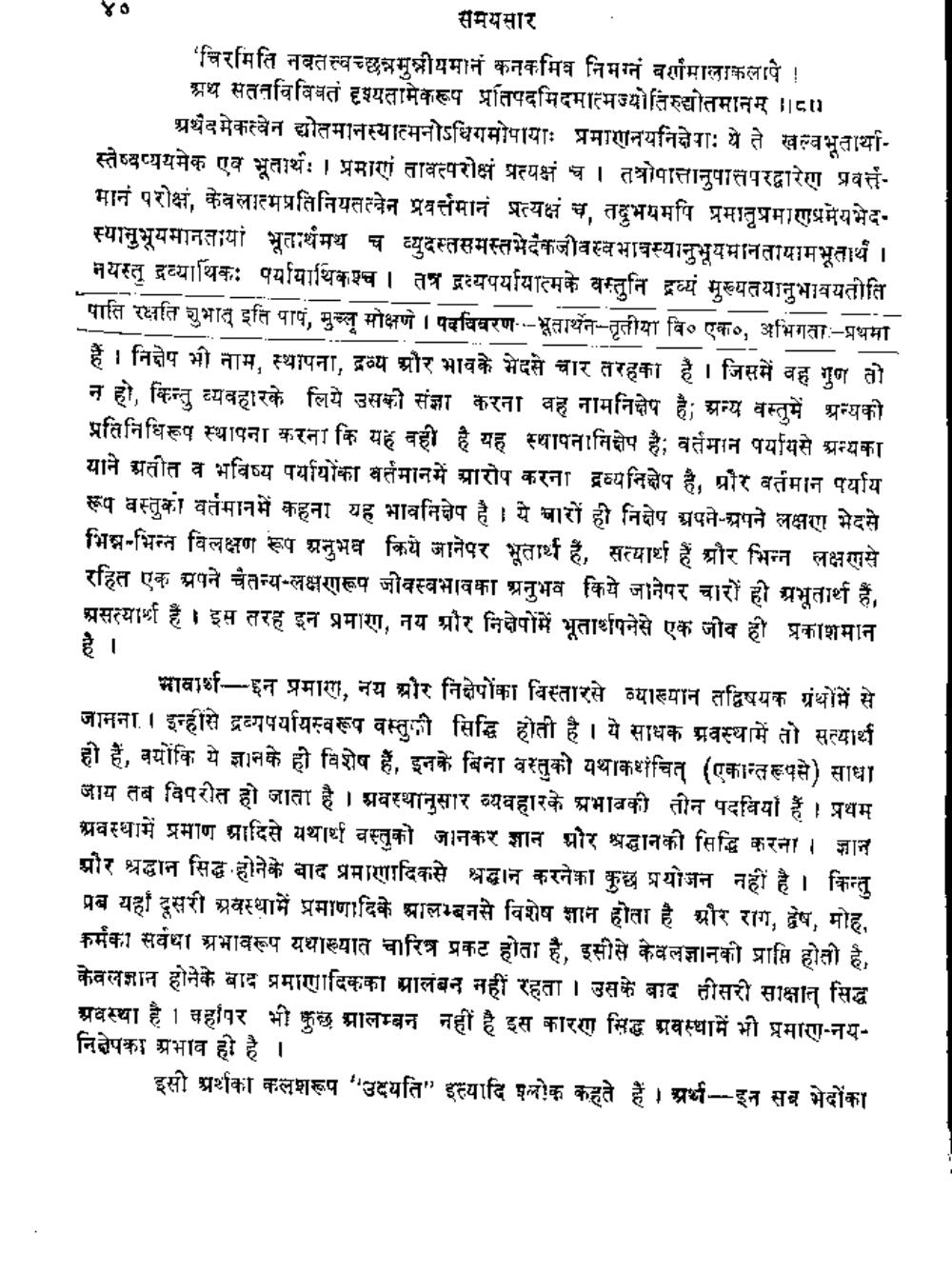________________
समयसार
'चिरमिति नवतस्वच्छन्नमुन्नीयमानं कनकमिव निमग्नं वर्णमालाकलापे ! अथ सततविविवतं दृश्यतामेकरूप प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरुद्योतमानम् ॥८॥
प्रथैवमेकत्वेन द्योतमानस्यात्मनोऽधिगमोपायाः प्रमाणनयनिक्षेपाः ये ते खल्वभूतार्थास्तेष्वप्ययमेक एव भूतार्थः । प्रमाणं तावत्परोक्षं प्रत्यक्षं च । तत्रोपात्तानुपात्तपरद्वारेण प्रवर्तमानं परोक्षं, केवलात्मप्रतिनियतत्वेन प्रवर्तमान प्रत्यक्षं च, तदुभयमपि प्रमातृप्रमाणप्रमेयभेदस्यानुभूयमानतायां भूतार्थमथ च व्युदस्तसमस्तभेदैकजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायामभूतार्थं । नयस्तु द्रव्याथिकः पर्यायाथिकश्च । तत्र द्रव्यपर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यं मुख्यतयानुभावयतीति पाति रक्षति शुभात् इति पापं, मुख्लु मोक्षणे । पदविवरण---भूतार्थेन-तृतीया वि० एक०, अभिगताः-प्रथमा हैं । निक्षेप भी नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे चार तरहका है । जिसमें वह गुण तो न हो, किन्तु व्यवहारके लिये उसको संज्ञा करना वह नामनिक्षेप है; अन्य वस्तुमें अन्यको प्रतिनिधिरूप स्थापना करना कि यह वही है यह स्थापनानिक्षेप है; वर्तमान पर्यायसे अन्यका याने अतीत व भविष्य पर्यायोंका वर्तमानमें आरोप करना द्रध्यनिक्षेप है, और वर्तमान पर्याय रूप वस्तुको वर्तमान में कहना यह भावनिक्षेप है । ये चारों ही निक्षेप अपने-अपने लक्षण भेदसे भिन्न-भिन्न विलक्षण रूप अनुभव किये जानेपर भूतार्थ हैं, सत्यार्थी हैं और भिन्न लक्षणसे रहित एक अपने चैतन्य लक्षणरूप जीवस्वभावका अनुभव किये जानेपर चारों ही अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। इस तरह इन प्रमाण, नय और निक्षेपोंमें भूतापिनेसे एक जीव ही प्रकाशमान
भावार्थ-इन प्रमाण, नय और निक्षेपोंका विस्तारसे व्याख्यान तद्विषयक ग्रंथों में से जामना । इन्हींसे द्रव्यपर्यायस्वरूप वस्तुकी सिद्धि होती है । ये साधक अवस्थामें तो सत्यार्थ ही हैं, क्योंकि ये ज्ञान के हो विशेष हैं, इनके बिना वस्तुको यथाकचित् (एकान्तरूपसे) साधा जाय तब विपरीत हो जाता है । अवस्थानुसार व्यवहारके प्रभावकी तीन पदवियों हैं। प्रथम अवस्थामें प्रमाण प्रादिसे यथार्था वस्तुको जानकर ज्ञान और श्रद्धानकी सिद्धि करना । ज्ञान पौर श्रद्धान सिद्ध होनेके बाद प्रमाणादिकसे श्रद्धान करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। किन्तु प्रब यहाँ दूसरी अवस्थामें प्रमाणादिके पालम्बनसे विशेष ज्ञान होता है और राग, द्वेष, मोह, कर्मका सर्वथा अभावरूप यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है, इसीसे केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है, केवलज्ञान होनेके बाद प्रमाणादिकका ग्रालंबन नहीं रहता। उसके बाद तीसरी साक्षात् सिद्ध अवस्था है । वहाँपर भी कुछ मालम्बन नहीं है इस कारण सिद्ध अवस्थामें भी प्रमाण-नयनिक्षेपका प्रभाव ही है ।
इसी अर्शका कलशरूप "उदयति" इत्यादि श्लोक कहते हैं । अर्थ--इन सर भेदोंका