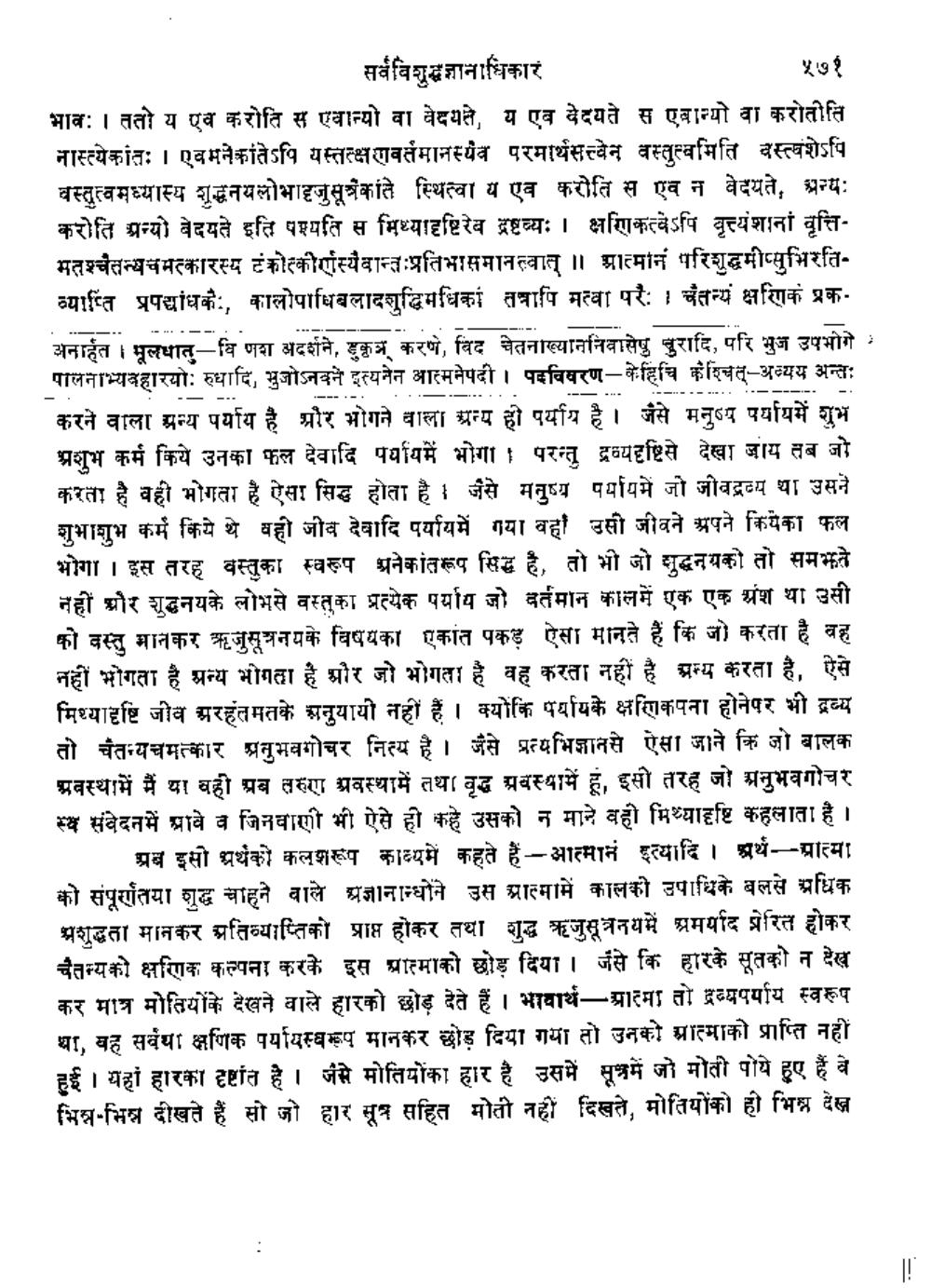________________
५.७१
सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार भावः । ततो य एवं करोति स एवान्यो वा वेदयते, य एव वेदयते स एवान्यो वा करोतीति नास्त्येकांतः । एवमनेकांतेऽपि यस्तत्क्षणवर्तमानस्येव परमार्थसत्त्वेन वस्तुत्वमिति वस्त्वंशेऽपि वस्तुत्वमध्यास्य शूद्धनयलोभाहजुसूत्रकांते स्थित्वा य एव करोति स एव न वेदयते, अन्यः करोति अन्यो बेदयते इति पश्यति स मिथ्यादृष्टि रेब द्रष्टव्यः । क्षणिकत्वेऽपि वृत्त्यशानां वृत्तिमतश्चैतन्यचमत्कारस्य टंकोत्कीर्णस्यैवान्तःप्रतिभासमानत्वात् ॥ प्रात्मानं परिशुद्धमीप्सुभिरतिव्याप्ति प्रपद्यांधकः, कालोपाधिबलादशुद्धिमधिका तत्रापि मत्वा परैः । चैतन्यं क्षणिक प्रक. अनाहत । मूलधातु-वि णश अदर्शने, डुकृञ् करणे, विद चेतनाख्याननिवासेषु चुरादि, परि भुज उपभोगे । पालनाभ्यवहारयोः रुधादि, मुजोऽनवने इत्यनेन आत्मनेपदी। पदविवरण-केचि कैश्चित्-अव्यय अन्तः करने वाला अन्य पर्याय है और भोगने वाला अन्य ही पर्याय है। जैसे मनुष्य पर्यायमें शुभ प्रशुभ कर्म किये उनका फल देवादि पर्यायमें भोगा। परन्तु द्रव्यदृष्टिसे देखा जाय तब जो करता है वही भोगता है ऐसा सिद्ध होता है । जैसे मनुष्य पर्यायमें जो जीवद्रव्य था उसने शुभाशुभ कर्म किये थे वही जीव देवादि पर्याय में गया वहाँ उसी जीवने अपने कियेका फल भोगा । इस तरह वस्तुका स्वरूप अनेकांतरूप सिद्ध है, तो भी जो सुद्धनको तो समझते नहीं और शुद्धनयके लोभसे वस्तुका प्रत्येक पर्याय जो वर्तमान काल में एक एक अंश था उसी को वस्तु मानकर ऋजुसूत्रनय के विषयका एकांत पकड़ ऐसा मानते हैं कि जो करता है वह नहीं भोगता है अन्य भोगता है और जो भोगता है वह करता नहीं है अन्य करता है, ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव अरहंत मतके अनुयायी नहीं हैं। क्योंकि पर्यायके क्षणिकपना होनेपर भी द्रव्य तो चैतन्यचमत्कार अनुभवगोचर नित्य है। जैसे प्रत्यभिज्ञानसे ऐसा जाने कि जो बालक अवस्थामें मैं था वही अब तरुण अवस्थामें तथा वृद्ध अवस्थामें हूं, इसी तरह जो अनुभवगोचर स्थ संवेदनमें प्रावे व जिनवाणी भी ऐसे ही कहे उसको न माने वही मिथ्यावृष्टि कहलाता है ।
__ अब इसो अर्थको कलशरूप काव्यमें कहते हैं--आत्मानं इत्यादि । अर्थ-प्रात्मा को संपूर्णतया शुद्ध चाहने वाले अज्ञानान्धोंने उस आत्मामें कालको उपाधिके बलसे अधिक अशुद्धता मानकर अतिव्याप्तिको प्राप्त होकर तथा शुद्ध ऋजुसूत्रनयमें अमर्याद प्रेरित होकर चैतन्यको क्षणिक कल्पना करके इस प्रात्माको छोड़ दिया। जैसे कि हारके सूतको न देख कर मात्र मोतियोंके देखने वाले हारको छोड़ देते हैं । भावार्थ-प्रात्मा तो द्रव्यपर्याय स्वरूप था, यह सर्वया क्षणिक पर्यायस्वरूप मानकर छोड़ दिया गया तो उनको प्रात्माको प्राप्ति नहीं हुई । यहां हारका दृष्टांत है। जैसे मोतियोंका हार है उसमें सूत्र में जो मोती पोये हुए हैं वे भिन्न-भिन्न दीखते हैं सो जो हार सूत्र सहित मोती नहीं दिखते, मोतियोंको ही भिन्न देख