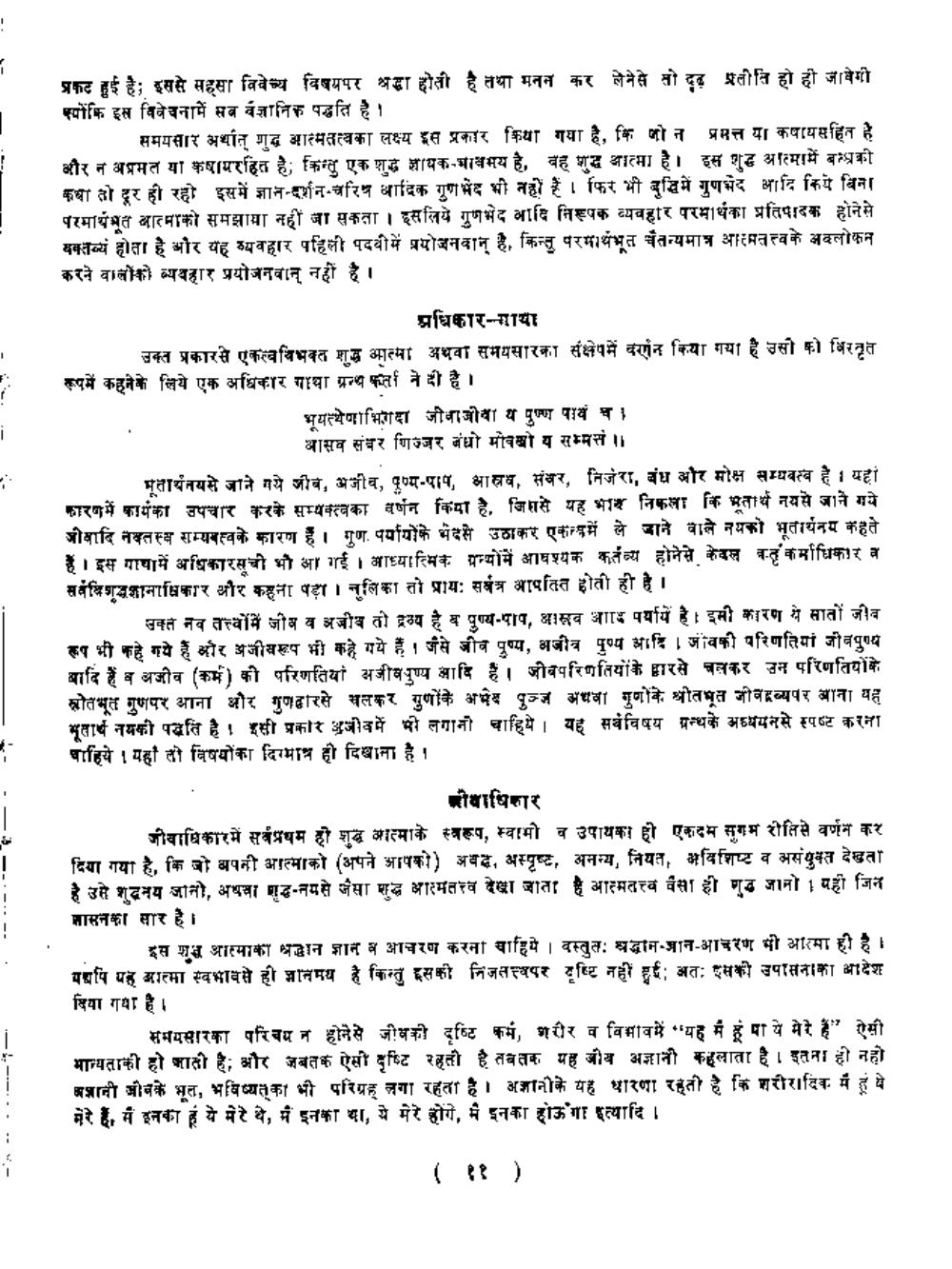________________
7
i
प्रकट हुई है; इससे सहसा विवेच्य विषयपर श्रद्धा होती है तथा मनन कर लेनेसे सो दृढ़ प्रतीति हो ही जावेगी क्योंकि इस विवेचनामें सब वैज्ञानिक पद्धति है ।
समयसार अर्थात् शुद्ध आत्मतत्वका लक्ष्य इस प्रकार किया गया है, कि जो न प्रमत्त या कषायसहित है और न अप्रमत या कषामरहित है; किन्तु एक शुद्ध ज्ञायक भावमय है, वह शुद्ध आत्मा है। इस शुद्ध आत्मामें बन्धकी कथा तो दूर ही रहो इसमें ज्ञान दर्शन- चरित्र आदिक गुणभेद भी नहीं हैं। फिर भी बुद्धि में गुणभेद आदि किये बिना परमार्थभूत आत्माको समझाया नहीं जा सकता। इसलिये गुणभेद आदि निरूपक व्यवहार परमार्थका प्रतिपादक होने से वक्तव्यं होता है और यह व्यवहार पहिली पदवी में प्रयोजनवान् है, किन्तु परमार्थभूत चैतन्यमात्र आत्मतत्त्व के अवलोकन करने वालोंको व्यवहार प्रयोजनवान् नहीं है ।
अधिकार-गाया
उक्त प्रकार से एकल्ब विभक्त शुद्ध आत्मा अथवा समयसारका संक्षेप में दर्शन किया गया है उसी को विस्तृत रूप में कहने के लिये एक अधिकार गाया ग्रन्थकर्ता ने दी है।
भूयत्येणाभिगदा जीवाजीवा व पुष्ण पाय च । आसव संवर णिज्जर बंधो मोखो य सम्मसं ॥
भूतानयसे जाने गये जीब, अजीव, पुण्य-पाप, आस्रव संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष सम्यवत्व है । यहां कारण में फार्मका उपचार करके सम्यक्त्वका वर्णन किया है, जिससे यह भाव निकला कि भूतार्थ नयसे जाने गये जीवादि नवस्थ सम्यमत्वके कारण हैं। गुण पर्यायोंके भेदसे उठाकर एक में ले जाने वाले नयको भूतार्थनय कहते हैं। इस गाथा में अधिकारसूची भी आ गई। आध्यात्मिक ग्रन्थोंमें आवश्यक कर्तव्य होनेसे केवल व कर्माधिकार व सर्वविज्ञानाधिकार और कहना पड़ा। नृलिका तो प्रायः सर्वत्र आपतित होती ही है ।
उक्त नव तत्त्वों में जीव व अजीव तो द्रव्य है व पुण्य-पाप, आसव आप पर्यायें है। इसी कारण ये सातों जीव रूप भी कहे गये हैं और अजीवरूप भी कहे गये हैं। जैसे जीव पुष्य, अजीव पुण्य आदि । जवकी परिणतियां जीवपुण्य बादि हैं व अजीव (कर्म) की परिणतियां अजीव पुण्य आदि हैं। जोवपरिणतियोंके द्वारसे चलकर उन परिणतियोंके स्रोतभूत गुणपर आना और गुणद्वारसे चलकर गुणोंके अभेद पुञ्ज अथवा गुणोंके श्रीतभूत जीवद्रव्यपर बना यह भूतार्थ नमकी पद्धति है। इसी प्रकार अजीव भी लगानी चाहिये। यह सर्वविषय ग्रन्थके अध्ययन से स्पष्ट करना चाहिये । यहाँ तो विषयोंका दिग्मात्र हो दिखाना है ।
श्रीवाधिकार
जीवाधिकार में सर्वप्रथम हो शुद्ध आत्माके स्वरूप, स्वामी व उपायका ही एकदम सुगम रीति से वर्णन कर दिया गया है, कि जो अपनी आत्माको (अपने आपको ) अवद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशिष्ट व असंयुक्त देखता है उसे शुद्धनय जानो, अथवा शुद्ध-नमसे जैसा शुद्ध आत्मतत्व देखा जाता है आत्मतत्त्व वैसा ही शुद्ध जानो । यही जिन शासनका सार है ।
इस शुद्ध आत्माका श्रद्धान ज्ञान व आचरण करना चाहिये। वस्तुतः श्रद्धान जान आचरण भी आत्मा ही है । यद्यपि यह आत्मा स्वभावसे ही ज्ञानमय है किन्तु इसकी निजतत्वपर दृष्टि नहीं हुई अतः इसकी उपासनाका आदेश दिया गया है।
समयसारका परिचय न होने से जीवको दृष्टि कर्म, शरीर व विभावमें "यह मैं हूं पाये मेरे हैं" ऐसी मान्यताकी हो जाती है; और जबतक ऐसी दृष्टि रहती है तबतक यह जीव अज्ञानी कहलाता है। इतना ही नहीं waratatah भूत, भविष्यत्का भी परिग्रह लगा रहता है। अज्ञानीके यह धारणा रहती है कि शरीरादिक में हूं ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ ये मेरे थे, में इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊंगा इत्यादि ।
( ११ )