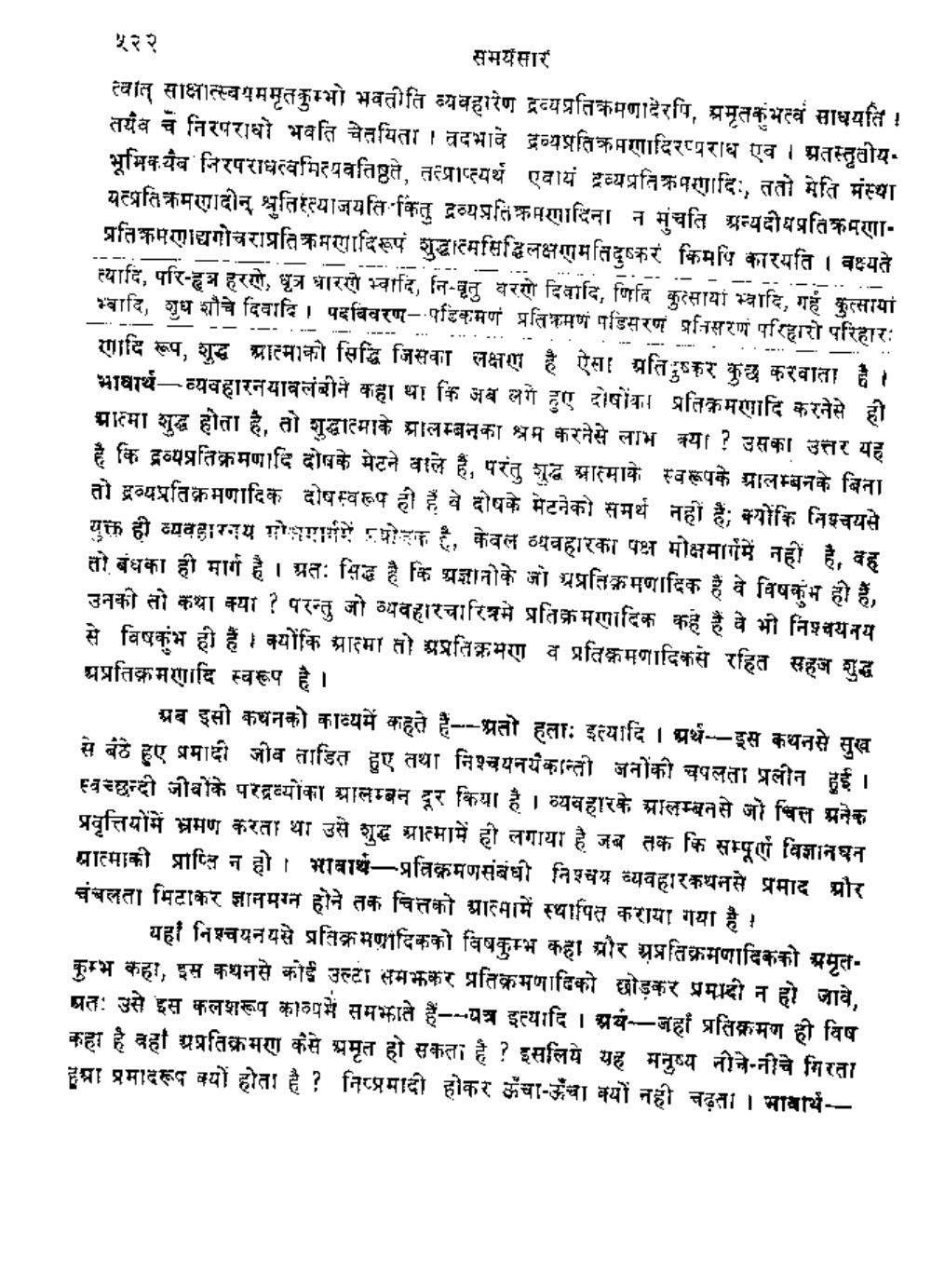________________
५२२
समयंसार स्वात् साक्षात्स्वयममृतकुम्भो भवतीति व्यवहारेण द्रव्यप्रतिक्रमणादेरपि, अमृतकुंभत्वं साधयति ! तयैव च निरपराधो भवति चेतयिता । वदभावे द्रव्यप्रतिक्रमणादिरप्पराध एव । प्रतस्तृतीयभूमिकयव निरपराधत्वमित्यवतिष्ठते, तत्प्राप्त्यर्थ एवायं द्रव्यप्रतिक्रमणादिः, ततो मेति मंस्था यत्प्रतिक्रमणादीन श्रुतिस्त्याजयति किंतु द्रव्यप्रतिक्रमणादिना न मुंचति अन्यदीयप्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणाद्यगोचराप्रतिक्रमणादिरूपं शुद्धात्मसिद्धिलक्षणमतिदुष्करं किमपि कारयति । वक्ष्यते त्यादि, परि-हत्र हरणे, धूत्र धारणे भ्वादि, नि-वृतु वरणे दिवादि, णिदि कुत्सायां भ्वादि, गई कुत्सायां भ्वादि, शुध शौचे दिवादि। पदविवरण- पडिकमण प्रतिक्रमणं पडिसरणं तिसरणं परिहारो परिहारः रणादि रूप, शुद्ध प्रात्माको सिद्धि जिसवा लक्षण है ऐसा अति पुष्कर कुछ करवाता है। भावार्थ-व्यवहारनयावलंबीने कहा था कि जब लगे हुए दोषोंवा प्रतिक्रमणादि करनेसे ही मात्मा शुद्ध होता है, तो शुद्धात्माके पालम्बनका श्रम करनेसे लाभ क्या ? उसका उत्तर यह है कि द्रव्यप्रतिक्रमणादि दोषके मेटने वाले हैं, परंतु शुद्ध अात्माके स्वरूपके पालम्बनके बिना तो द्रव्यप्रतिक्रमणादिक दोषस्वरूप ही हैं वे दोषके मेटनेको समर्थ नहीं हैं; क्योंकि निश्चयसे युक्त ही व्यवहारमय गोत्रमार्ग में प्रोना है, केवल व्यवहारका पक्ष मोक्षमार्गमें नहीं है, वह तो बंधका ही मार्ग है । अतः सिद्ध है कि अज्ञानोके जो अप्रतिक्रमणादिक हैं वे विषकम ही हैं, उनकी तो कथा क्या ? परन्तु जो व्यवहारचारित्रमे प्रतिक्रमणादिक कहे हैं वे भी निश्चयनय से विषकुंभ ही हैं। क्योंकि आत्मा तो अतिक्रमण व प्रतिक्रमणादिकसे रहित सहज शुद्ध अतिक्रमणादि स्वरूप है।
अब इसी कथनको काव्यमें कहते हैं--प्रतो हलाः इत्यादि । अर्थ-इस कथनसे सुख से बैठे हुए प्रमादी जीव ताडित हुए तथा निश्चयनये कान्ती जनोंको चपलता प्रलीन हुई । स्वच्छन्दी जीवोंके परद्रव्योंका पालम्बन दूर किया है । व्यवहारके पालम्बनसे जो चित्त अनेक प्रवृत्तियोंमें भ्रमण करता था उसे शुद्ध प्रात्मामें ही लगाया है जब तक कि सम्पूर्ण विज्ञानघन मात्माकी प्राप्ति न हो। भावार्थ-प्रतिक्रमणसंबंधी निश्चय व्यवहारकथनसे प्रमाद और चंचलता मिटाकर ज्ञानमग्न होने तक चित्तको आत्मामें स्थापित कराया गया है।
यहां निश्चयन यसे प्रतिक्रमणादिकको विषकुम्भ कहा और अप्रतिक्रमणादिकको अमृतकुम्भ कहा, इस कथनसे कोई उल्टा समझकर प्रतिक्रमणादिको छोड़कर प्रमादी न हो जावे, प्रतः उसे इस कलशरूप काव्यमें समझाते हैं--यत्र इत्यादि । अयं-जहाँ प्रतिक्रमण ही विष कहा है वहाँ अप्रतिक्रमण कैसे अमृत हो सकता है ? इसलिये यह मनुष्य नोचे-नीचे गिरता हमा प्रमादरूप क्यों होता है ? निष्प्रमादी होकर ऊँचा-ऊँचा क्यों नहीं चढ़ता । भावार्थ