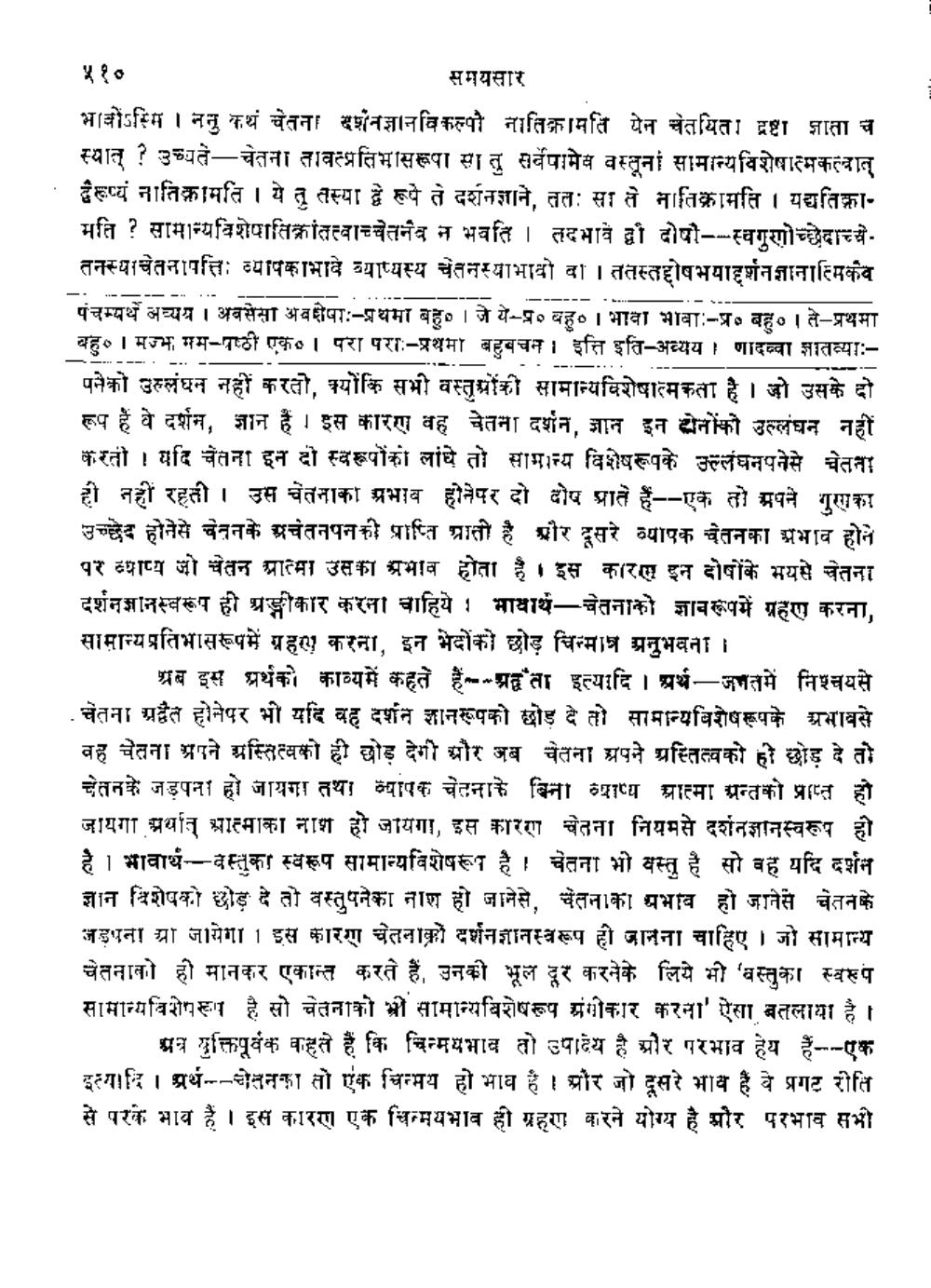________________
५१०
समयसार
भावोऽस्मि । ननु कथं चेतना दर्शनज्ञानविकल्पो नातिकामति येन चेतयिता द्रष्टा ज्ञाता च स्यात् ? उच्यते-चेतना तावत्प्रतिभासरूपा सा तु सर्वेपामेव वस्तूनां सामान्यविशेषात्मकत्वात् द्वैरूप्यं नातिकामति । ये तु तस्या द्वे रूपे ते दर्शनज्ञाने, ततः सा ते नातिकामति । यद्यतिकामति ? सामान्य विशेषातिक्रांतत्वाच्चेतनव न भवति । तदभावे द्वी दोषौ---स्वगुणोच्छेदाच्चेतनस्याचेतनापत्तिः व्यापकाभावे व्याप्यस्य चेतनस्याभावो वा । ततस्तदोषभयाद्दर्शनज्ञानात्मिकंव पंचम्यर्थे अव्यय । अवसेसा अवशेषाः-प्रथमा बहु० । जे ये-प्र०बहु । भावा भावाः-प्र. बह ० । ते-प्रथमा बहु० । मज्भ मम-पष्ठी एक० । परा परा:-प्रथमा बहुवचन । इत्ति इति-अव्यय । णादब्वा ज्ञातव्या:पनेको उल्लंघन नहीं करतो, क्योंकि सभी वस्तुओं की सामान्यविशेषात्मकता है । जो उसके दो रूप हैं वे दर्शन, ज्ञान हैं । इस कारण वह चेतना दर्शन, ज्ञान इन दोनोंको उल्लंघन नहीं करती । यदि चेतना इन दो स्वरूपोंको लांधे तो सामान्य विशेषरूपके उल्लंघनपनेसे चेतना ही नहीं रहती। उस चेतनाको अभाव होनेपर दो दोष पाते हैं--एक तो अपने गुराका उच्छेद होनेसे चेननके अचेतनपनकी प्राप्ति प्रातो है और दूसरे व्यापक चेतनका अभाव होने पर व्याप्य जो चेतन आत्मा उसका प्रभाव होता है । इस कारण इन दोषोंके भयसे चेतना दर्शनझानस्वरूप ही अङ्गीकार करना चाहिये । भावार्थ-चेतनाको ज्ञावरूपमें ग्रहण करना, सामान्य प्रतिभासरूपमें ग्रहण करना, इन भेदोंको छोड़ चिन्मात्र अनुभवना ।।
___ अब इस अर्थको काव्यमें कहते हैं--प्रदता इत्यादि । अर्थ-जनतमें निश्चयसे चेतना अद्वैत होनेपर भी यदि वह दर्शन ज्ञानरूपको छोड़ दे तो सामान्यविशेषरूपके अमावसे वह चेतना अपने अस्तित्वको ही छोड़ देगी और अब चेतना अपने अस्तित्वको ही छोड़ दे तो चेतनके जड़पना हो जायगा तथा व्यापक चेतनाके बिना व्याप्य प्रात्मा अन्तको प्राप्त हो जायगा अर्थात् आत्माका नाश हो जायगा, इस कारण चेतना नियमसे दर्शनज्ञानस्वरूप हो है । भावार्थ---वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषरूप है। चेतना भी वस्तु है सो वह यदि दर्शन ज्ञान विशेषको छोड़ दे तो वस्तुपनेका नाश हो जानेसे, चेतनाका अभाव हो जानेसे चेतनके जइपना या जायेगा 1 इस कारण चेतनाको दर्शनज्ञानस्वरूप ही जानना चाहिए । जो सामान्य चेतनाको ही मानकर एकान्त करते हैं, उनकी भूल दूर करनेके लिये भी 'वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषरूप है सो चेतनाको भी सामान्य विशेषरूप अंगीकार करना' ऐसा बतलाया है ।
अत्र युक्तिपूर्वक वाहते हैं कि चिन्मयभाव तो उपादेय है और परभाव हेय हैं----एक इत्यादि । अर्थ---चेतनका तो एक चिन्मय हो भाव है । और जो दूसरे भाव है वे प्रगट रोति से परके भाव हैं । इस कारण एक चिन्मयभाव ही ग्रहण करने योग्य है और परभाव सभी