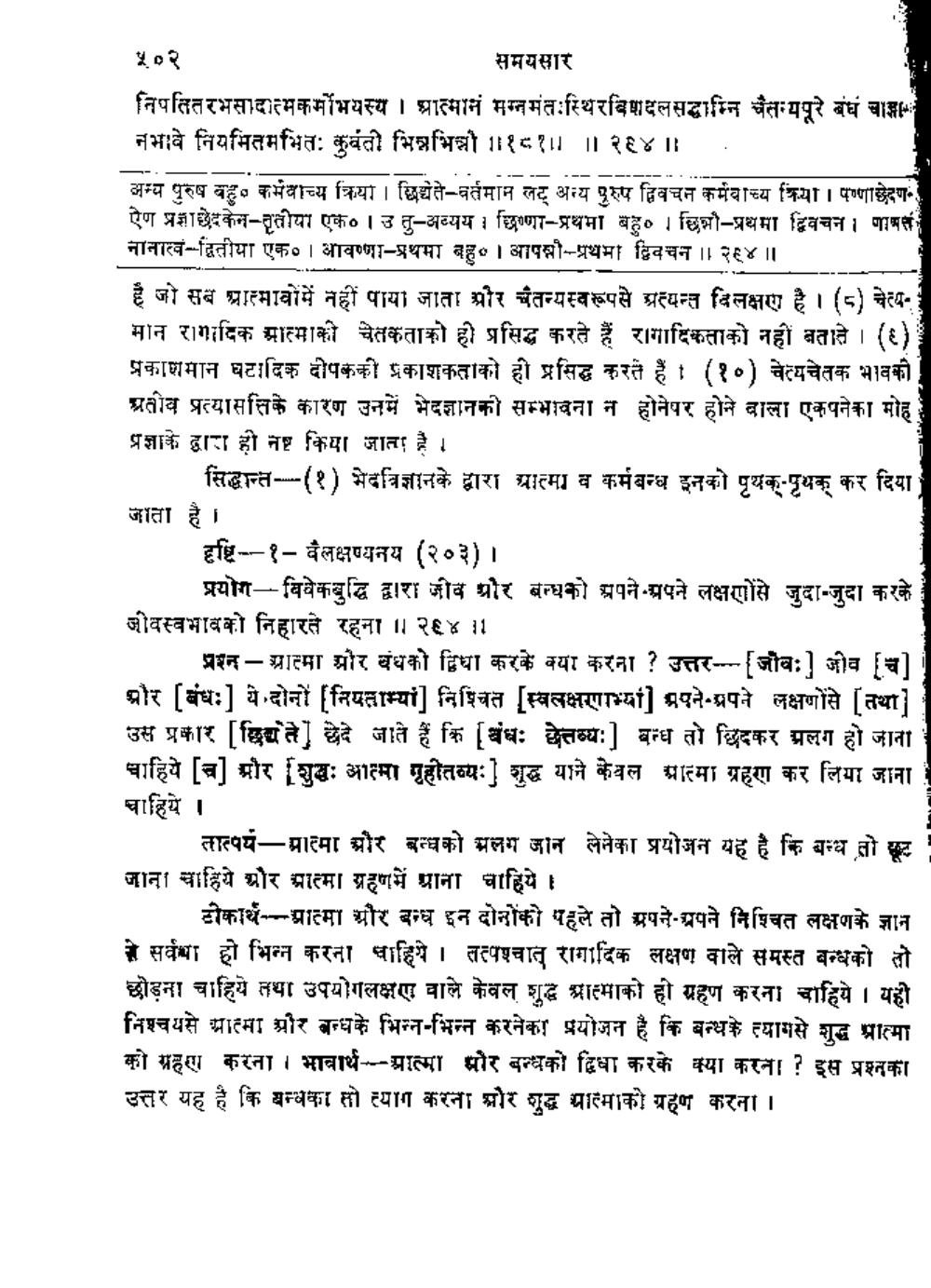________________
समयसार निपतित रभसादात्मकर्मोभयस्य । प्रात्मानं मम्नमंतःस्थिरविशदलसद्धाम्नि चैतन्यपूरे बंध चाहा नभावे नियमितमभित: कुवंती भिन्नभिन्नौ ॥१८१॥ ॥ २६४ ॥ . अन्य पुरुष बहु० कर्मवाच्य क्रिया । छियेते-वर्तमान लट् अन्य पुरुप द्विवचन कर्मवाच्य किया। पण्णाछेदगऐण प्रज्ञाछेद केन-तृतीया एक० । उ तु-अव्यय । छिण्णा-प्रथमा बहु० । छिनौ-प्रथमा द्विवचन । गायत नानात्व-द्वितीया एक० । आवण्णा-प्रथमा बहु । आपनी-प्रथमा द्विवचन ।। २९४ ।। है जो सब प्रात्मावों में नहीं पाया जाता और चतन्यस्वरूपसे अत्यन्त दिलक्षण है। (८) चेत्यमान रागादिक आत्माको चेतकताको ही प्रसिद्ध करते हैं रागादिकताको नहीं बताते । (६) प्रकाशमान घटादिक दीपककी प्रकाशकताको ही प्रसिद्ध करते हैं । (१०) चेत्यचेतक भावको प्रतीव प्रत्यासत्ति के कारण उनमें भेदज्ञानको सम्भावना न होनेपर होने वाला एकपनेका मोह । प्रज्ञाके द्वारा ही नष्ट किया जाता है ।
सिद्धान्त--(१) भेदविज्ञानके द्वारा ग्रात्मा व कर्मबन्ध इनको पृथक्-पृथक् कर दिया जाता है।
दृष्टि--१- वैलक्षण्यनय (२०३) ।
प्रयोग-विवेकबुद्धि द्वारा जीव और बन्धको अपने अपने लक्षणोंसे जुदा-जुदा करके । जीवस्वभावको निहारते रहना ।। २६४ 11
प्रश्न - प्रात्मा और बंधको द्विधा करके क्या करना ? उत्तर---- जीवः] जीव च] | प्रौर [बंधः] ये दोनों [नियताभ्यां] निश्चित [स्वलक्षणाभ्यां] अपने अपने लक्षणोंसे [तथा उस प्रकार [छिद्य ते छेदे जाते हैं कि [बंधः छेत्तव्यः] बन्ध तो छिदकर अलग हो जाना चाहिये [च] और शुक्षः आत्मा गृहीतव्यः] शुद्ध याने केवल प्रात्मा ग्रहण कर लिया जाना ! चाहिये ।
तात्पर्य-मात्मा और बन्धको अलग जान लेनेका प्रयोजन यह है कि बन्ध तो फूट जाना चाहिये और प्रात्मा ग्रहण में पाना चाहिये ।
टोकार्थ-प्रात्मा और बन्ध इन दोनोंको पहले तो अपने-अपने निश्चित लक्षणके ज्ञान से सर्वधा हो भिन्न करना चाहिये । तत्पश्चात् रागादिक लक्षण वाले समस्त बन्धको तो छोड़ना चाहिये तथा उपयोगलक्षण वाले केवल शुद्ध आत्माको हो ग्रहण करना चाहिये । यही निश्चयसे मात्मा और बन्धके भिन्न-भिन्न करनेका प्रयोजन है कि बन्धके त्यागसे शुद्ध प्रात्मा को ग्रहण करना । भावार्थ---प्रात्मा भोर बन्धको द्विधा करके क्या करना ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि बन्धका तो त्याग करना और शुद्ध पात्माको ग्रहण करना ।