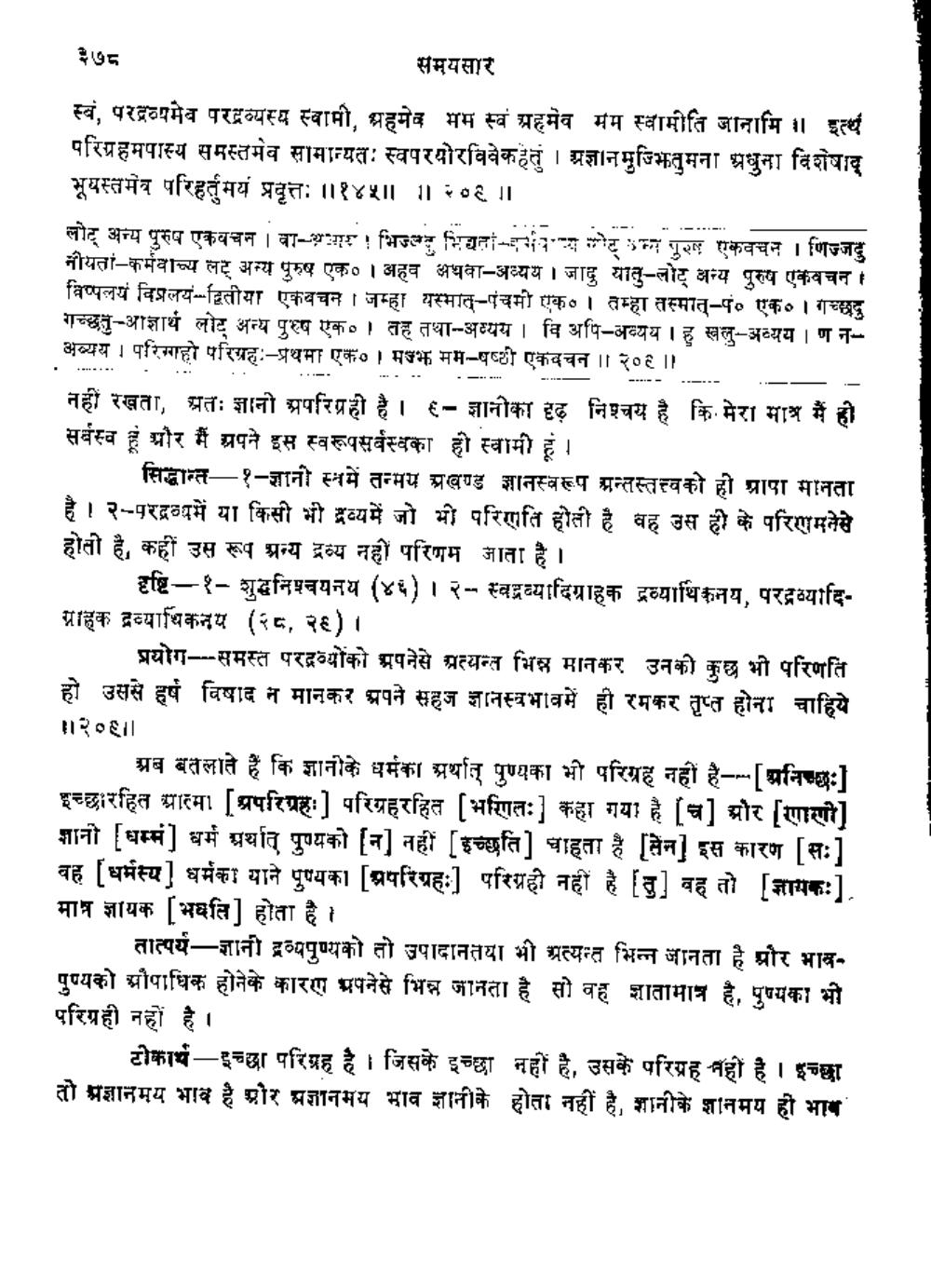________________
समयसार
स्व, परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वामी, अहमेव मम स्वं अहमेव मम स्वामीति जानामि ॥ इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेक हेतुं । अज्ञान मुज्झितुमना अधुना विशेषाद् भूयस्तमेव परिहर्तुमयं प्रवृत्तः ।।१४५।। ।। २०६ ।। लोट् अन्य पुरुष एकवचन । वा-यगर ! भिज्ज भिद्यतांवर अकोट म गुरुल एकवचन । णिज्जदु नौयतां-कर्मवाच्य लट् अन्य पुरुष एक० । अहव अथवा-अव्यय । जादु यातु-लोट् अन्य पुरुष एकवचन । विप्पलयं विप्रलय-द्वितीया एकवचन । जम्हा यस्मात-पंचमी एक० । तम्हा तस्मात्-पं० एक० । गच्छदु गच्छतु-आज्ञार्थ लोट् अन्य पुरुष एकः । तह तथा--अव्यय । वि अपि-अव्यय । हु खलु-अव्यय । ण नअव्यय । परिग्गहो परिग्रहः-प्रथमा एक० । माझ मम-षष्ठी एकवचन ।। २०६ ।। नहीं रखता, अतः ज्ञानी अपरिग्रही है । - ज्ञानीका दृढ़ निश्चय है कि मेरा मात्र में ही सर्बस्व हूं और मैं अपने इस स्वरूपसर्वस्वका ही स्वामी हूं।
सिद्धान्त-१-ज्ञानी स्नमें तन्मय अखण्ड ज्ञानस्वरूप अन्तस्तत्त्वको ही प्रापा मानता है। २-परद्रव्यमें या किसी भी द्रव्यमें जो भी परिणति होती है वह उस हो के परिणामसे होती है, कहीं उस रूप अन्य द्रव्य नहीं परिणम जाता है।
दृष्टि-१- शुद्धनिश्चयनय (४६) । २-- स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय, परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय (२८, २९) ।
प्रयोग---समस्त परद्रव्योंको अपनेसे अत्यन्त भिन्न मानकर उनकी कुछ भी परिणति हो उससे हर्ष विषाद न मानकर अपने सहज ज्ञानस्वभावमें ही रमकर तृप्त होना चाहिये ॥२०६।।
अब बतलाते हैं कि ज्ञानीके धर्मका अर्थात् पुण्यका भी परिग्रह नहीं है---[अनिच्छः] इच्छारहित प्रात्मा [अपरिग्रहः] परिग्रहरहित [भरिणतः] कहा गया है [च] और [रणारणी] शानी [धम्म] धर्म अर्थात् पुण्यको [न] नहीं [इच्छति] चाहता है [सेन] इस कारण [सः] वह [धर्मस्य] धर्मका याने पुण्यका [अपरिग्रहः] परिग्रही नहीं हैं [तु] वह तो [ज्ञायकः]. मात्र ज्ञायक [भवति] होता है।
तात्पर्य-ज्ञानी द्रव्यपुण्यको तो उपादानतया भी अत्यन्त भिन्न जानता है और भावपुण्यको औपाधिक होनेके कारण अपनेसे भिन्न जानता है सो वह ज्ञातामात्र है, पुण्यका भी परिग्रही नहीं है।
टोकार्थ-इच्छा परिग्रह है । जिसके इच्छा नहीं है, उसके परिग्रह नहीं है । इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और प्रज्ञानमय भाव ज्ञानीके होता नहीं है, शानीके ज्ञानमय ही भाव