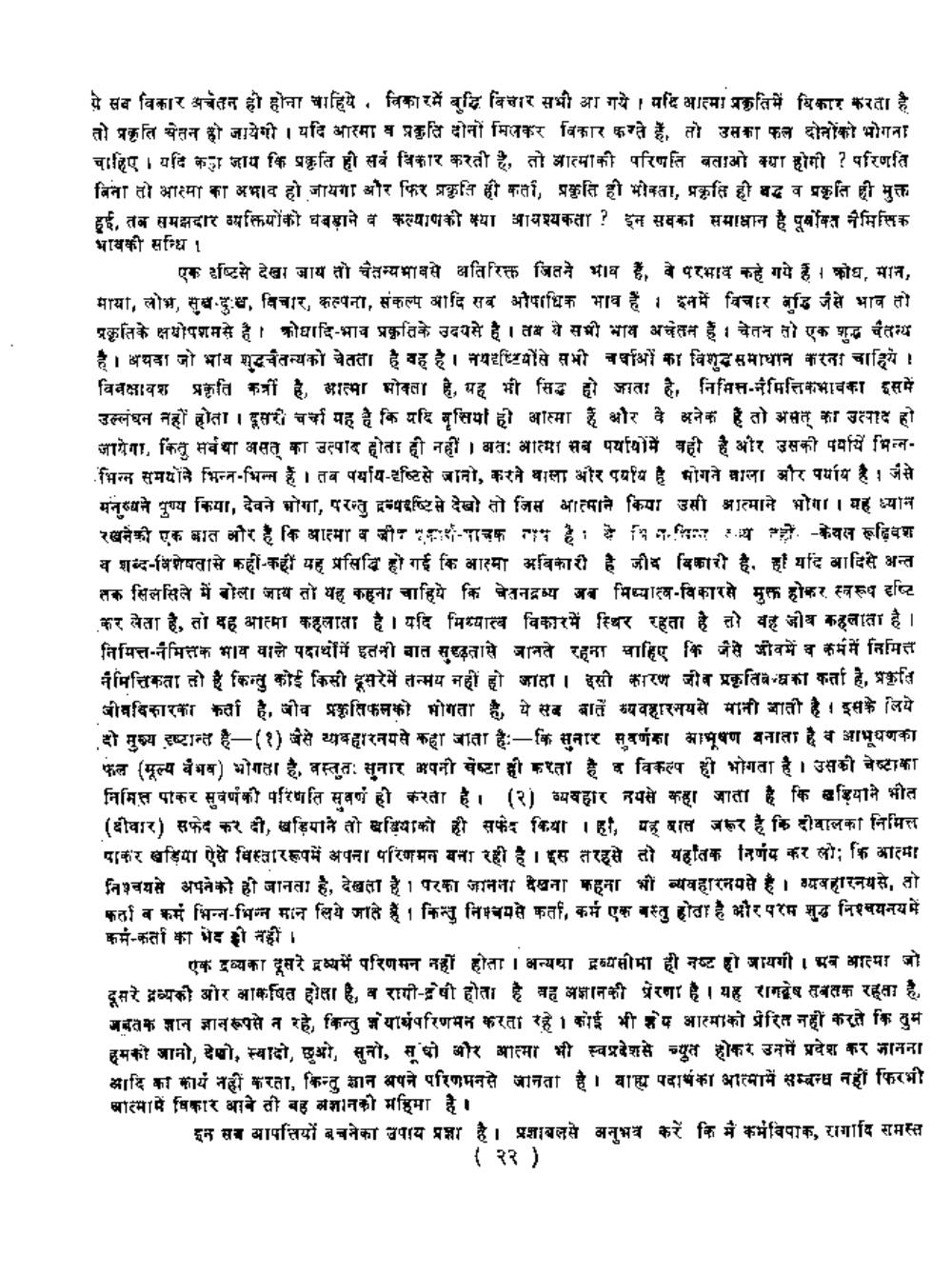________________
से सब विकार अचेतन ही होना चाहिये विकार में बुद्धि विचार सभी आ गये। यदि आत्मा प्रकृतिमें विकार करता है. तो प्रकृति वेतन हो जायेगी । यदि आत्मा व प्रकृति दोनों मिलकर विकार करते हैं, तो उसका फल दोनोंको भोगना
"
चाहिए। यदि कहा जाय कि प्रकृति सर्व विकार करती है, तो आत्माको परिणति बताओ क्या होगी ? परिणति बिना तो आत्मा का अभाव हो जायगा और फिर प्रकृति ही कर्ता, प्रकृति ही भोक्ता, प्रकृति ही बद्ध व प्रकृति ही मुक्त हुई, तब समझदार व्यक्तियों को चबढ़ाने व कल्याणकी क्या आवश्यकता ? इन सबका समाधान है पूर्वोक्त नैमिकि भावकी सन्धि
एक दृष्टिसे देखा जाय तो चैतन्य भाव से अतिरिक्त जितने
है।
भाव हैं, वे परभाव कहे गये हैं । क्रोध, मान, माया, लोभ, सुख-दुःख, विचार, कल्पना, संकल्प आदि सब औपाधिक भाव हैं । इनमें विचार बुद्धि जैसे भाव तो प्रकृति के क्षयोपशम से है। क्रोधादि-भाव प्रकृतिके उदयसे है । तब ये सभी भाव अचेतन है | चेतन तो एक शुद्ध चैतन्य है । अथवा जो भाव शुद्धचैतन्यको चेतता है वह है । नयदृष्टियों सभी चर्चाओं का विशुद्धसमाधान करना चाहिये । विवक्षावंश प्रकृति कत्रीं है, आत्मा मोक्ता है, यह भी सिद्ध हो जाता है, निमित्तनैमित्तिकभावका इसमें उल्लंघन नहीं होता । दूसरी चर्चा यह है कि यदि वृत्तियों हो आत्मा है और दे अनेक है तो असत् का उत्पाद हो जायेगा, किंतु सर्वथा असत् का उत्पाद होता ही नहीं । अतः आत्मा सब पर्यायों में वही है और उसकी पर्यायें भिन्नभिन्न समयों भिन्न-भिन्न है। तब पर्याय दृष्टिसे जातो, करने वाला और पर्याय है भोगने वाला और पर्याय है । जैसे मनुष्यने पुण्य किया, देवने भोगा, परन्तु द्रव्यष्टि से देखो तो जिस आत्माने किया उसी आत्माने भोगा | यह ध्यान रखने की एक बात और है कि आत्मा व पाचक केवल रूढ़िवश य शब्द - विशेषता से कहीं-कहीं यह प्रसिद्धि हो गई कि आत्मा अविकारी है जीद विकारी है. हाँ यदि आदिसे अन्त तक सिलसिले में बोला जाय तो यह कहना चाहिये कि वेतनद्रस्य जब मिध्यात्व-विकार से मुक्त होकर स्वरूप दृष्टि कर लेता है, तो वह आत्मा कहलाता है । यदि मिथ्यात्व विकार में स्थिर रहता है तो वह जीव कहलाता है । निमित्त कि भाव वाले पदार्थों में इतनी बात सुतासे जानते रहना चाहिए कि जैसे जीव व कर्म में निमित्त नैमित्तिकता तो हैं किन्तु कोई किसी दूसरे में तन्मय नहीं हो जाता। इसी कारण जीव प्रकृतिवन्धका कर्ता है, प्रकृति aafeerer कर्ता है, जीव प्रकृतिफलको भोगता है, ये सब बातें व्यवहारमय से मानी जाती है। इसके लिये दो मुख्य दृष्टान्त हैं- ( १ ) जैसे व्यवहारनयसे कहा जाता है: - कि सुनार सुवर्णका माभूषण बनाता है व आभूषणका फल ( मूल्य वैभव ) भोगता है, वस्तुतः सुनार अपनी बेष्टा ही करता है व विकल्प हो भोगता है। उसकी चेष्टाका निमित्त पाकर सुवर्णकी परिणति सुवणं ही करता है। (२) व्यवहार नपसे कहा जाता है कि याने भीत (दीवार) सफेद कर दी, खड़ियाने तो खड़िया को ही सफेद किया । हाँ, यह बात जरूर है कि दीवालका निमित्त पाकर खड़िया ऐसे विस्ताररूपमें अपना परिणमन बना रही है। इस तरहसे तो यहृतिक निर्णय कर लो कि आत्मा निश्चयसे अपने को ही जानता है, देखता है। परका जानना देखना कहना भी व्यवहारनयसे है। व्यवहारसे, तो कर्ता व कर्म भिन्न-भिन्न मान लिये जाते हैं । किन्तु निश्चय कर्ता, कर्म एक वस्तु होता है और परम शुद्ध निश्चयनय में कर्म-कर्ता का भेद ही नहीं ।
एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यमें परिणमन नहीं होता । अन्यथा द्रव्यसीमा ही नष्ट हो जायगी । भव आत्मा जो दूसरे द्रव्यकी ओर आकर्षित होता है, व रागी-द्रषी होता है वह अज्ञानकी प्रेरणा है। यह रागद्वेष तक रहता है, जबतक ज्ञान ज्ञानरूपसे न रहे, किन्तु ज्ञेयार्थपरिणमन करता रहे। कोई भी शेय आत्माको प्रेरित नहीं करते कि तुम हमको जानो, देखो, स्वादो, छुओ, सुनो, सूचो और आत्मा भी स्वप्रदेश से च्युत होकर उनमें प्रवेश कर जानना आदि का कार्य नहीं करता, किन्तु ज्ञान अपने परिणमनसे जानता है । बाह्य पदार्थका आत्मामें सम्बन्ध नहीं फिरभी मायें विकार आने ती बह अज्ञानको महिमा है ।
इन सब व्यापत्तियों बचनेका उपाय प्रशा है। प्रशाबलसे अनुभव करें कि मैं कर्मविपाक, रागादि समस्त ( २२ )