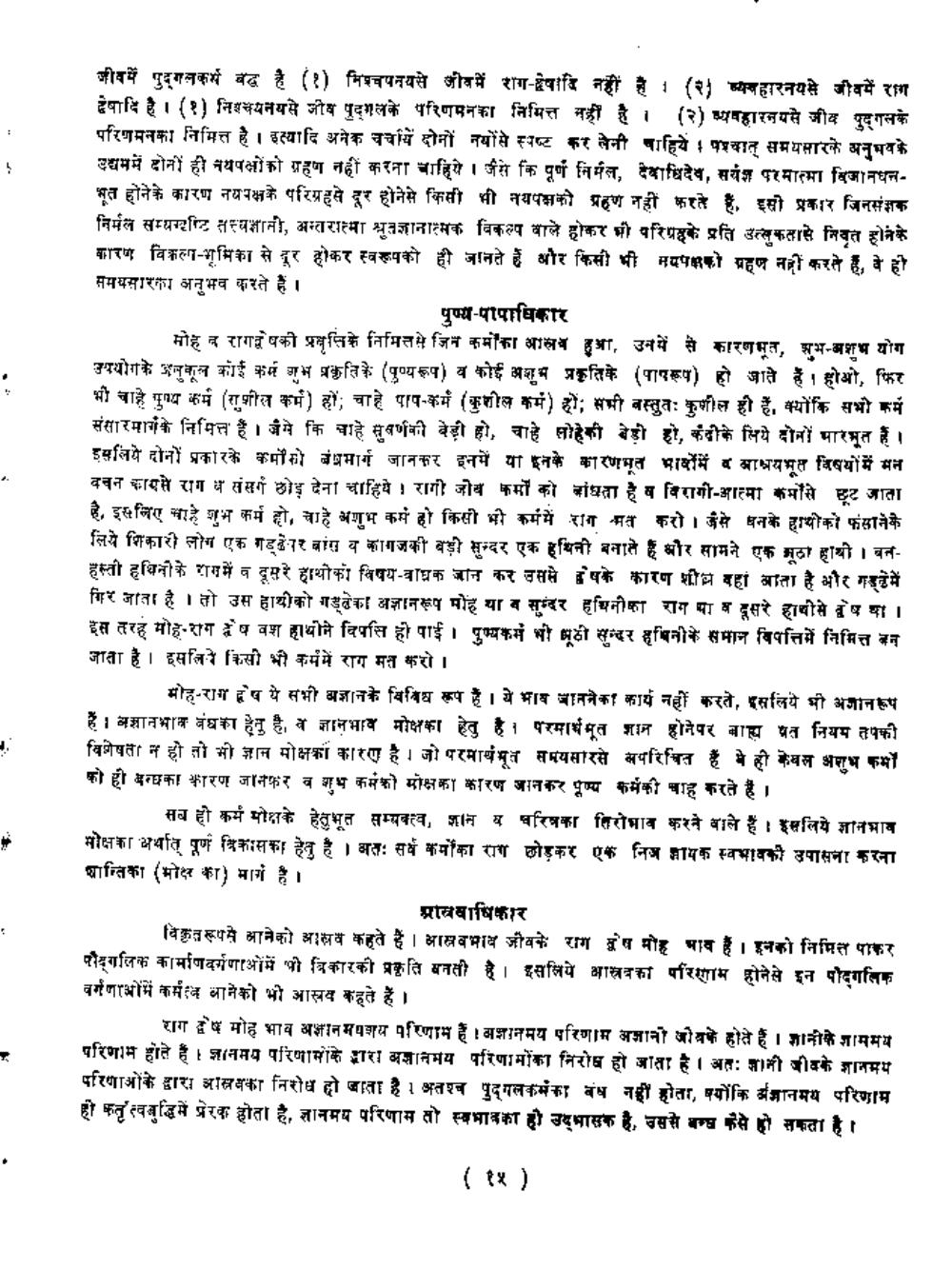________________
जीव, पुद्गलकर्ष बद्ध है (१) मिश्चपनयसे जीवमें राग-द्वेषादि नहीं है । (२) व्यवहारनयसे जीवमें राग द्वेषादि है । (१) निश्चयनयसे जीव पुद्गलके परिणमनका निमित्त नहीं है । (२) व्यवहारमयसे जीव पुद्गलके परिणमनका निमित्त है । इत्यादि अनेक चर्चाये दोनों नयों से स्पष्ट कर लेनी चाहिये पश्चात् समयसारके अनुभव के उद्यममें दोनों ही नयपक्षों को ग्रहण नहीं करना चाहिये । जैसे कि पूर्ण निर्मल, देवाधिदेव, सर्वज्ञ परमात्मा विमानधन - भूत होने के कारण नयपक्षके परिग्रहसे दूर होनेसे किसी भी नयपक्षको ग्रहण नहीं करते हैं, इसी प्रकार जिनसंज्ञक निर्मल सम्यग्दष्टि तत्वज्ञानी, अन्तरात्मा श्रुतज्ञानात्मक विकल्प वाले होकर भी परिप्रहके प्रति उत्सुकतासे निवृत होने के कारण विकल्प-शूमिका से दूर होकर स्वरूपको ही जानते हैं और किसी भी मयपक्षको ग्रहण नहीं करते हैं, वे ही समयसारका अनुभव करते हैं।
पुण्य-पापाधिकार मोह व रागद्वेषकी प्रवृतिके निमित्तसे जिन कोका आश्रय हुआ, उनमें से कारणभूत, अभ-अशुभ योग उपयोग के अनुकूल कोई कर्म शुभ प्रकृति के (पुण्यरूप) व कोई अशुभ प्रकृतिके (पापरूप) हो जाते हैं। होओ, फिर भी चाहे पुण्य कर्म (राशील कर्म) हों; चाहे पाप-कर्म (कुशील कर्म) हो; सभी वस्तुतः कुशील ही हैं, क्योंकि सभी कम संसारमार्गके निमित्त हैं। जैसे कि चाहे सुवर्णवी बेड़ी हो, चाहे लोहेकी बेडी हो, कंदीके लिये दोनों भारभूत हैं। इसलिये दोनों प्रकार के कर्मों को बंधमार्ग जानकर इनमें या इनके कारणभूत भावों में बाश्रयभूत विषयों में मन वचन कारसे राग घ संसर्ग छोड़ देना चाहिये । रागी जोय कर्मों को बांधता है व विरागी-आत्मा कोसे छूट जाता है, इसलिए चाहे शुभ कर्म हो, चाहे अशुभ कर्म हो किसी भी कर्ममें राग मत करो। जैसे उनके हाथोको फंसाने के लिये शिकारी लोग एक गड़गर बांस व कागजकी बड़ी सुन्दर एक हथिनी बनाते हैं और सामने एक मूठा हाथी। बनहस्ती हुधिनी के ग्राम में व दूसरे हाथोको विषय-वाचक जान कर उससे षके कारण शीच वहां आता है और गड्ढे में गिर जाता है । तो उस हाथीको गड्ढेका अज्ञानरूप मोह था व समंदर हथिनीका राग या दूसरे हाथीसे वेष था। इस तरह मोह-राग द्वेष वश हाथीने विपसि हो पाई। पुण्यकर्म भी मूठी सुन्दर हधिनीके समान विपत्तिमें निमित्त बन जाता है। इसलिरे किसी भी कर्ममें राग मत करो।
मोह-राग द्वेष ये सभी अज्ञानके विविश्व रूप है । ये भाव जाननेका कार्य नहीं करते, इसलिये भी अजानरूप हैं। अमानमात्र बंधका हेतु है, वे ज्ञानभाव मोक्षका हेतु है। परमार्थ मृत ज्ञान होने पर बाय प्रत नियम तपकी विशेषता हो तो भी ज्ञान मोक्षका कारण है। जो परमार्यभूत समयसारसे अपरिचित हैं ये ही केवल अशुभ कों को ही बग्धका कारण जानकर व शुभ कमको मोक्षका कारण जानकर पूण्य कर्मकी चाह करते है।
सब हो कर्म मोक्षके हेतभूत सम्यक्त्व, ज्ञान व परित्रका तिरोभाव करने वाले हैं। इसलिये ज्ञानमाव मोक्षका अर्थात् पूर्ण विकासका हेतु है । अत: सर्व कर्मों का राग छोड़कर एक निजज्ञापक स्वभावकी उपासना करना शान्तिका (मोक्ष का) मार्ग है।
प्राखवाधिकार विकृतरूपसे आनेको आसव कहते हैं । आम्रवभाव जीवके राग तूष मोह भाव हैं। इनको निमित्त पाकर पौगलिक कार्माणवर्गणाओंमें पी विकारकी प्रकृति बनती है। इसलिये आस्रवका परिणाम होनेसे इन पौदगलिक वर्गणाओं में कर्मद आने को भी आस्रव कहते हैं।
राग देष मोह भाव अज्ञानमयशय परिणाम हैं। अज्ञानमय परिणाम अज्ञानी जीवके होते हैं । ज्ञानीके ज्ञाममय परिणाम होते हैं। ज्ञानमय परिणामोंके द्वारा अज्ञानमय परिणामोंका निरोष हो जाता है। अत: जानी जीवके ज्ञानमय
रा आसमका निरोध हो जाता है। अतश्च पदगलकमका बंध नहीं होता. पयोंकि शानमय परिणाम हो फर्तृत्वबुद्धि में प्रेरक होता है, ज्ञानमय परिणाम तो स्वभावका हो उद्भासक है, उससे बन्ध कैसे हो सकता है।
(१५)