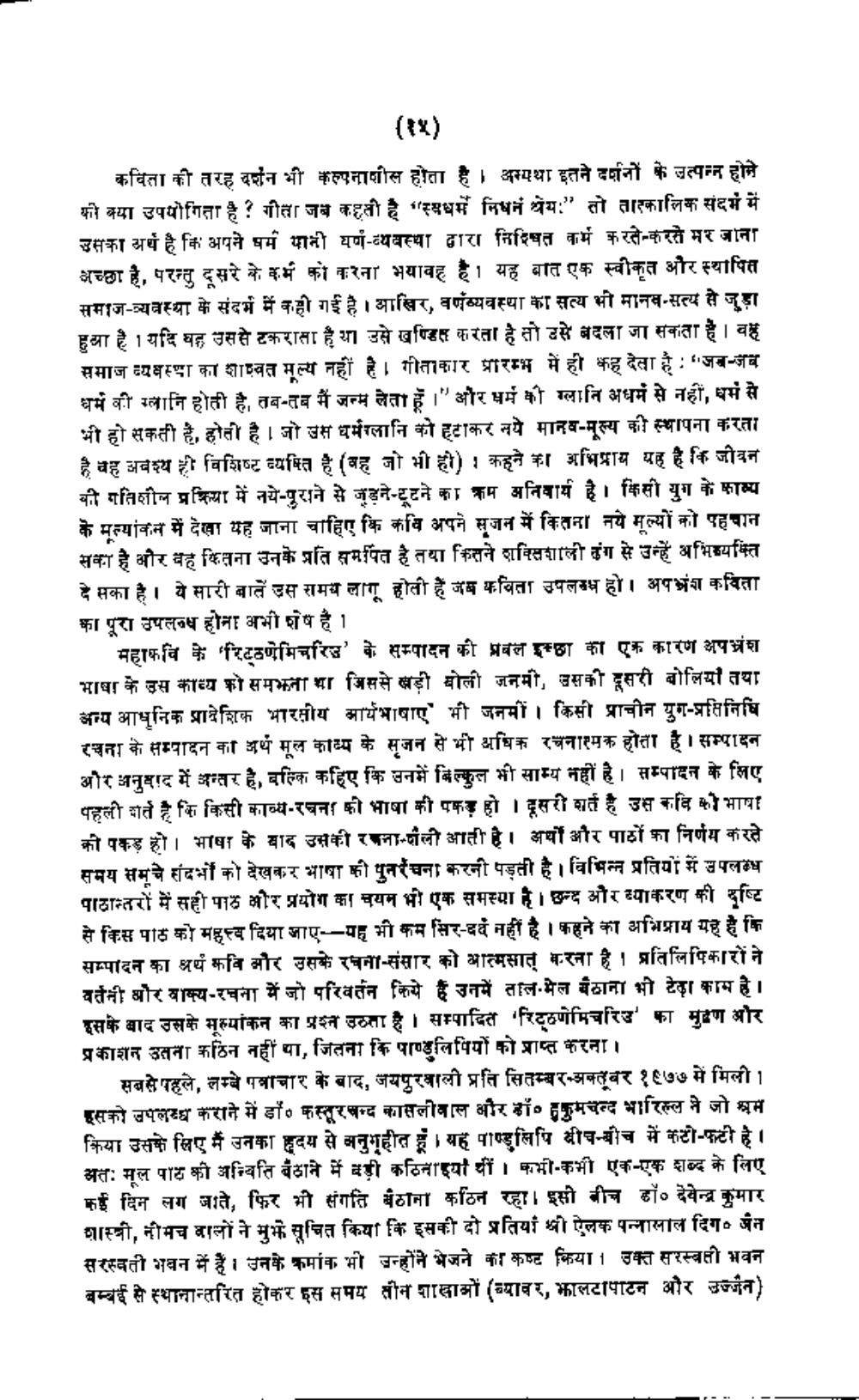________________
कविता की तरह दर्शन भी कल्पनाशीस होता है। अन्यथा इतने दर्शनों के उत्पन्न होने को क्या उपयोगिता है ? गीता जब कहती है "स्वधर्म निधनं थेयः" तो तात्कालिक संदर्भ में उसका अर्थ है कि अपने धर्म यानी वर्ण-व्यवस्था द्वारा निश्चित कर्म करते-करते मर जाना अच्छा है, परन्तु दूसरे के कर्म को करना भयावह है। यह बात एक स्वीकृत और स्थापित समाज-व्यवस्था के संदर्भ में कही गई है। आखिर, वर्णव्यवस्था का सत्य भी मानव-सत्य से जुड़ा हुआ है । यदि यह उससे टकरासा है या उसे खण्डित करता है तो उसे बदला जा सकता है। वह समाज व्यवस्था का शाश्वत मूल्य नहीं है। गीताकार प्रारम्भ में ही कह देता है : “जब-जब धर्म की ग्लानि होती है, तब-तब मैं जन्म लेता हूँ।" और धर्म की ग्लानि अधर्म से नहीं, धर्म से भी हो सकती है, होती है। जो उस धर्मग्लानि को हटाकर नये मानव-मूल्य की स्थापना करता है वह अवश्य ही विशिष्ट व्यक्ति है (वह जो भी हो) । कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन वी गतिशील प्रक्रिया में नये-पुराने से जुड़ने-टूटने का क्रम अनिवार्य है। किसी युग के फाम्प के मूल्यांकन में देखा यह जाना चाहिए कि कवि अपने सूजन में कितना नये मूल्यों को पहचान सका है और वह कितना उनके प्रति समर्पित है तया कितने शक्तिशाली ढंग से उन्हें अभिव्यक्ति दे सका है। ये सारी बातें उस समय लागू होती हैं जब कविता उपलब्ध हो। अपभ्रंश कविता का पूरा उपलब्ध होना अभी शेष है।
महाकवि के 'रिवणेमिचरित' के सम्पादन की प्रबल इक्छा का एक कारण अपभ्रंश भाषा के उस काव्य को समझना था जिससे खड़ी बोली जनमी, उसकी दूसरी बोलियो तथा अन्य आधुनिक प्रादेशिक भारतीय आर्यभाषाए' भी जनमी। किसी प्राचीन युग-प्रतिनिधि रचना के सम्पादन का अर्थ मूल काव्य के सृजन से भी अधिक रचनात्मक होता है। सम्पादन
और अनुवाद में अन्तर है, बल्कि कहिए कि उनमें बिल्कुल भी साम्य नहीं है। सम्पादन के लिए पहली बात है कि किसी काव्य-रचना की भाषा की पकड़ हो । दूसरी शर्त है उस कवि की भाषा को पकड़ हो। भाषा के बाद उसकी रचना-शैली आती है। अर्थों और पाठों का निर्णय करते समय समचे संदर्भो को देखकर भाषा की पुनर्रचना करनी पड़ती है। विभिन्न प्रतियों में उपलब्ध पाठान्तरों में सही पाठ और प्रयोग का चयम भी एक समस्या है। छन्द और व्याकरण की दृष्टि से किस पाठ को महत्त्व दिया जाए--यह भी कम सिर-दई नहीं है । कहने का अभिप्राय यह है कि सम्पादन का अर्थ कवि और उसके रचना-संसार को आत्मसात् करना है। प्रतिलिपिकारों ने वर्तनी और वाक्य-रचना में जो परिवर्तन किये हैं उनमें ताल-मेल बैठाना भी टेढ़ा काम है। इसके बाद उसके मूल्यांकन का प्रश्न उठता है । सम्पादित 'रिट्ठणेमिचरिउ' का मुद्रण और प्रकाशन उसना कठिन नहीं था, जितना कि पाण्डुलिपियों को प्राप्त करना।
सबसे पहले, लम्बे पत्राचार के बाद, जयपुरवाली प्रति सितम्बर-अक्तूबर १९७७ में मिली। इसको उपलब्ध कराने में डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल और डॉ० कुमचन्द भारिल्ल ने जो श्रम क्रिया उसके लिए मैं उनका हृदय से अनुगृहीत हूं। यह पाण्डुलिपि बीच-बीच में कटी-फटी है। अतः मूल पाट की अन्विति बैठाने में बड़ी कठिनाइयो थीं। कभी-कभी एक-एक शब्द के लिए कई दिन लग जाते, फिर भी संगति बैठाना कठिन रहा। इसी बीच डॉ. देवेन्द्र कुमार शास्त्री, नीमच वालों ने मुझे सूचित किया कि इसकी दो प्रतियां श्री ऐलक पन्नालाल दिग जैन सरस्वती भवन में हैं। उनके कमांक भी उन्होंने भेजने का कष्ट किया। उक्त सरस्वती भवन बम्बई से स्थानान्तरित होकर इस समय तीन शाखाओं (ब्यावर, झालटापाटन और उज्जैन)