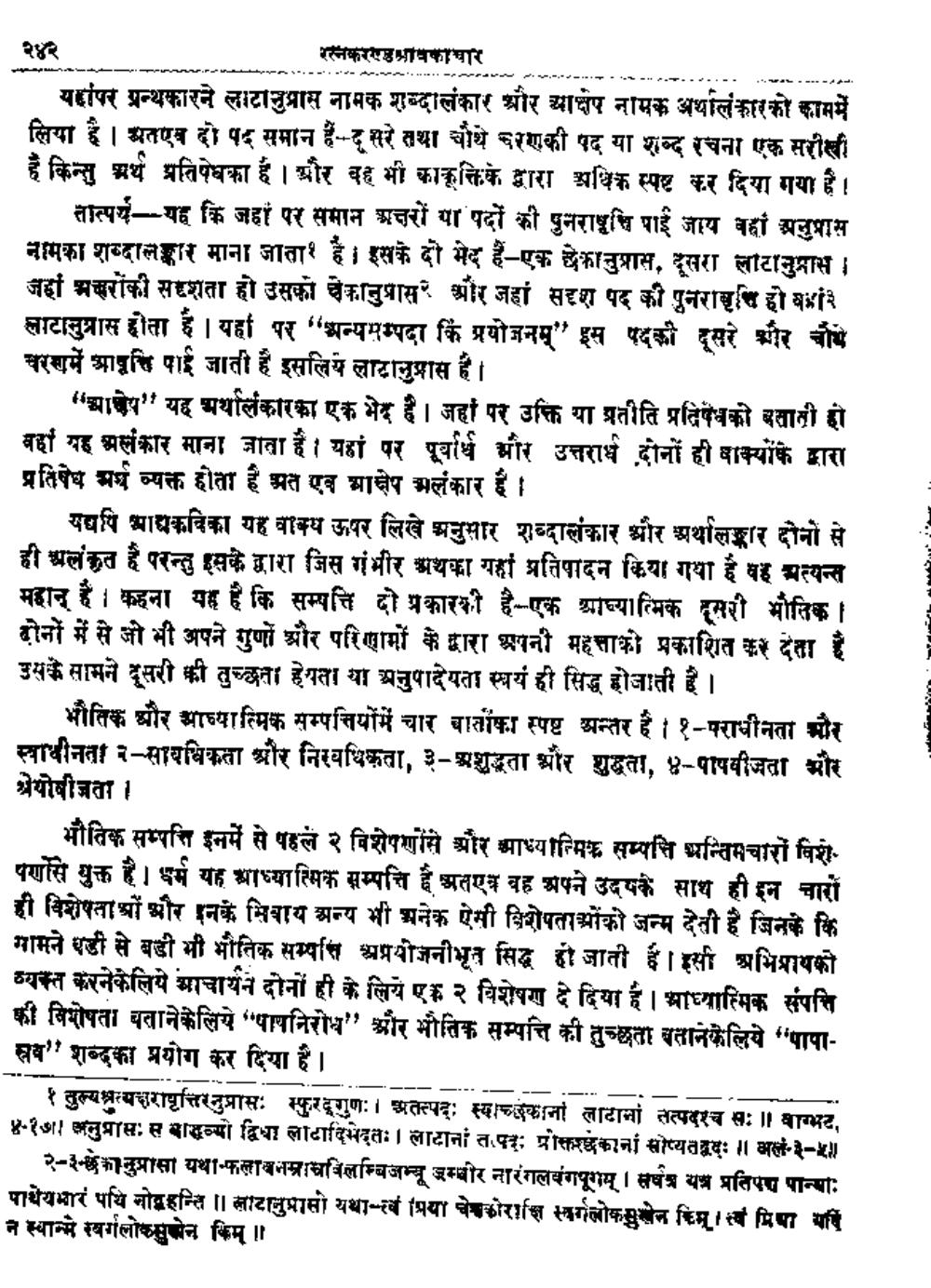________________
ર
रत्नकरण्ड श्रावकाचार
यहां पर ग्रन्थकारने लाटानुप्रास नामक शब्दालंकार और आक्षेप नामक अर्थालंकारको काममें लिया है । अतएव दो पद समान हैं-दूसरे तथा चौथे चरण की पद या शब्द रचना एक सरीखी है किन्तु अर्थ प्रतिषेधका है । और वह भी काकूक्तिके द्वारा अधिक स्पष्ट कर दिया गया है
!
--
तात्पर्य यह कि जहां पर समान अक्षरों या पदों की पुनरावृति पाई जाय वहां अनुप्रास नामका शब्दालङ्कार माना जाता हैं। इसके दो भेद हैं- एक छेकानुप्रास, दूसरा लाटानुप्रास । जहां अक्षरोंकी सदृशता हो उसको चेकानुप्रास और जहां सदृश पद की पुनरावृद्धि हो वहां लाटानुप्रास होता है | यहां पर "अन्यसम्पदा किं प्रयोजनम्" इस पदको दूसरे और चौथे वर में पाई जाती है इसलिये लाटानुप्रास है।
"च्याक्षेप" यह अर्थालंकारका एक भेद है। जहां पर उक्ति या प्रतीति प्रतिदेव को बताती हो वह यह अलंकार माना जाता है। यहां पर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ही वाक्योंके द्वारा प्रतिषेध अर्थ व्यक्त होता है अत एव आक्षेप अलंकार हैं।
यद्यपि श्राद्यकविका यह वाक्य ऊपर लिखे अनुसार शब्दालंकार और अर्थालङ्कार दोनों से ही अलंकृत है परन्तु इसके द्वारा जिस गंभीर अथका यहां प्रतिपादन किया गया है वह अत्यन्त महान् हैं। कहना यह है कि सम्पत्ति दो प्रकारकी है - एक आध्यात्मिक दूसरी भौतिक दोनों में से जो भी अपने गुणों और परिणामों के द्वारा अपनी महत्ताको प्रकाशित कर देता है उसके सामने दूसरी की तुच्छता हेयता या अनुपादेयता स्वयं ही सिद्ध होजाती है।
atre और Horroमक सम्पत्तियों में चार चातका स्पष्ट स्वाधीनता - साविकता और निरवधिकता, ३- श्रशुद्धता और श्रेयोवीजता ।
अन्तर है । १ - पराधीनता और शुद्धता, ४- पापवीजता और
भौतिक सम्पत्ति इनमें से पहले २ विशेषणोंसे और आध्यात्मिक सम्पत्ति अन्तिम चारों विशेपणास युक्त है। धर्म यह आध्यात्मिक सम्पत्ति है अतएव वह अपने उदयके साथ ही इन चारों ही विशेषताओं और इनके सिवाय अन्य भी अनेक ऐसी विशेषताओंको जन्म देती हैं जिनके कि मामने घडी से बड़ी भी भौतिक सम्पति अप्रयोजनीभूत सिद्ध हो जाती है। इसी अभिप्रायको व्यक्त करने के लिये आचार्यने दोनों ही के लिये एक २ विशेषण दे दिया है। आध्यात्मिक संपत्ति की विशेषता बतानेके लिये "पापनिरोध" और भौतिक सम्पत्ति की तुच्छता बतानेके लिये "पापाaa" शब्दका प्रयोग कर दिया है।
१ तुल्यश्रुत्यक्षरावृत्तिरनुप्रासः स्फुरद्गुणः । अतस्पदः स्याककानां लाटानां तत्पदश्च सः ॥ वाग्भट, ४-१७।। अनुप्रासः स बाद्धव्यो द्विधा लाटादिभेदतः । लाटानां तपः प्रोक्तकानां सोप्यतद्वदः ॥ अलं-३-५॥
२-३-कानुप्रासा यथा-फलाबनम्रात्रविलम्बिजम्बू जम्बीर नारंगलवंगपूगम् । सर्वत्र यत्र प्रतिपच पान्याः पाथेयभ्यारं पथि नोहन्ति || सायानुप्रासो यथा त्वं प्रिया वेचकोराशि स्वर्गलोकसुखेन किम् स्वं मिश्रा पि न स्वान्मे स्वर्गलोकसुसेन किम् ॥