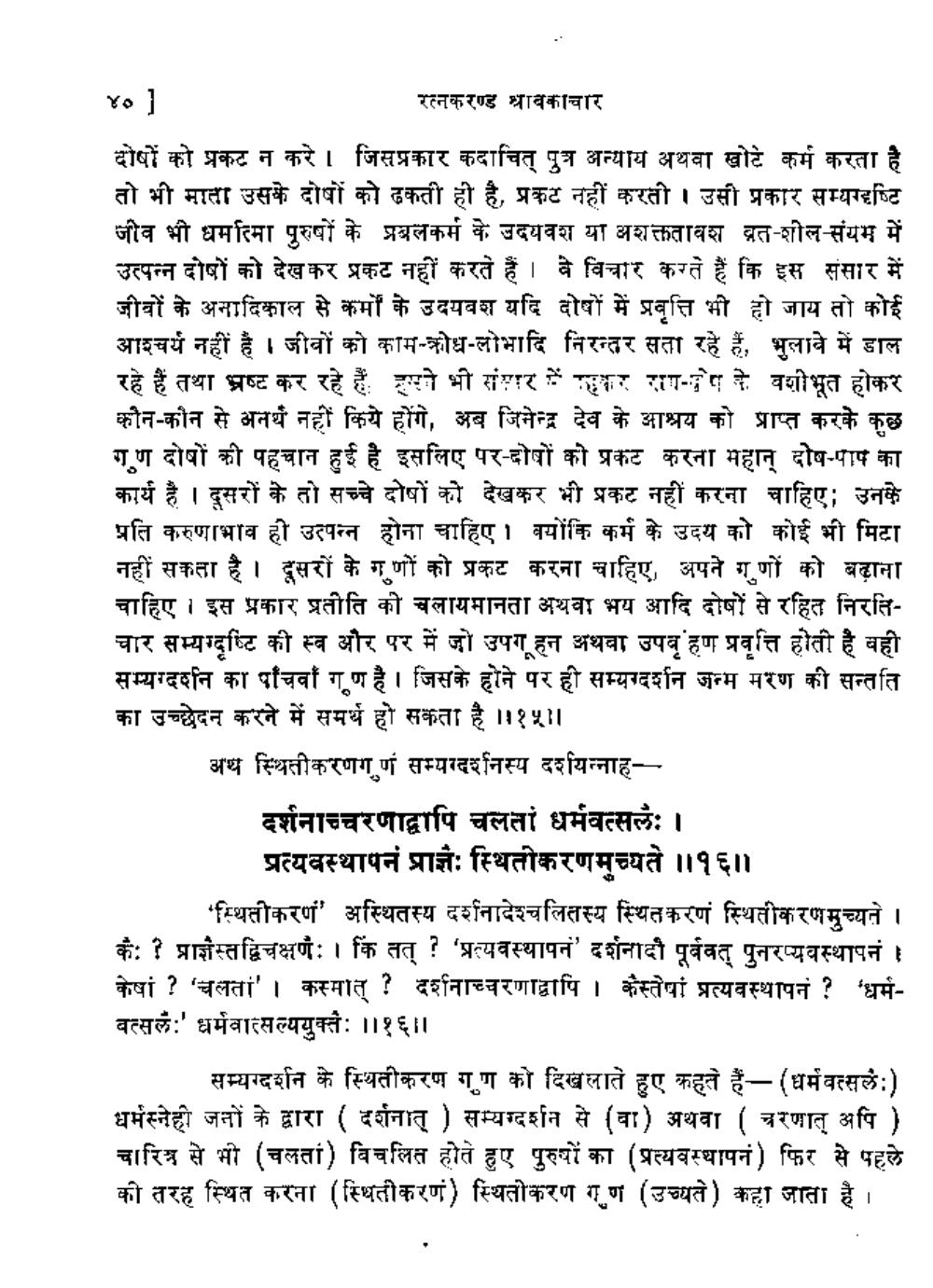________________
रत्नकरण्ड श्रावकाचार
४०] दोषों को प्रकट न करे । जिसप्रकार कदाचित् पुत्र अन्याय अथवा खोटे कर्म करता है तो भी माता उसके दोषों को ढकती ही है, प्रकट नहीं करती। उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव भी धर्मात्मा पुरुषों के प्रबलकर्म के उदयवश या अशक्ततावश व्रत-शील-संयम में उत्पन्न दोषों को देख कर प्रकट नहीं करते हैं । वे विचार करते हैं कि इस संसार में जीवों के अनादिकाल से कर्मों के उदयवश यदि दोषों में प्रवृत्ति भी हो जाय तो कोई आश्चर्य नहीं है । जीवों को काम-क्रोध-लोभादि निरन्तर सता रहे हैं, भुलावे में डाल रहे हैं तथा भ्रष्ट कर रहे हैं. हमो भी संपार हमारा पके वशीभूत होकर कौन-कौन से अनर्थ नहीं किये होंगे, अब जिनेन्द्र देव के आश्रय को प्राप्त करके कुछ गुण दोषों की पहचान हुई है इसलिए पर-दोषों को प्रकट करना महान् दोष-पाप का कार्य है । दूसरों के तो सच्चे दोषों को देखकर भी प्रकट नहीं करना चाहिए; उनके प्रति करुणाभाव ही उत्पन्न होना चाहिए। क्योंकि कर्म के उदय को कोई भी मिटा नहीं सकता है। दूसरों के गुणों को प्रकट करना चाहिए, अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए । इस प्रकार प्रतीति को चलायमानता अथवा भय आदि दोषों से रहित निरतिचार सम्यग्दृष्टि की स्व और पर में जो उपग हन अथवा उपबहण प्रवृत्ति होती है वहीं सम्यग्दर्शन का पांचवां ग ण है । जिसके होने पर ही सम्यग्दर्शन जन्म मरण की सन्तति का उच्छेदन करने में समर्थ हो सकता है ॥१५॥
अथ स्थितीकरणगणं सम्यग्दर्शनस्य दर्शयन्नाह
दर्शनाच्चरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलः ।
प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितीकरणमुच्यते ॥१६॥ "स्थितीकरण' अस्थितस्य दर्शनादेश्चलितस्य स्थितकरणं स्थितीकरणमुच्यते । कैः ? प्रास्तद्विचक्षणः । किं तत् ? 'प्रत्यवस्थापनं' दर्शनादी पूर्ववत् पुनरप्यवस्थापनं । केषां ? 'चलता'। कस्मात् ? दर्शनाच्चरणाद्वापि । कैस्तेषां प्रत्यवस्थापन ? 'धर्मबत्सल:' धर्मवात्सल्ययुक्तः ।।१६।।
सम्यग्दर्शन के स्थितीकरण गण को दिखलाते हुए कहते हैं-(धर्मवत्सल:) धर्मस्नेही जनों के द्वारा ( दर्शनात् ) सम्यग्दर्शन से (वा) अथवा ( चरणात् अपि ) चारित्र से भी (चलतां) बिचलित होते हुए पुरुषों का (प्रत्यवस्थापनं) फिर से पहले की तरह स्थित करना (स्थितीकरणं) स्थितीकरण ग ण (उच्यते) कहा जाता है।