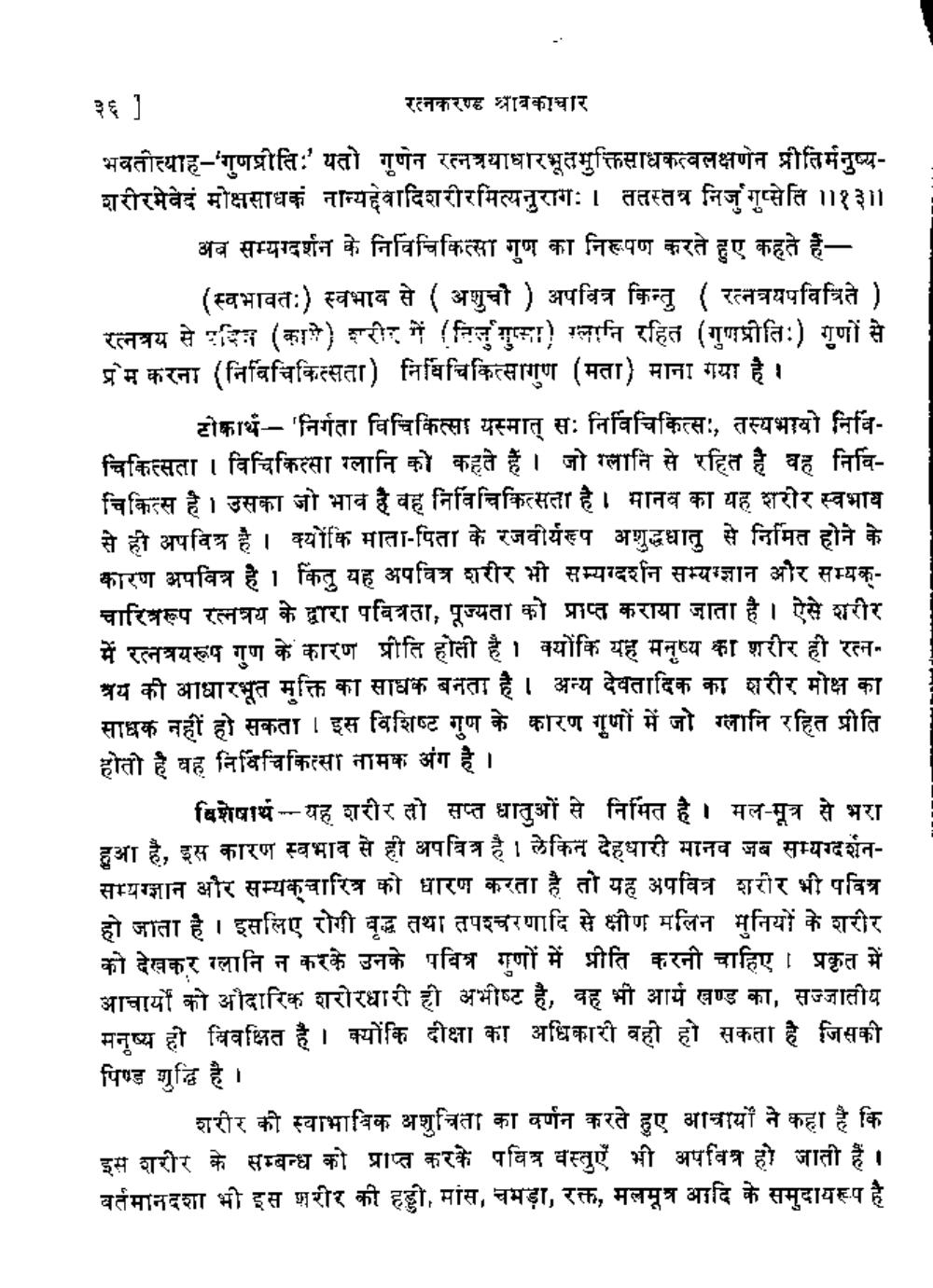________________
३६ ]
भवतीत्याह - 'गुणप्रीति' यतो गुणेन रत्नत्रयाधारभूतमुक्तिसाधकत्वलक्षणेन प्रीतिर्मनुष्यशरीरमेवेदं मोक्षसाधकं नान्यद्देवादिशरीरमित्यनुरागः । ततस्तत्र निर्जुगुप्सेति ||१३|| अब सम्यग्दर्शन के निविचिकित्सा गुण का निरूपण करते हुए कहते हैं
रत्नकरण्ड श्रावकाचार
( स्वभावतः ) स्वभाव से ( अशुचो ) अपवित्र किन्तु ( रत्नत्रयपवित्रिते ) रत्नत्रय से ( कार्य ) शरीर में (दिलु गुफा) ग्लानि रहित ( गुणप्रीतिः ) गुणों से प्रेम करना (निर्विचिकित्सता ) निर्विचिकित्सागुण ( मता ) माना गया है ।
टोकार्थ- 'निर्गता विचिकित्सा यस्मात् सः निर्विचिकित्सः, तस्यभावो निर्वि चिकित्सता । विचिकित्सा ग्लानि को कहते हैं । जो ग्लानि से रहित है वह निविचिकित्स है । उसका जो भाव है वह निर्विचिकित्सता है। मानव का यह शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है । क्योंकि माता-पिता के रजवीर्यरूप अशुद्धधातु से निर्मित होने के कारण अपवित्र है । किंतु यह अपवित्र शरीर भी सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रय के द्वारा पवित्रता, पूज्यता को प्राप्त कराया जाता है । ऐसे शरीर में रत्नत्रयरूप गुण के कारण प्रीति होती है। क्योंकि यह मनुष्य का शरीर ही रत्नश्रय की आधारभूत मुक्ति का साधक बनता है अन्य देवतादिक का शरीर मोक्ष का साधक नहीं हो सकता । इस विशिष्ट गुण के कारण गुणों में जो ग्लानि रहित प्रीति होती है वह निर्विचिकित्सा नामक अंग है ।
।
विशेषार्थ -- यह शरीर तो सप्त धातुओं से निर्मित है । मल-मूत्र से भरा हुआ है, इस कारण स्वभाव से ही अपवित्र है । लेकिन देहधारी मानव जब सम्यग्दर्शनसम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र को धारण करता है तो यह अपवित्र शरीर भी पवित्र हो जाता है । इसलिए रोगी वृद्ध तथा तपश्चरणादि से क्षीण मलिन मुनियों के शरीर को देखकर ग्लानि न करके उनके पवित्र गुणों में प्रीति करनी चाहिए। प्रकृत में आचार्यो को औदारिक शरीरधारी ही अभीष्ट है, वह भी आर्य खण्ड का, सज्जातीय मनुष्य हो विवक्षित है। क्योंकि दीक्षा का अधिकारी वही हो सकता है जिसकी पिण्ड शुद्धि है ।
शरीर की स्वाभाविक अशुचिता का वर्णन करते हुए आचार्यों ने कहा है कि इस शरीर के सम्बन्ध को प्राप्त करके पवित्र वस्तुएँ भी अपवित्र हो जाती हैं । वर्तमानदशा भी इस शरीर की हड्डी, मांस, चमड़ा, रक्त, मलमूत्र आदि के समुदायरूप है