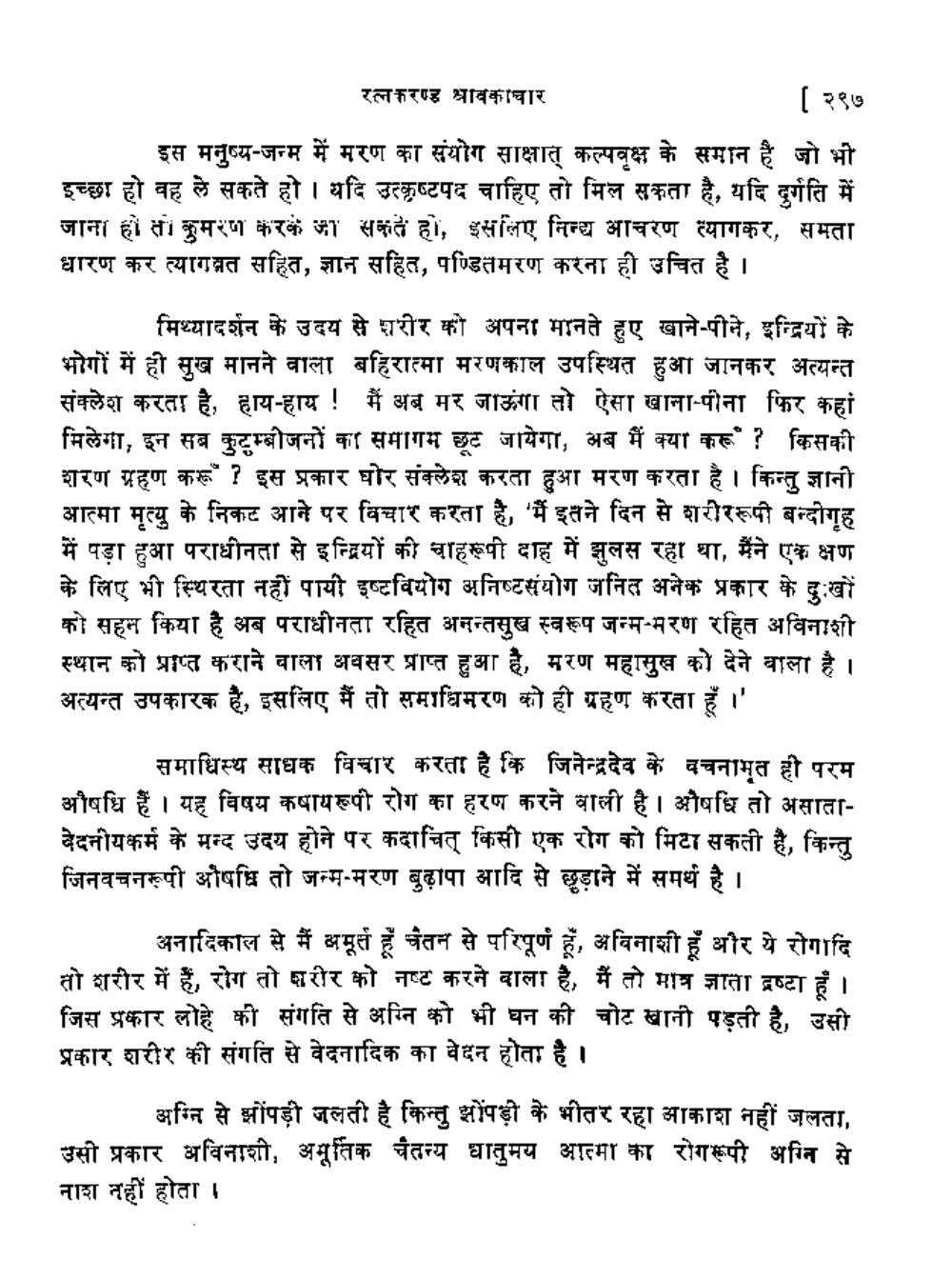________________
रत्नकरण्ड श्रावकाचार
इस मनुष्य-जन्म में मरण का संयोग साक्षात् कल्पवृक्ष के समान है जो भी इच्छा हो वह ले सकते हो । यदि उत्कृष्टपद चाहिए तो मिल सकता है, यदि दुर्गति में जाना हो ता कुमरण करके जा सकते हो, इसलिए निन्द्य आचरण त्यागकर, समता धारण कर त्यागनत सहित, ज्ञान सहित, पण्डितमरण करना ही उचित है ।
मिथ्यादर्शन के उदय से शरीर को अपना मानते हुए खाने-पीने, इन्द्रियों के भोगों में ही सुख मानने वाला बहिरात्मा मरणकाल उपस्थित हुआ जानकर अत्यन्त संक्लेश करता है, हाय-हाय ! मैं अब मर जाऊंगा तो ऐसा खाना-पीना फिर कहां मिलेगा, इन सब कुटुम्बीजनों का समागम छुट जायेगा, अब मैं क्या करूं ? किसकी शरण ग्रहण करू ? इस प्रकार घोर संक्लेश करता हुआ मरण करता है। किन्तु ज्ञानी आत्मा मृत्यु के निकट आने पर विचार करता है, 'मैं इतने दिन से शरीररूपी बन्दीगृह में पड़ा हुआ पराधीनता से इन्द्रियों की चाहरूपी दाह में झुलस रहा था, मैंने एक क्षण के लिए भी स्थिरता नहीं पायी इष्टवियोग अनिष्टसंयोग जनित अनेक प्रकार के दुःखों को सहन किया है अब पराधीनता रहित अनन्तसुख स्वरूप जन्म-मरण रहित अविनाशी स्थान को प्राप्त कराने वाला अवसर प्राप्त हुआ है, मरण महासुख को देने वाला है। अत्यन्त उपकारक है, इसलिए मैं तो समाधिमरण को ही ग्रहण करता हूँ।'
समाधिस्थ साधक विचार करता है कि जिनेन्द्रदेव के वचनामृत ही परम औषधि हैं । यह विषय कषायरूपी रोग का हरण करने वाली है । औषधि तो असातावेदनीयकर्म के मन्द उदय होने पर कदाचित् किसी एक रोग को मिटा सकती है, किन्तु जिनवचनरूपी औषधि तो जन्म-मरण बुढ़ापा आदि से छुड़ाने में समर्थ है ।
___ अनादिकाल से मैं अमूर्त हूँ चैतन से परिपूर्ण हूँ, अविनाशी हूँ और ये रोगादि तो शरीर में हैं, रोग तो शरीर को नष्ट करने वाला है, मैं तो मात्र ज्ञाता द्रष्टा हूँ। जिस प्रकार लोहे की संगति से अग्नि को भी धन की चोट खानी पड़ती है, उसी प्रकार शरीर की संगति से वेदनादिक का वेदन होता है ।
____ अग्नि से झोंपड़ी जलती है किन्तु झोंपड़ी के भीतर रहा आकाश नहीं जलता, उसी प्रकार अविनाशी, अमूर्तिक चैतन्य धातुमय आत्मा का रोगरूपी अग्नि से नाश नहीं होता।