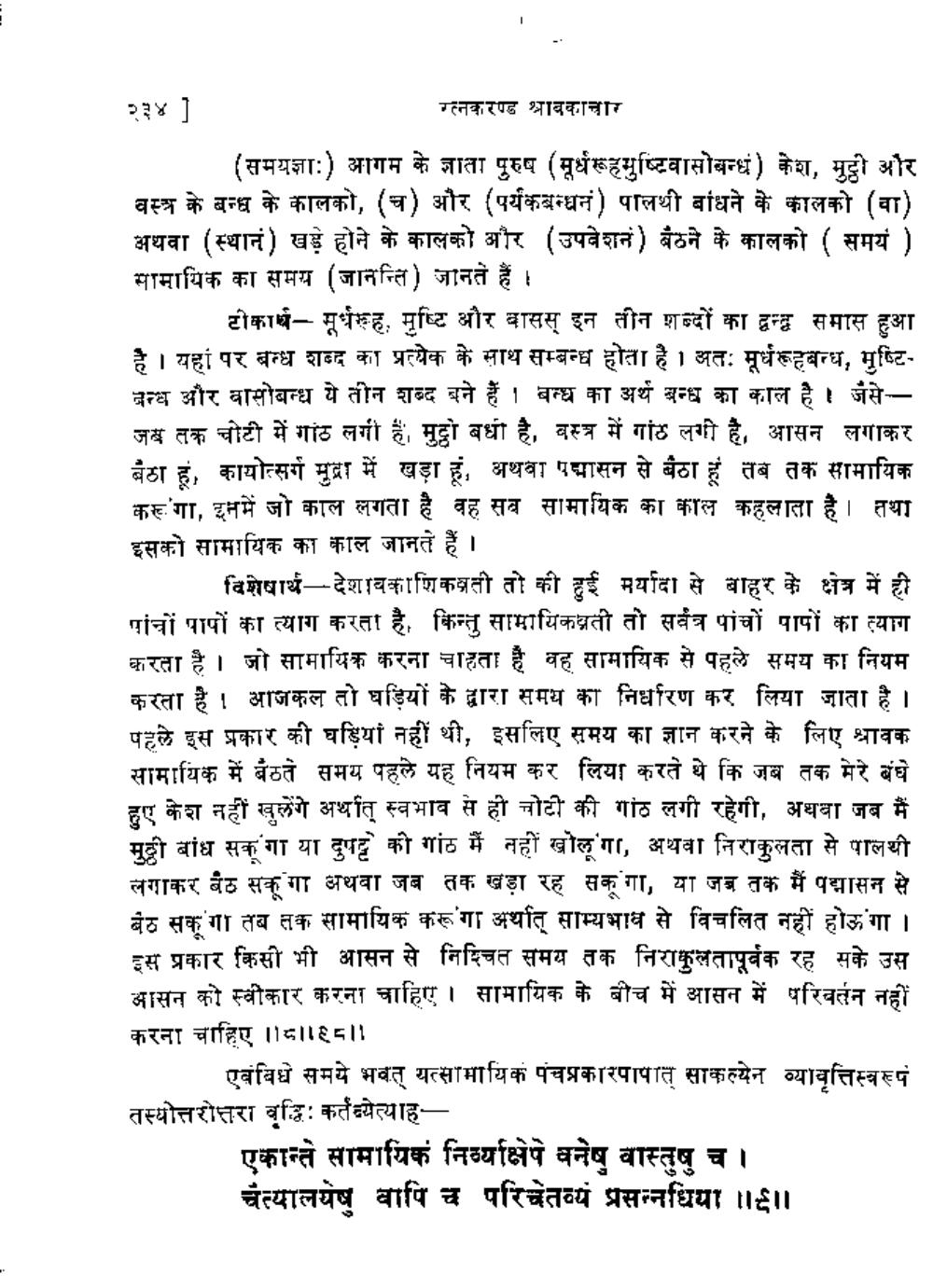________________
२३४ ]
रत्नकरण्ड श्रावकाचार (समयज्ञाः) आगम के ज्ञाता पुरुष (मूर्धरूहमुष्टिवासोबन्धं) केश, मुट्ठी और वस्त्र के बन्ध के कालको, (च) और (पर्यकबन्धनं) पालथी बांधने के कालको (वा) अथवा (स्थान) खड़े होने के कालको और (उपवेशनं) बैठने के कालको ( समयं ) मामायिक का समय (जानन्ति) जानते हैं।
टीकार्थ- मूर्धरुह, मुष्टि और बासस् इन तीन शब्दों का द्वन्द्व समास हुआ है। यहां पर बन्ध शब्द का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध होता है । अतः मूर्धरूहबन्ध, मुष्टिबन्ध और वासोबन्ध ये तीन शब्द बने हैं । बन्ध का अर्थ बन्ध का काल है। जैसेजब तक चोटी में गांठ लगी है। मुट्ठो बधी है, वस्त्र में गांठ लगी है, आसन लगाकर बैठा हूं, कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ा हूं, अथवा पद्मासन से बैठा हूं तब तक सामायिक करूगा, इनमें जो काल लगता है वह सब सामायिक का काल कहलाता है। तथा इसको सामायिक का काल जानते हैं ।
विशेषार्थ-देशावकाशिकवती तो की हुई मर्यादा से बाहर के क्षेत्र में ही पांचों पापों का त्याग करता है, किन्तु सामायिकन्नती तो सर्वत्र पांचों पापों का त्याग करता है। जो सामायिक करना चाहता है वह सामायिक से पहले समय का नियम करता है। आजकल तो घड़ियों के द्वारा समय का निर्धारण कर लिया जाता है। पहले इस प्रकार की घड़ियां नहीं थी, इसलिए समय का ज्ञान करने के लिए श्रावक सामायिक में बैठते समय पहले यह नियम कर लिया करते थे कि जब तक मेरे बंधे हए केश नहीं खुलेंगे अर्थात स्वभाव से ही चोटी की गांठ लगी रहेगी, अथवा जब मैं मठी बांध सकंगा या दुपट्टे को गांठ मैं नहीं खोलूगा, अथवा निराकुलता से पालथी लगाकर बैठ सकूगा अथवा जब तक खड़ा रह सकूगा, या जब तक मैं पद्मासन से बैठ सकगा तब तक सामायिक करूगा अर्थात् साम्यभाव से विचलित नहीं होऊंगा। इस प्रकार किसी भी आसन से निश्चित समय तक निराकुलतापूर्वक रह सके उस आसन को स्वीकार करना चाहिए। सामायिक के बीच में आसन में परिवर्तन नहीं करना चाहिए ।।८॥६॥
एवंबिधे समये भवत् यत्सामायिक पंचप्रकारपापात् साकल्येन व्यावृत्तिस्त्ररूपं तस्योत्तरोत्तरा वृद्धिः कर्तब्येत्याह
एकान्ते सामायिक निाक्षेपे वनेषु वास्तुषु च । चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया ॥६॥