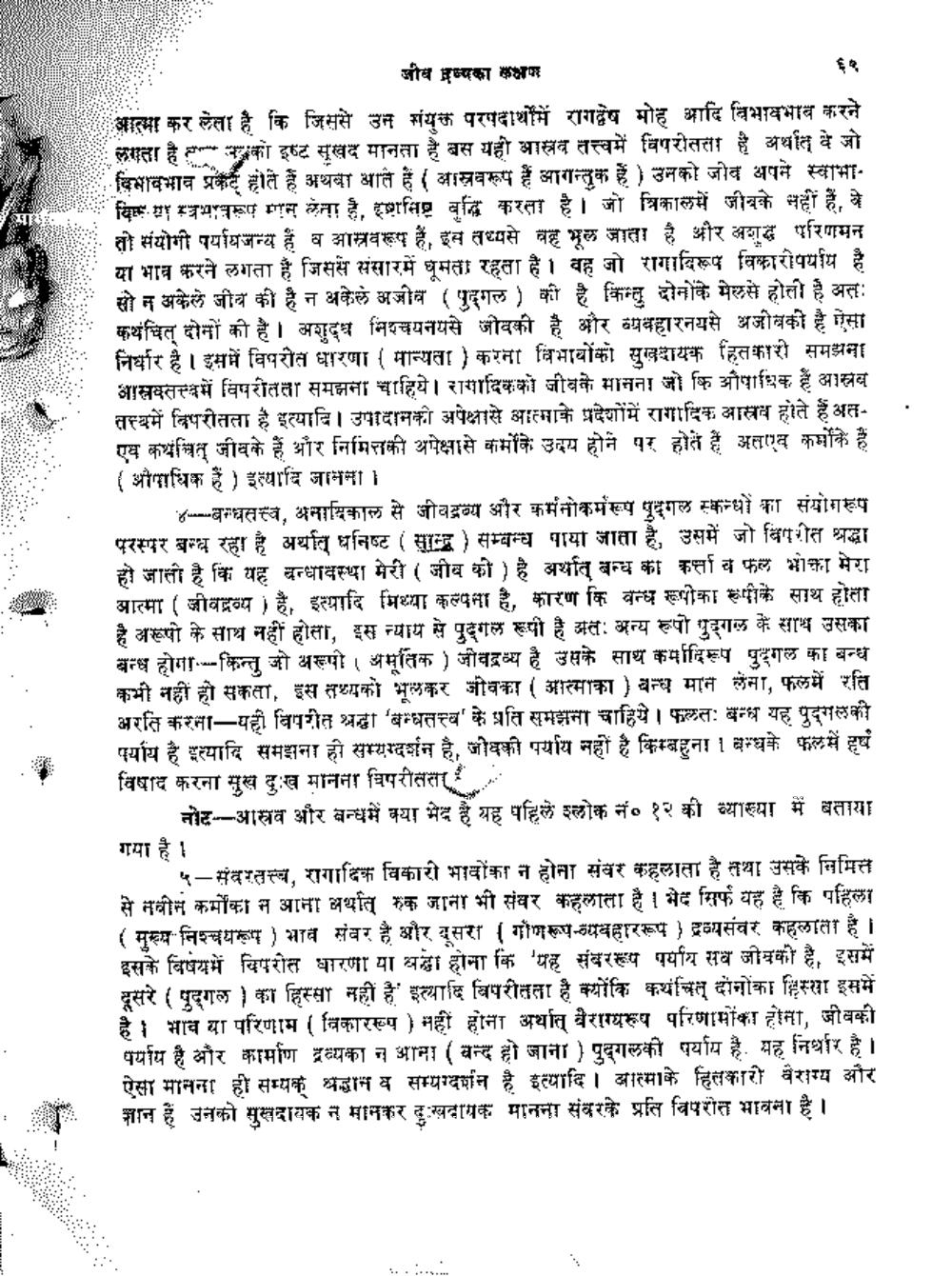________________
जीव व्यका कक्षा
आत्मा कर लेता है कि जिससे उन संयुक्त परपदार्थोंमें रागद्वेष मोह आदि विभावभाव करने लगता है को इष्ट सुखद मानता है बस यही आस्रव तत्त्वमें विपरीतत्ता है अर्थात वे जो विभावभाव प्रकट होते हैं अथवा आत हैं { आस्रवरूप हैं आगन्तुक हैं ) उनको जीव अपने स्वाभा. यिया स्वभावरूप मान लेता है, हासिष्ट बुद्धि करता है। जो त्रिकालमें जीवके नहीं हैं, के तो संयोगी पर्यायजन्य हैं व आम्रवरूप हैं, इस तथ्यसे वह भूल जाता है और अशुद्ध परिणमन या भाव करने लगता है जिससे संसारमें धमता रहता है। वह जो रागादिरूप विकारीपर्याय है सोन अकेले जीव की है न अकेले अजीव (पुद्गल ) की है किन्तु दोनोंके मेल से होती है अतः कथंचित् दोनों की है। अशुद्ध निश्चयनयसे जीवकी है और व्यवहारनयसे अजीबको है ऐसा निर्धार है । इसमें विपरीत धारणा ( मान्यता ) करना विभावोंको सुखदायक हितकारी समझना आसक्तत्वमें विपरीतता समझना चाहिये। रागादिकको जीबके मानना जो कि औपाधिक है आस्रब तत्त्वमें विपरीतता है इत्यादि । उपादानको अपेक्षासे आत्माके प्रदेशोंमें रागादिक आस्रव होते हैं अस्तएव कथंचित् जीवके हैं और निमित्तकी अपेक्षासे कर्मोके उदय होने पर होते हैं अतएव कर्मोके हैं ( औपाधिक हैं ) इत्यादि जानना ।
----बन्धसत्त्व, अनादिकाल से जीवद्रव्य और कमनोकर्मरूप पुद्गल स्कन्धों का संयोगरूप परस्पर बन्ध रहा है अर्थात् धनिष्ट ( सान्द्र) सम्बन्ध पाया जाता है, उसमें जो विपरीत श्रद्धा हो जाती है कि यह बन्धावस्था मेरी ( जीब को ) है अर्थात् बन्ध का कर्ता व फल भोका मेरा आत्मा ( जीवद्रव्य ) है, इत्यादि मिथ्या कल्पना है, कारण कि वन्ध रूपोका रूपीके साथ होता है अरूपी के साथ नहीं होता, इस न्याय से पुद्गल रूपी है अतः अन्य रूपो पुगल के साथ उसका बन्ध होगा---किन्तु जो अरूपी । अमूर्तिक ) जीवद्रव्य है उसके साथ कर्मादिरूप पुद्गल का बन्ध कभी नहीं हो सकता, इस तथ्यको भूलकर जीवका ( आरमाका )बन्ध मान लेना, फलमें रति अरति करना-यही विपरीत श्रद्धा 'बन्धतत्त्व' के प्रति समझना चाहिये। फलतः बन्ध यह पुद्गलकी पाय है इत्यादि समझाना ही सम्यग्दर्शन है, जोधकी पर्याय नहीं है किम्बहुना 1 बन्धके फल में हर्ष विषाद करना सुख दुःख मानना विपरीतता.
नोद-आस्रव और बन्धों क्या भेद है यह पहिले श्लोक नं०१२ की व्याख्या में बताया गया है।
५-संवरतत्व, रागादिक विकारी भावोंका न होना संवर कहलाता है तथा उसके निमित्त से नवीन कर्मोका न आना अर्थात् कक जाना भी संवर कहलाता है । भेद सिर्फ यह है कि पहिला ( मुख्य निश्चयरूप) भाव संवर है और दूसरा ( गौणरूप-व्यवहाररूप ) द्रव्यसंवर कहलाता है। इसके विषयमें विपरीत धारणा या बद्धा होना कि 'यह संवररूप पर्याय सब जीवको है, इसमें दूसरे ( पुद्गल ) का हिस्सा नहीं हैं इत्यादि विपरीतता है क्योंकि कथंचित् दोनोंका हिस्सा इसमें है। भाव या परिणाम ( विकाररूप ) नहीं होना अर्थात् वैराग्यरूप परिणामोंका होना, जीवकी पर्याय है और कार्माण द्रक्ष्यका च आना ( बन्द हो जाना ) पुद्गलकी पर्याय है. यह निर्धार है। ऐसा मानना ही सम्यक श्रद्धान व सम्यग्दर्शन है इत्यादि । आत्माके हितकारी वैराग्य और शान हैं उनको सुखदायक न मानकर दु:खदायक मानना संबर के प्रति विपरीत भावना है।