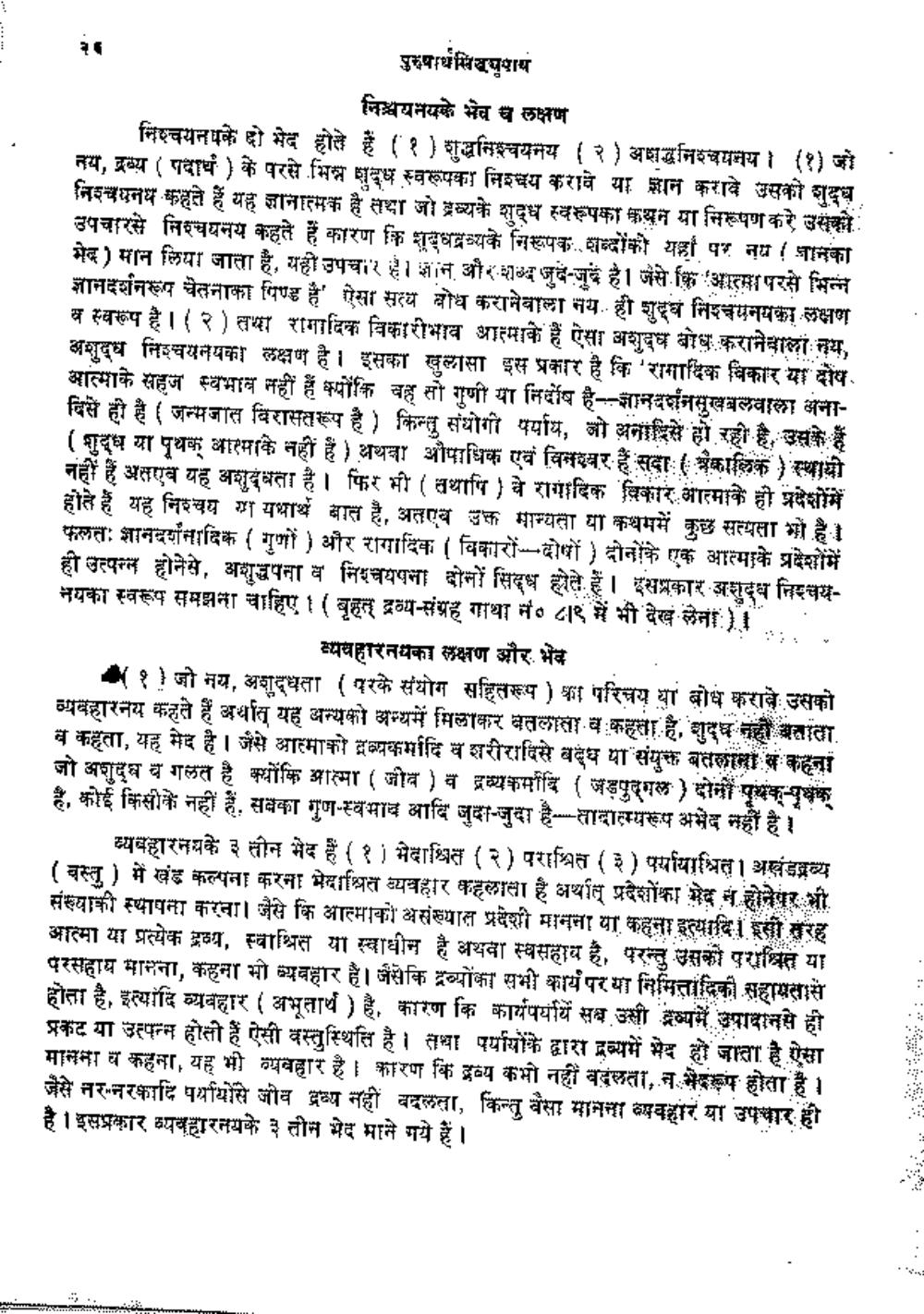________________
पुरुषार्थविश
निश्वयनयके भेव च लक्षण
froarrus दो भेद होते हैं ( १ ) शुद्धनिश्वयनय ( २ ) अशद्धनिश्चयनय । (१) जो तय, द्रव्य (पदार्थ) के परसे भिन्न शुद्ध स्वरूपका निश्चय करावे या ज्ञान करावे उसको शुध freeurs कहते हैं यह ज्ञानात्मक है तथा जो द्रव्यके शुद्ध स्वरूपका कथन या निरूपण करे उसको उपचारसे निश्चयनय कहते हैं कारण कि शुद्धद्रव्यके निरूपकः शब्दोको यहां पर न ( जानका भेद ) मान लिया जाता है, यही उपचार है। ज्ञान और शब्द जुदे जुड़े है। जैसे कि आत्मा परसे भिन्न ज्ञानदर्शनरूप चेतनाका frue है' ऐar are atध करानेवाला नय ही शुद्ध निश्चयनका लक्षण व स्वरूप है । ( २ ) तथा रामादिक विकारीभाव आत्मा हैं ऐसा अशुद्ध बोध करानेवाला नय अशुe fraurant लक्षण है। इसका खुलासा इस प्रकार है कि 'रामादिक विकार या दोष. आत्मा सहज स्वभाव नहीं हैं क्योंकि वह सो गुणी या निर्दोष है-- ज्ञानदर्शनसुखबलवाला अनादिसे हो है ( जन्मजात विरासतरूप है ) किन्तु संयोगी पर्याय, जो अनादिसे हो रही है, उसके हैं ( शुद्ध या पृथक आत्मा नहीं हैं ) अथवा औपाधिक एवं विनश्वर हैं सदा (कालिक ) स्थायी नहीं हैं अतएव यह अशुद्धता है। फिर भी ( तथापि ) वे रागादिक विकार आत्माके हो प्रदेशों में होते हैं यह निश्चय या यथार्थ बात है, अतएव उक्त मान्यता या कथममें कुछ सत्यता भो है । फलतः ज्ञानदर्शनादिक ( गुणों ) और रागादिक ( विकारों-दोषों ) दोनोंके एक आत्माके प्रदेशों में ही उत्पन्न होनेसे अशुद्धपना व निश्चयपना दोनों सिद्ध होते हैं। इसप्रकार अशुद्ध निश्चयनया स्वरूप समझना चाहिए ( बृहत् द्रव्य-संग्रह गाथा नं० दार में भी देख लेना ) ।
व्यवहारतका लक्षण और भेद
१) जो नय, अशुद्धता ( परके संयोग सहितरूप ) का परिचय या बोध करावे उसको व्यवहारनय कहते हैं अर्थात् यह अन्यको अन्यमें मिलाकर बतलाता व कहता है, शुद्ध नहीं बताता. व कहता, यह मेद है | जैसे आत्माको द्रव्यकर्मादि व शरीरादिसे बद्ध या संयुक्त बतलाना व कहना जो अशुद्ध व गलत है क्योंकि आत्मा (जीव ) व द्रव्यकर्मा ( जडपुदगल ) दोनों पृथक-पृथक है, कोई किसी नहीं हैं. सबका गुण-स्वभाव आदि जुदा-जुदा है- तादात्म्यरूप अभेद नहीं है ।
arearers ३ तीन भेद हैं ( १ ) भेदाश्रित ( २ ) पराश्रित (३) पर्यायाश्रित | अखंडद्रव्य ( वस्तु ) में खंड कल्पना करना मदाश्रित व्यवहार कहलाता है अर्थात् प्रदेशोंका मेद न होनेपर भी. संख्या स्थापना करना । जैसे कि आत्माको असंख्यात प्रदेशी मानना या कहना इत्यादि । इसी तरह आत्मा या प्रत्येक द्रव्य, स्वाश्रित या स्वाधीन है अथवा स्वसहाय है, परन्तु उसको पराश्रित या परसहाय मानना, कहना भी व्यवहार है। जैसेकि द्रव्योंका सभी कार्य परया निमित्तादिकी सहायता से होता है, इत्यादि व्यवहार ( अभूतार्थं ) है, कारण कि कार्यपर्यायें सब उसी द्रव्यमें उपादानसे ही प्रकट या उत्पन्न होती हैं ऐसी वस्तुस्थिति है । तथा पर्यायोंके द्वारा द्रव्यमें भेद हो जाता है ऐसा मानना व कहना, यह भी व्यवहार है। कारण कि द्रव्य कभी नहीं बदलता, न भेदरूप होता है । जैसे नर नरकादि पर्यायोसे जीव द्रव्य नहीं बदलता, किन्तु वैसा मानना व्यवहार या उपचार हो है । इसप्रकार व्यवहारयके ३ तीन भेद माने गये हैं ।