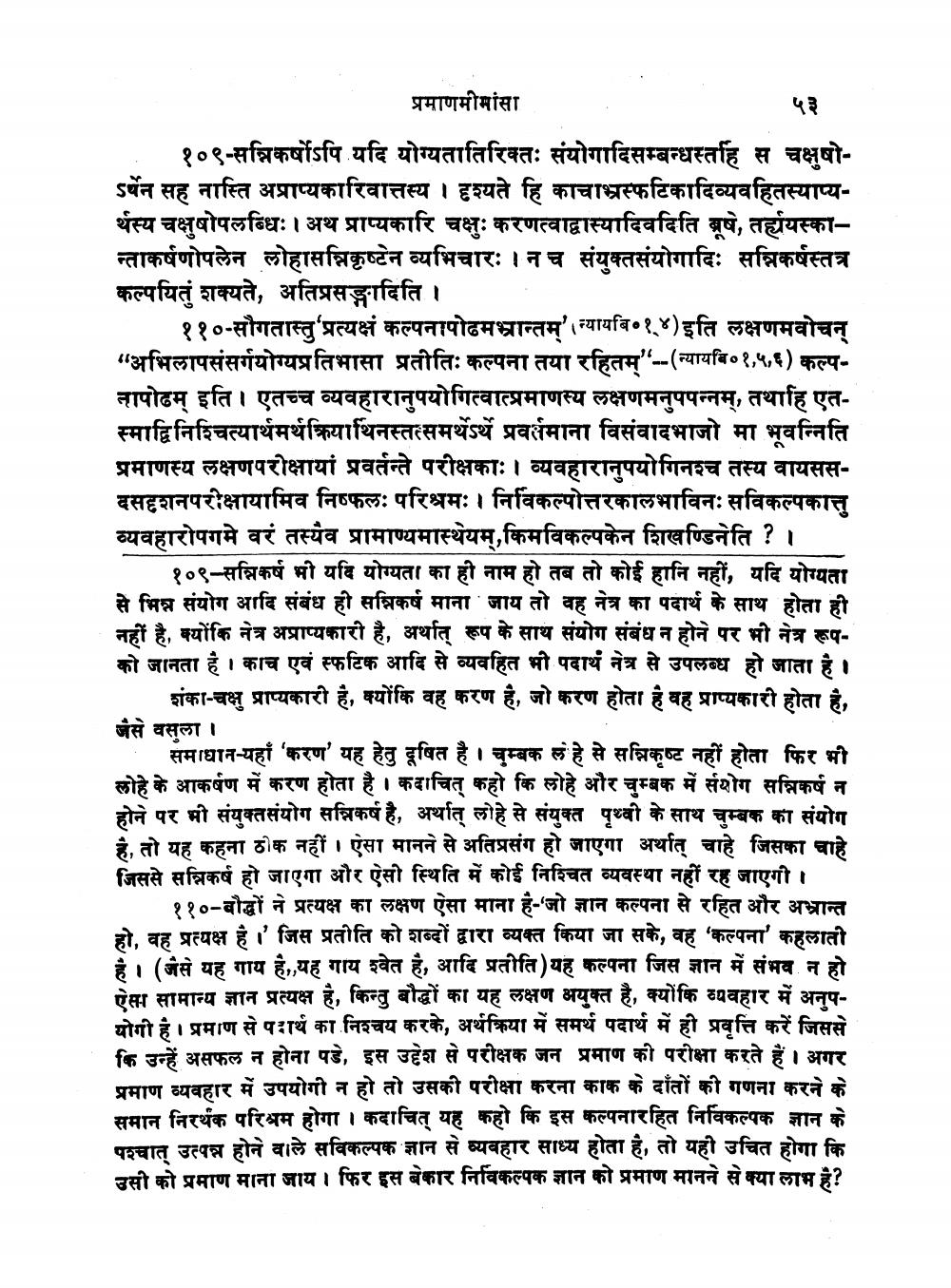________________
प्रमाणमीमांसा
५३ १०९-सन्निकर्षोऽपि यदि योग्यतातिरिक्तः संयोगादिसम्बन्धस्तहि स चक्षुषोऽर्थेन सह नास्ति अप्राप्यकारिवात्तस्य । दृश्यते हि काचाभ्रस्फटिकादिव्यवहितस्याप्यर्थस्य चक्षुषोपलब्धिः। अथ प्राप्यकारि चक्षुः करणत्वाद्वास्यादिवदिति ब्रूषे, तमुयस्कान्ताकर्षणोपलेन लोहासनिकृष्टेन व्यभिचारः । न च संयुक्तसंयोगादिः सन्निकर्षस्तत्र कल्पयितुं शक्यते, अतिप्रसङ्गादिति ।
११०-सौगतास्तु प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तम्' न्यायबि०१४) इति लक्षणमवोचन् "अभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना तया रहितम्"-(न्यायबि०१,५,६) कल्पनापोढम् इति । एतच्च व्यवहारानुपयोगित्वात्प्रमाणस्य लक्षणमनुपपन्नम्, तथाहि एतस्माद्विनिश्चित्यार्थमर्थक्रियार्थिनस्तत्समर्थेऽर्थे प्रवर्तमाना विसंवादभाजो मा भूवन्निति प्रमाणस्य लक्षणपरीक्षायां प्रवर्तन्ते परीक्षकाः। व्यवहारानुपयोगिनश्च तस्य वायससदसद्दशनपरीक्षायामिव निष्फलः परिश्रमः । निर्विकल्पोत्तरकालभाविनः सविकल्पकात्तु व्यवहारोपगमे वरं तस्यैव प्रामाण्यमास्थेयम्,किमविकल्पकेन शिखण्डिनेति ? ।
१०९-सन्निकर्ष भी यदि योग्यता का ही नाम हो तब तो कोई हानि नहीं, यदि योग्यता से भिन्न संयोग आदि संबंध ही सन्निकर्ष माना जाय तो वह नेत्र का पदार्थ के साथ होता ही नहीं है, क्योंकि नेत्र अप्राप्यकारी है, अर्थात् रूप के साथ संयोग संबंध न होने पर भी नेत्र रूपको जानता है । काच एवं स्फटिक आदि से व्यवहित भी पदार्थ नेत्र से उपलब्ध हो जाता है।
शंका-चक्षु प्राप्यकारी है, क्योंकि वह करण है, जो करण होता है वह प्राप्यकारी होता है, जैसे वसुला। . समाधान-यहाँ 'करण' यह हेतु दूषित है । चुम्बक ले हे से सन्निकृष्ट नहीं होता फिर भी लोहे के आकर्षण में करण होता है । कदाचित् कहो कि लोहे और चुम्बक में संयोग सन्निकर्ष न होने पर भी संयुक्तसंयोग सन्निकर्ष है, अर्थात् लोहे से संयुक्त पृथ्वी के साथ चुम्बक का संयोग है, तो यह कहना ठीक नहीं । ऐसा मानने से अतिप्रसंग हो जाएगा अर्थात् चाहे जिसका चाहे जिससे सन्निकर्ष हो जाएगा और ऐसी स्थिति में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं रह जाएगी।
११०-बौद्धों ने प्रत्यक्ष का लक्षण ऐसा माना है-'जो ज्ञान कल्पना से रहित और अभ्रान्त वह प्रत्यक्ष है। जिस प्रतीति को शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सके, वह 'कल्पना' कहलाती है। (जैसे यह गाय है,,यह गाय श्वेत है, आदि प्रतीति) यह कल्पना जिस ज्ञान में संभव न हो ऐसा सामान्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, किन्तु बौद्धों का यह लक्षण अयुक्त है, क्योंकि व्यवहार में अनुपयोगी है। प्रमाण से पदार्थ का निश्चय करके, अर्थक्रिया में समर्थ पदार्थ में ही प्रवृत्ति करें जिससे कि उन्हें असफल न होना पडे, इस उद्देश से परीक्षक जन प्रमाण की परीक्षा करते हैं। अगर प्रमाण व्यवहार में उपयोगी न हो तो उसकी परीक्षा करना काक के दाँतों की गणना करने के समान निरर्थक परिश्रम होगा। कदाचित् यह कहो कि इस कल्पनारहित निर्विकल्पक ज्ञान के पश्चात उत्पन्न होने वाले सविकल्पक ज्ञान से व्यवहार साध्य होता है, तो यही उचित होगा कि उसी को प्रमाण माना जाय। फिर इस बेकार निर्विकल्पक ज्ञान को प्रमाण मानने से क्या लाभ?
वर