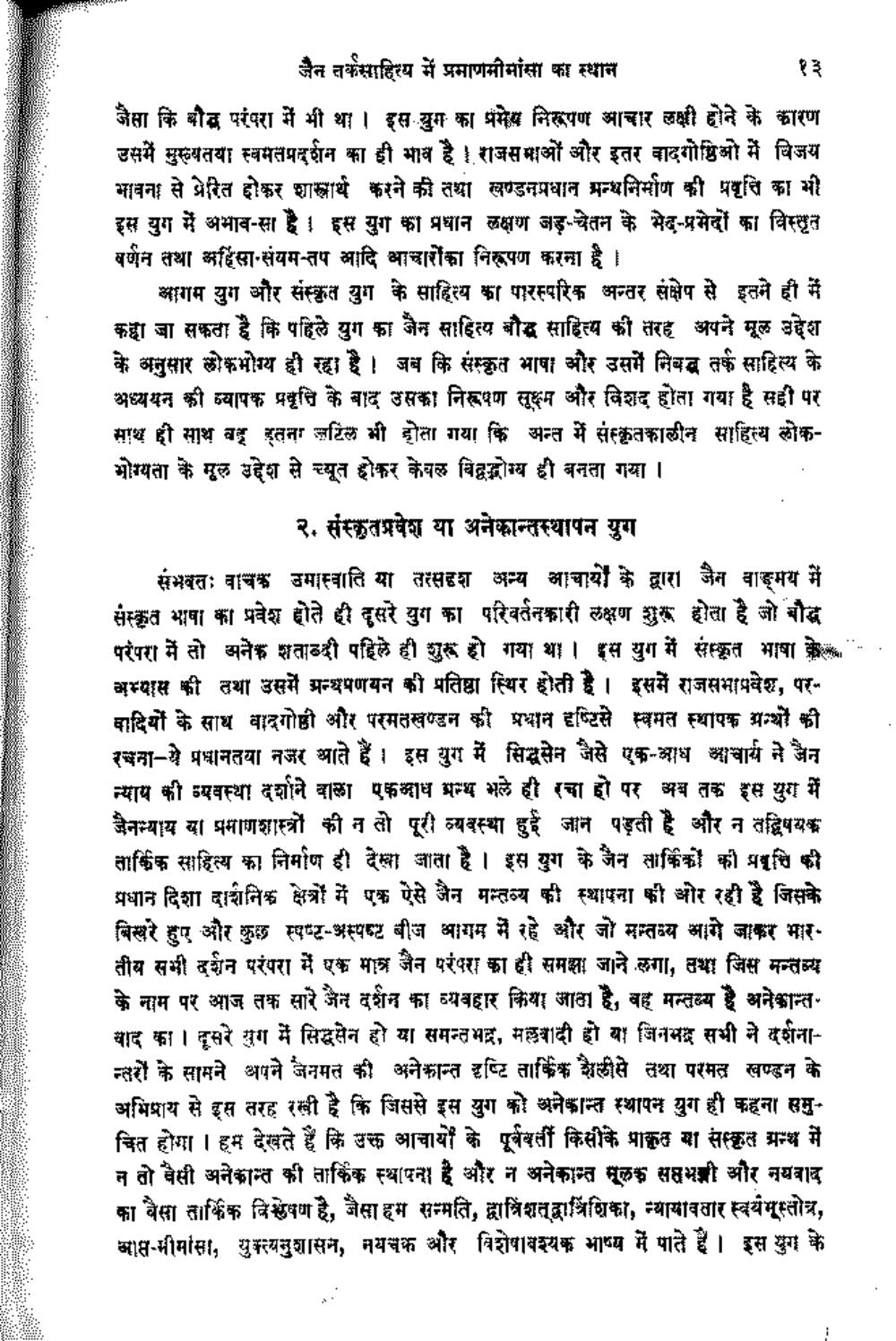________________
Heasilsina
जैन तर्कसाहित्य में प्रमाणमीमांसा का स्थान जैसा कि बौद्ध परंपरा में भी था। इस युग का प्रमेय निरूपण आचार लक्षी होने के कारण उसमें मुख्यतया स्वमतप्रदर्शन का ही भाव है ! राजसमाओं और इतर वादगोष्ठिओ में विजय भावना से प्रेरित होकर शास्त्रार्थ करने की तथा खण्डनप्रधान अन्धनिर्माण की प्रवृत्ति का भी इस युग में अभाव-सा है। इस युग का प्रधान लक्षण जड़-चेतन के भेद-प्रमेदों का विस्तृत वर्णन तथा अहिंसा-संयम-तप आदि आचारोंका निरूपण करना है।
आगम युग और संस्कृत युग के साहित्य का पारस्परिक अन्तर संक्षेप से इतने ही में कहा जा सकता है कि पहिले युग का जैन साहित्य बौद्ध साहित्य की तरह अपने मूल उद्देश के अनुसार लोकभोग्य ही रहा है। जब कि संस्कृत भाषा और उसमें निबद्ध तर्क साहित्य के अध्ययन की व्यापक प्रवृत्ति के बाद उसका निरूपण सूक्ष्म और विशद होता गया है सही पर माथ ही साथ वह इतना जटिल भी होता गया कि अन्त में संस्कृतकालीन साहित्य लोकभोग्यता के मूल उद्देश से च्यूत होकर केवल विद्वद्भोग्य ही बनता गया ।
Paymensahindi
२. संस्कृतप्रवेश या अनेकान्तस्थापन युग संभवतः वाचा उमास्वाति या तत्सहश अन्य आचार्यों के द्वारा जैन वाङ्मय में संस्कृत भाषा का प्रवेश होते ही दुसरे युग का परिवर्तनकारी लक्षण शुरू होता है जो बौद्ध परंपरा में तो अनेक शताब्दी पहिले ही शुरू हो गया था। इस युग में संस्कृत भाषा केला. ... अभ्यास की तथा उसमें ग्रन्थपणयन की प्रतिष्ठा स्थिर होती है। इसमें राजसभाप्रवेश, परवादियों के साथ वादगोही और परमतखण्डन की प्रधान दृष्टिसे स्वमत स्थापक अन्थों की रचना-ये प्रधानतया नजर आते हैं। इस युग में सिद्धसेन जैसे एक-आध आचार्य ने जैन न्याय की व्यवस्था दर्शाने वाला एकमाध अन्य भले ही रचा हो पर अब तक इस युग में जैनन्याय या प्रमाणशास्त्रों की न तो पूरी व्यवस्था हुई जान पड़ती है और न तद्विषयक तार्किक साहित्य का निर्माण ही देखा जाता है । इस युग के जैन सार्किको की प्रवृत्ति की प्रधान दिशा दार्शनिक क्षेत्रों में एक ऐसे जैन मन्तव्य की स्थापना की ओर रही है जिसके बिखरे हुए और कुछ स्पष्ट-अस्पष्ट बीज भागम में रहे और जो मन्तव्य आगे जाकर भार. तीय सभी दर्शन परंपरा में एक मात्र जैन परंपरा का ही समझा जाने लगा, तथा जिस मन्तव्य के नाम पर आज तक सारे जैन दर्शन का व्यवहार किया जाता है, वह मन्तव्य है अनेकान्त. वाद का। दूसरे युग में सिद्धसेन हो या समन्तभद्र, मल्लवादी हो या जिनमद सभी ने दर्शनान्तरों के सामने अपने जैनमत्त की अनेकान्त दृष्टि तार्किक शैलीसे तथा परमत खण्डन के
अभिप्राय से इस तरह रखी है कि जिससे इस युग को अनेकान्त स्थापन युग ही कहना समु. चित होगा । हम देखते हैं कि उक्त आचार्यों के पूर्ववती किसीके प्राकृत या संस्कृत ग्रन्थ में न तो वैसी अनेकान्त की तार्किक स्थापना है और न अनेकान्त मूलक सप्तमनी और नयवाद का वैसा तार्किक विश्लेषण है, जैसा हम सन्मति, द्वात्रिंशत्वात्रिंशिका, न्यायावतार स्वयंमस्तोत्र, आस-मीमांसा, युक्त्यनुशासन, नयचक और विशेषावश्यक भाष्य में पाते है। इस युग के