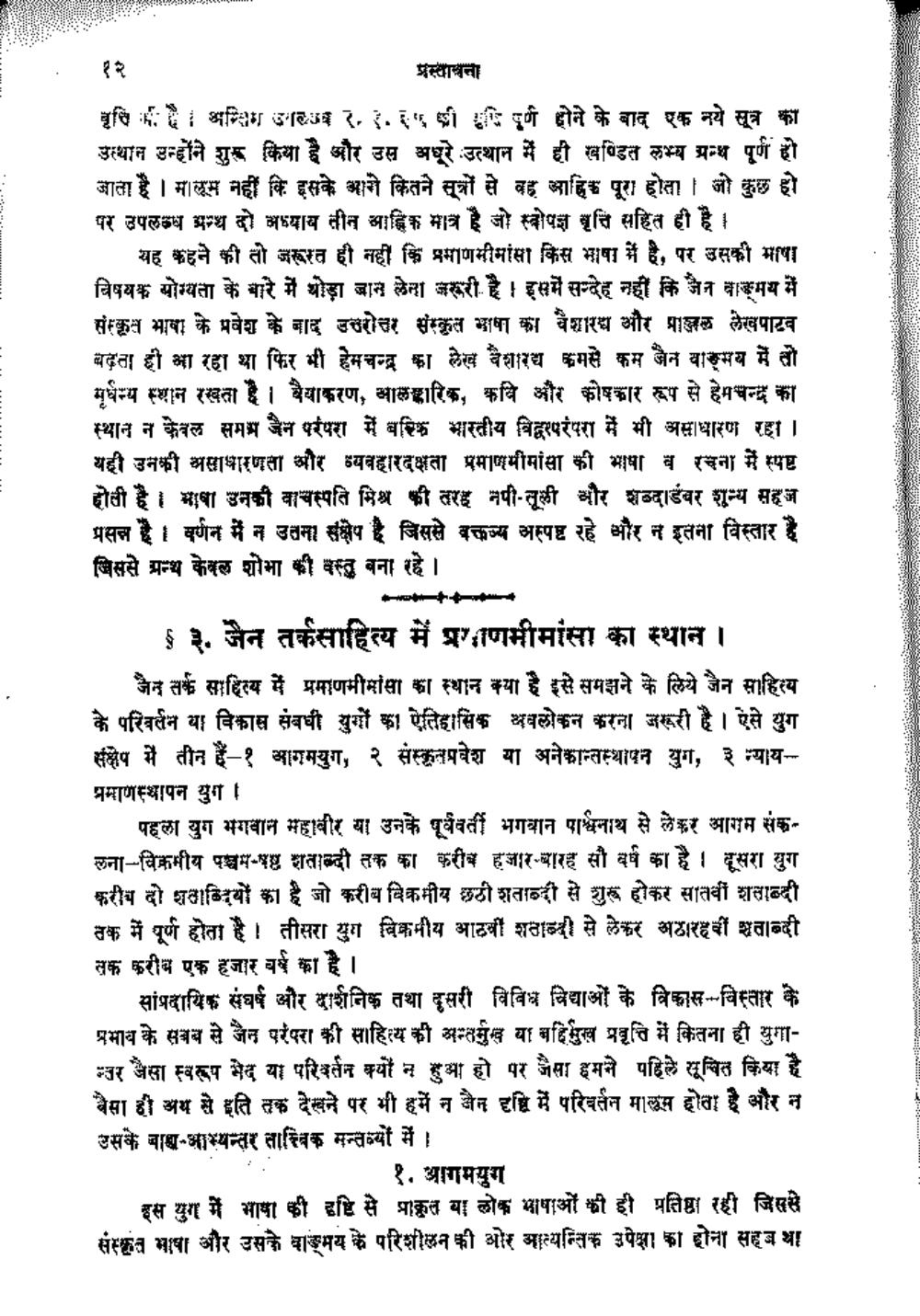________________
वृत्ति है। असिम ल २, १.६." श्री मति पूर्ण होने के बाद एक नये सूत्र का उत्थान उन्होंने शुरू किया है और उस अधूरे उत्थान में ही खण्डित लभ्य ग्रन्थ पूर्ण हो जाता है । मालूम नहीं कि इसके आगे कितने सूत्रों से वह आहिक पूरा होता । जो कुछ हो पर उपलब्ध अन्य दो अध्याय तीन आह्निक मात्र है जो स्वोपज्ञ वृत्ति सहित ही है ।।
यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि प्रमाणमीमांसा किस भाषा में है, पर उसकी भाषा विषयक योग्यता के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। इसमें सन्देह नहीं कि जैन वाङ्मय में संस्कृत भाषा के प्रवेश के बाद उत्तरोत्तर संस्कृत भाषा का वैशारध और पाजल लेखपाटव बढ़ता ही आ रहा था फिर भी हेमचन्द्र का लेख वैशारच कमसे कम जैन वाङ्मय में तो मृर्धन्य स्थान रखता है। वैयाकरण, आलङ्कारिक, कवि और कोषकार रूप से हेमचन्द्र का स्थान न केवल समन जैन परंपरा में बरिक भारतीय विद्वरपरंपरा में भी असाधारण रहा । यही उनकी असाधारणता और व्यवहारदक्षता प्रमाणमीमांसा की भाषा व रचना में स्पष्ट होती है। भाषा उनकी वाचस्पति मिश्र की तरह नपी-तूली और शब्दाडंबर शुन्य सहज प्रसन्न है। वर्णन में न उत्तमा संक्षेप है जिससे वक्तव्य अस्पष्ट रहे और न इतना विस्तार है जिससे ग्रन्थ केवल शोभा की वस्तु बना रहे।
३. जैन तर्कसाहित्य में प्राणमीमांसा का स्थान । जैन सर्क साहित्य में प्रमाणमीमांसा का स्थान क्या है इसे समझने के लिये जैन साहित्य के परिवर्तन या विकास संबधी युगों का ऐतिहासिक अवलोकन करना जरूरी है। ऐसे युग संक्षेप में तीन हैं-१ आगमयुग, २ संस्कृतप्रवेश या अनेकान्तस्थापन युग, ३ न्यायप्रमाणस्थापन युग। ___ पहला युग भगवान महावीर या उनके पूर्ववर्ती भगवान पाश्चनाथ से लेकर आगम संकलना-विक्रमीय पञ्चम-पष्ट शताब्दी तक का करीब हजार-बारह सौ वर्ष का है। दूसरा युग करीब दो शताब्दियों का है जो करीब विक्रमीय छठी शताब्दी से शुरू होकर सातवीं शताब्दी तक में पूर्ण होता है। तीसरा युग विक्रमीय आठवीं शताब्दी से लेकर अठारहवीं शताब्दी तक करीब एक हजार वर्ष का है।
सांप्रदायिक संघर्ष और दार्शनिक तथा दुसरी विविध विद्याओं के विकास-विस्तार के प्रभाव के सबब से जैन परंपरा की साहित्य की अन्तर्मुख या बहिर्मुख प्रवृत्ति में कितना ही युगातर जैसा स्वरूप भेद या परिवर्तन क्यों न हुआ हो पर जैसा हमने पहिले सूचित किया है वैसा ही अब से इति तक देखने पर भी हमें न जैन दृष्टि में परिवर्तन मालूम होता है और न उसके बाद्य-आभ्यन्तर तास्विक मन्तव्यों में।
१. आगमयुग इस युग में भाषा की दृष्टि से प्राकृत या लोक भाषाओं की ही प्रतिष्ठा रही जिससे संस्कृत भाषा और उसके वाङ्मय के परिशीलन की ओर आत्यन्तिक उपेक्षा का होना सहज था