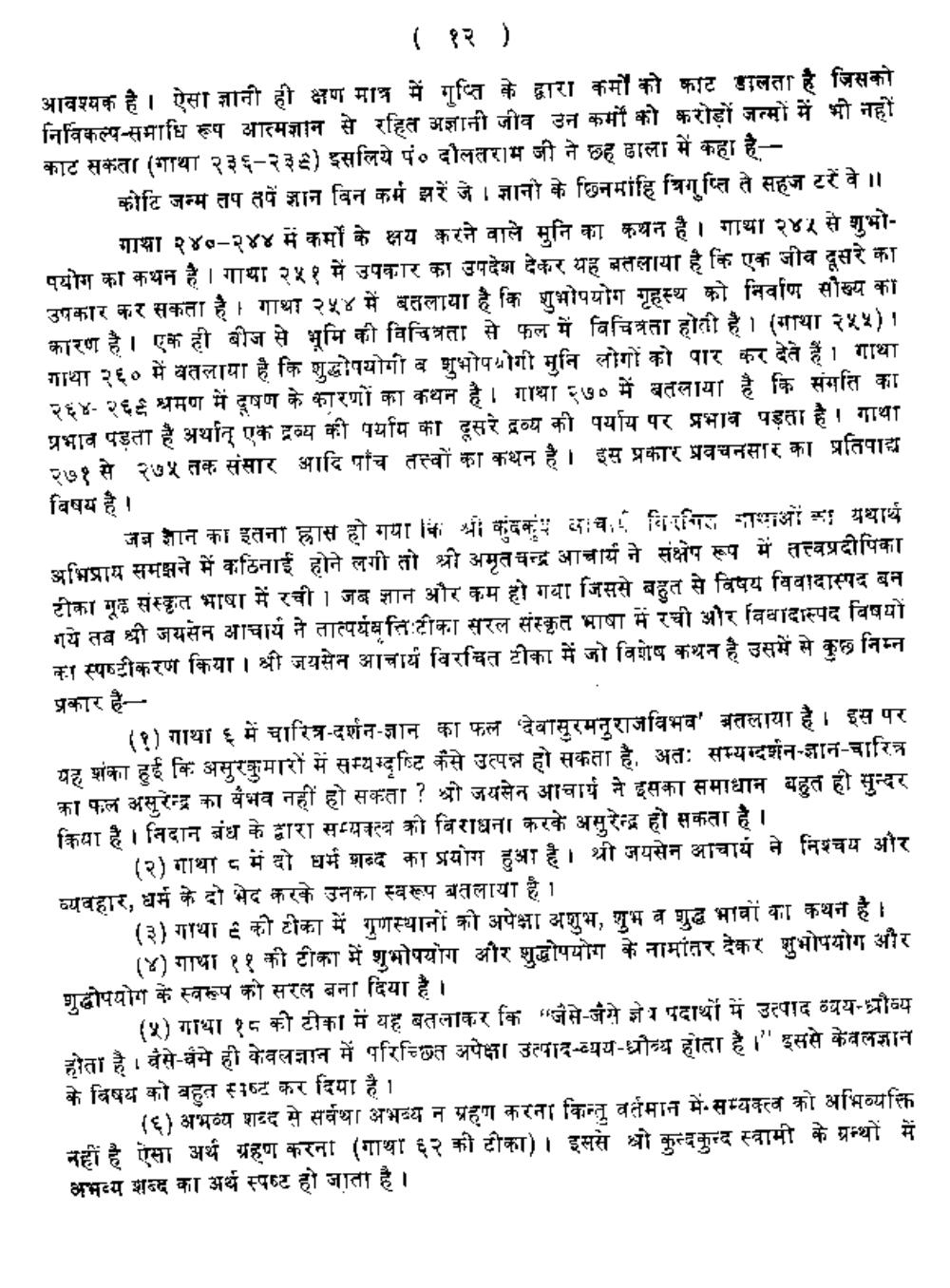________________
आवश्यक है। ऐसा ज्ञानी ही क्षण मात्र में गुप्ति के द्वारा कर्मों को काट डालता है जिसको निर्विकल्प-समाधि रूप आत्मज्ञान से रहित अज्ञानी जीव उन कर्मों को करोड़ों जन्मों में भी नहीं काट सकता (गाथा २३६-२३६) इसलिये पं० दौलतराम जी ने छह ढाला में कहा है
कोटि जन्म तप तपें ज्ञान विन कर्म झरे जे । ज्ञानी के छिनमांहि त्रिगुप्ति ते सहज टरें वे ॥
गाथा २४०-२४४ में कर्मों के क्षय करने वाले मुनि का कथन है। गाथा २४५ से शुभोपयोग का कथन है । गाथा २५१ में उपकार का उपदेश देकर यह बतलाया है कि एक जीव दूसरे का उपकार कर सकता है। गाथा २५४ में बतलाया है कि शुभोपयोग गृहस्थ को निर्वाण सौख्य का कारण है। एक ही बीज से भूमि की विचित्रता से फल में विचित्रता होती है। (गाथा २५५)। गाथा २६० में बतलाया है कि शुद्धोपयोगी व शुभोपयोगी मुनि लोगों को पार कर देते हैं। गाथा २६४- २६६ श्रमण में दुषण के कारणों का कथन है। गाथा २७० में बतलाया है कि संमति का प्रभाव पड़ता है अर्थात् एक द्रव्य की पर्याय का दूसरे द्रव्य की पर्याय पर प्रभाव पड़ता है। गाथा २७१ से २७५ तक संसार आदि पाँच तत्वों का कथन है। इस प्रकार प्रवचनसार का प्रतिपाद्य विषय है।
जब ज्ञान का इतना ह्रास हो गया कि श्री कुंदकर याच विरगिल मामाओं का यथार्थ अभिप्राय समझने में कठिनाई होने लगी तो श्री अमृत चन्द्र आचार्य ने संक्षेप रूप में तत्त्वप्रदीपिका टीका मूह संस्कृत भाषा में रची। जब ज्ञान और कम हो गया जिससे बहुत से विषय विवादास्पद बन गये तब श्री जयसेन आचार्य ने तात्पर्यवृत्तिःटीका सरल संस्कृत भाषा में रची और विवादास्पद विषयों का स्पष्टीकरण किया। श्री जयसेन आचार्य विरचित टीका में जो विशेष कथन है उसमें से कुछ निम्न प्रकार है
(१) गाथा ६ में चारित्र-दर्शन-ज्ञान का फल 'देवासुरमनुराजविभव' बतलाया है। इस पर यह शंका हुई कि असुरकुमारों में सम्यग्दृष्टि कैसे उत्पन्न हो सकता है, अत: सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र का फल असुरेन्द्र का वैभव नहीं हो सकता ? श्री जयसेन आचार्य ने इसका समाधान बहुत ही सुन्दर किया है। निदान बंध के द्वारा सम्यक्त्व को बिराधना करके असुरेन्द्र हो सकता है।
(२) गाथा ८ में दो धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। श्री जयसेन आचार्य ने निश्चय और व्यवहार, धर्म के दो भेद करके उनका स्वरूप बतलाया है।
(३) गाथा को टीका में गुणस्थानों की अपेक्षा अशुभ, शुभ व शुद्ध भावों का कथन है।
(४) गाथा ११ की टीका में शुभोपयोग और शुद्धोपयोग के नामांतर देकर शुभोपयोग और शुद्धोपयोग के स्वरूप को सरल बना दिया है।
(५) गाथा १८ को टीका में यह बतलाकर कि "जैसे-जैसे ज्ञेय पदार्थों में उत्पाद व्यय-प्रौव्य होता है। वैसे-वैसे ही केवलज्ञान में परिच्छित अपेक्षा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य होता है। इससे केवलज्ञान के विषय को बहुत सष्ट कर दिया है।
(६) अभव्य शब्द से सर्वथा अभब्य न ग्रहण करना किन्तु वर्तमान में सम्यक्त्व को अभिव्यक्ति नहीं है ऐसा अर्थ ग्रहण करना (गाथा ६२ को टीका)। इससे श्री कुन्दकुन्द स्वामी के ग्रन्थों में अभव्य शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है।