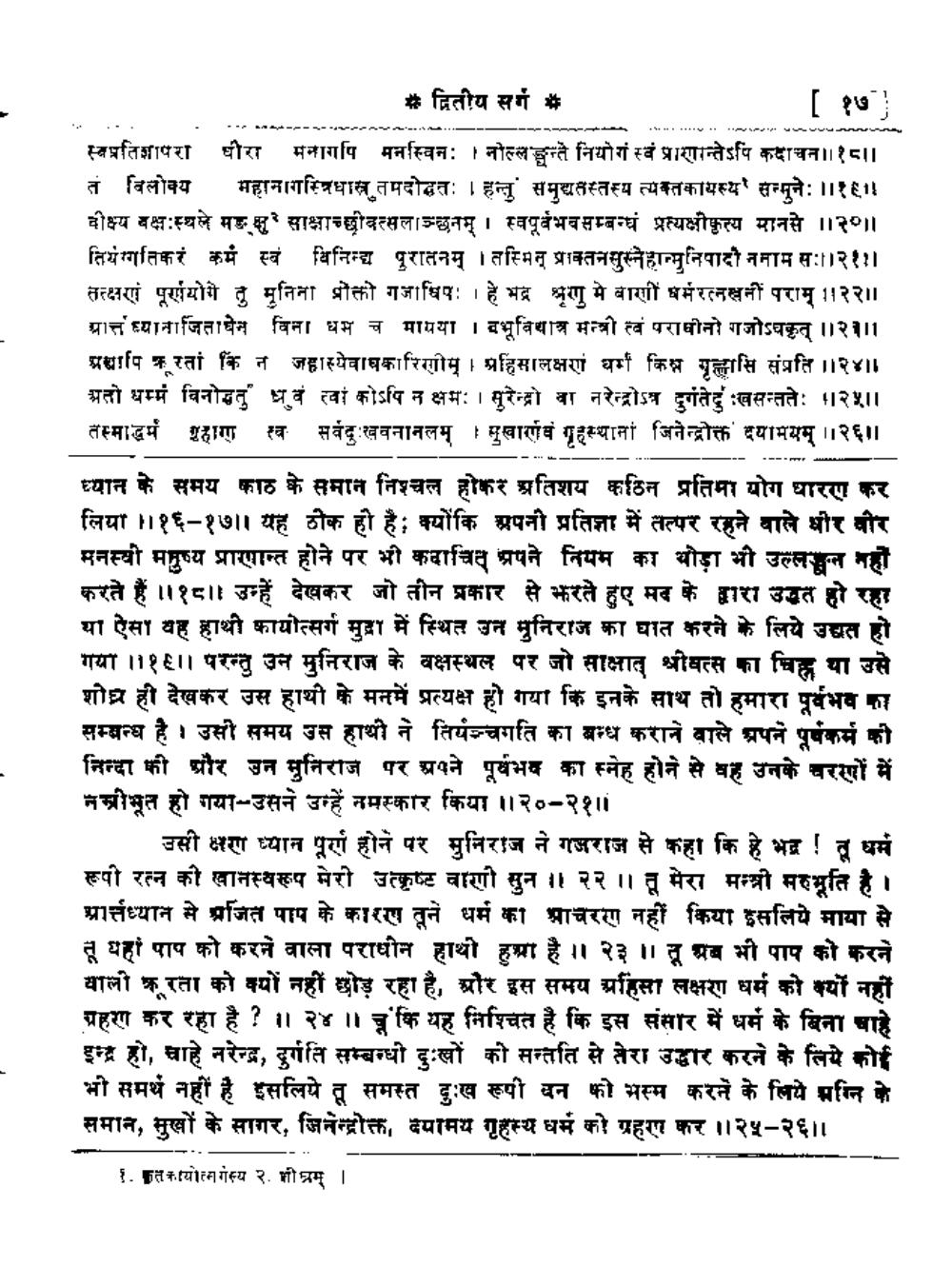________________
* द्वितीय सर्ग * स्वप्रतिज्ञापरा धोरा मनागपि मनस्विनः । नोल्लङ्घन्ते नियोगं स्वं प्राणान्तेऽपि कदाचन।।१८|| तं विलोक्य महानागस्त्रिधात्र तमदोदतः । हन्तुं समुद्यतस्तस्य त्यक्तकायस्य सन्मुनेः ।।१६॥ वीक्ष्य वक्षःस्थले मा झु साक्षाच्छीवत्सलाञ्छनम् । स्वपूर्वभव सम्बन्धं प्रत्यक्षीफुल्य मानसे ॥२०॥ तिर्यग्गतिकरं कर्म स्वं विनिन्द्य पुरातनम् । तस्मिन् प्राक्तनसुस्नेहान्मुनिपादौ नमाम सः।।२१। तत्क्षणं पूर्ण योगे तु मुनिना प्रोक्तो गजाधिपः । हे भद्र श्रृणु मे बाणी धर्मरत्नखनी पराम् ।।२२॥ प्रात्त ध्यानाजिताधेन विना धम च मायया । बभूविथात्र मन्त्री त्वं पराधीनो गजोऽवकृत् ।।२।। प्रचापि ऋ रतां किं न जहास्येवाघकारिणीम् । अहिसालक्षणं धर्म किन्न गृह्णासि संप्रति ॥२४॥ अतो धम्मं विनोद्ध ध्रुवं त्वां कोऽपि न क्षमः । सुरेन्द्रो वा नरेन्द्रोऽत्र दुर्गतेद् खसन्ततेः ।।२।। तस्माद्धर्म यहागा स्वः सर्वदुःखवनानलम् । मुखार्गवं गृहस्थानां जिनेन्द्रोक्त दयामयम् ।।२६।। ध्यान के समय काठ के समान निश्चल होकर अतिशय कठिन प्रतिमा योग धारण कर लिया ।।१६-१७॥ यह ठोक ही है। क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा में तत्पर रहने वाले धीर वीर मनस्वी मनुष्य प्राणान्त होने पर भी कदाचित् अपने नियम का थोड़ा भी उल्लखन नहीं करते हैं ॥१८॥ उन्हें देखकर जो तीन प्रकार से करते हुए मद के द्वारा उक्त हो रहा या ऐसा वह हाथी कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित उन मुनिराज का घात करने के लिये उद्यत हो गया ।।१६।। परन्तु उन मुनिराज के वक्षस्थल पर जो साक्षात् श्रीवत्स का बिल था उसे शोघ्र ही देखकर उस हाथी के मनमें प्रत्यक्ष हो गया कि इनके साथ तो हमारा पूर्वभव का सम्बन्ध है । उसी समय उस हाथी ने तियंञ्चगति का बन्ध कराने वाले अपने पूर्षकर्म की निन्दा की और उन मुनिराज पर अपने पूर्वभव का स्नेह होने से वह उनके चरणों में नम्रीभूत हो गया-उसने उन्हें नमस्कार किया ॥२०-२१॥
उसी क्षण ध्यान पूर्ण होने पर मुनिराज ने गजराज से कहा कि हे भद्र ! तू धर्म रूपी रत्न को खानस्वरूप मेरी उत्कृष्ट वाणी सुन ।। २२ ।। तू मेरा मन्त्री मरुभूति है। प्रार्तध्यान से अजित पाप के कारण तूने धर्म का आचरण नहीं किया इसलिये माया से तू यहां पाप को करने वाला पराधीन हाथी हुया है ॥ २३ ।। तू अब भी पाप को करने वाली करता को क्यों नहीं छोड़ रहा है, और इस समय अहिसा लक्षरण धर्म को क्यों नहीं ग्रहण कर रहा है ? ॥ २४ ॥ कि यह निश्चित है कि इस संसार में धर्म के बिना बाहे इन्द्र हो, चाहे नरेन्द्र, दुर्गति सम्बन्धी दुःखों को सन्तति से तेरा उद्धार करने के लिये कोई भी समर्थ नहीं है इसलिये तू समस्त दुःख रूपी बन को भस्म करने के लिये अग्नि के समान, सुखों के सागर, जिनेन्द्रोक्त, दयामय गृहस्थ धर्म को ग्रहण कर ॥२५-२६।।
१. कतकायोत्मगंस्य २. शीघ्रम् ।