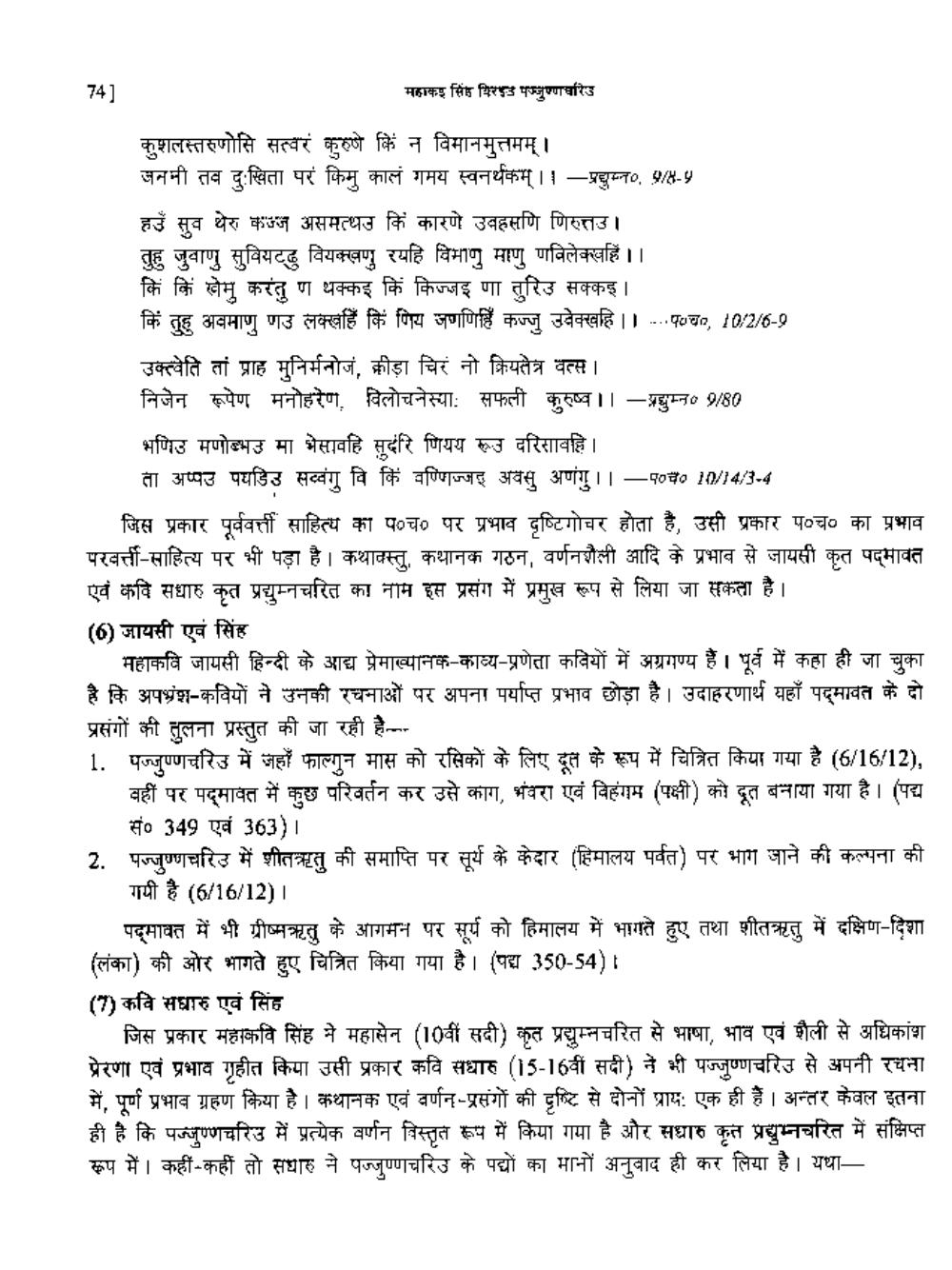________________
74]
महाकश सिंह विरइड पम्जुण्णरित
कुशलस्तरुणोसि सत्वरं कुरुणे किं न विमानमुत्तमम् । जननी तब दुःखिता परं किमु कालं गमय स्वनर्थकम् ।। – प्रद्युम्न०, 9/8-9 हउँ सुव थेर कज्ज असमत्थउ किं कारणे उवहसणि णिरुत्तउ। तुहु जुवाणु सुवियर्ड्स वियक्खणु रयहि विमाणु माणु णविलेक्खहिं ।। किं किं खेमु करंतु ण थक्कइ किं किज्जइ णा तुरिउ सक्कइ। किं तुहु अवमाणु णउ लक्खहिँ किं णिय जणणिहिँ कज्जु उवेक्खहि ।। ...प०च०, 10/2/6-9 उक्त्वेति तां प्राह मुनिर्मनोज, क्रीड़ा चिरं नो क्रियतेत्र वत्स । निजेन रूपेण मनोहरेण, विलोचनेस्याः सफली कुरुष्व।। – प्रद्युम्न० 9/80 भणिउ मणोड्भउ मा भेसावहि सुदंरि णियय रूज दरिसावहि ।
ता अप्पउ पयडिउ सव्वंगु वि किं वणिज्जद् अवसु अणंगु।। –प०० 10/14/3-4 जिस प्रकार पूर्ववर्ती साहित्य का प०च० पर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार प०च० का प्रभाव परवर्ती-साहित्य पर भी पड़ा है। कथावस्तु, कथानक गठन, वर्णनशैली आदि के प्रभाव से जायसी कृत पद्मावत एवं कवि सधारु कृत प्रद्युम्नचरित का नाम इस प्रसंग में प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। (6) जायसी एवं सिंह
महाकवि जायसी हिन्दी के आद्य प्रेमाख्यानक-काव्य-प्रणेता कवियों में अग्रगण्य है। पूर्व में कहा ही जा चुका है कि अपभ्रंश-कवियों ने उनकी रचनाओं पर अपना पर्याप्त प्रभाव छोड़ा है। उदाहरणार्थ यहाँ पद्मावत के दो प्रसंगों की तुलना प्रस्तुत की जा रही है.... 1. पन्जुण्णचरिउ में जहाँ फाल्गुन मास को रसिकों के लिए दूत के रूप में चित्रित किया गया है (6/16/12),
वहीं पर पद्मावत में कुछ परिवर्तन कर उसे काग, भंवरा एवं विहंगम (पक्षी) को दूत बनाया गया है। (पद्य
सं० 349 एवं 363)। 2. पन्जुण्णचरिउ में शीतऋतु की समाप्ति पर सूर्य के केदार (हिमालय पर्वत) पर भाग जाने की कल्पना की
गयी है (6/16/12)। पद्मावत में भी ग्रीष्मऋतु के आगमन पर सूर्य को हिमालय में भागते हुए तथा शीतऋतु में दक्षिण-दिशा (लंका) की ओर भागते हुए चित्रित किया गया है। (पद्म 350-54)। (7) कवि सधारु एवं सिंह
जिस प्रकार महाकवि सिंह ने महासेन (10वीं सदी) कृत प्रद्युम्नचरित से भाषा, भाव एवं शैली से अधिकांश प्रेरणा एवं प्रभाव ग्रहीत किया उसी प्रकार कवि सधारु (15-16वीं सदी) ने भी पज्जुण्णचरिउ से अपनी रचना में, पूर्ण प्रभाव ग्रहण किया है। कथानक एवं वर्णन-प्रसंगों की दृष्टि से दोनों प्राय: एक ही हैं । अन्तर केवल इतना ही है कि पज्जुण्णचरिउ में प्रत्येक वर्णन विस्तृत रूप में किया गया है और सधारु कृत प्रद्युम्नचरित में संक्षिप्त रूप में। कहीं-कहीं तो सधारु ने पन्जुण्णचरिउ के पद्यों का मानों अनुवाद ही कर लिया है। यथा—