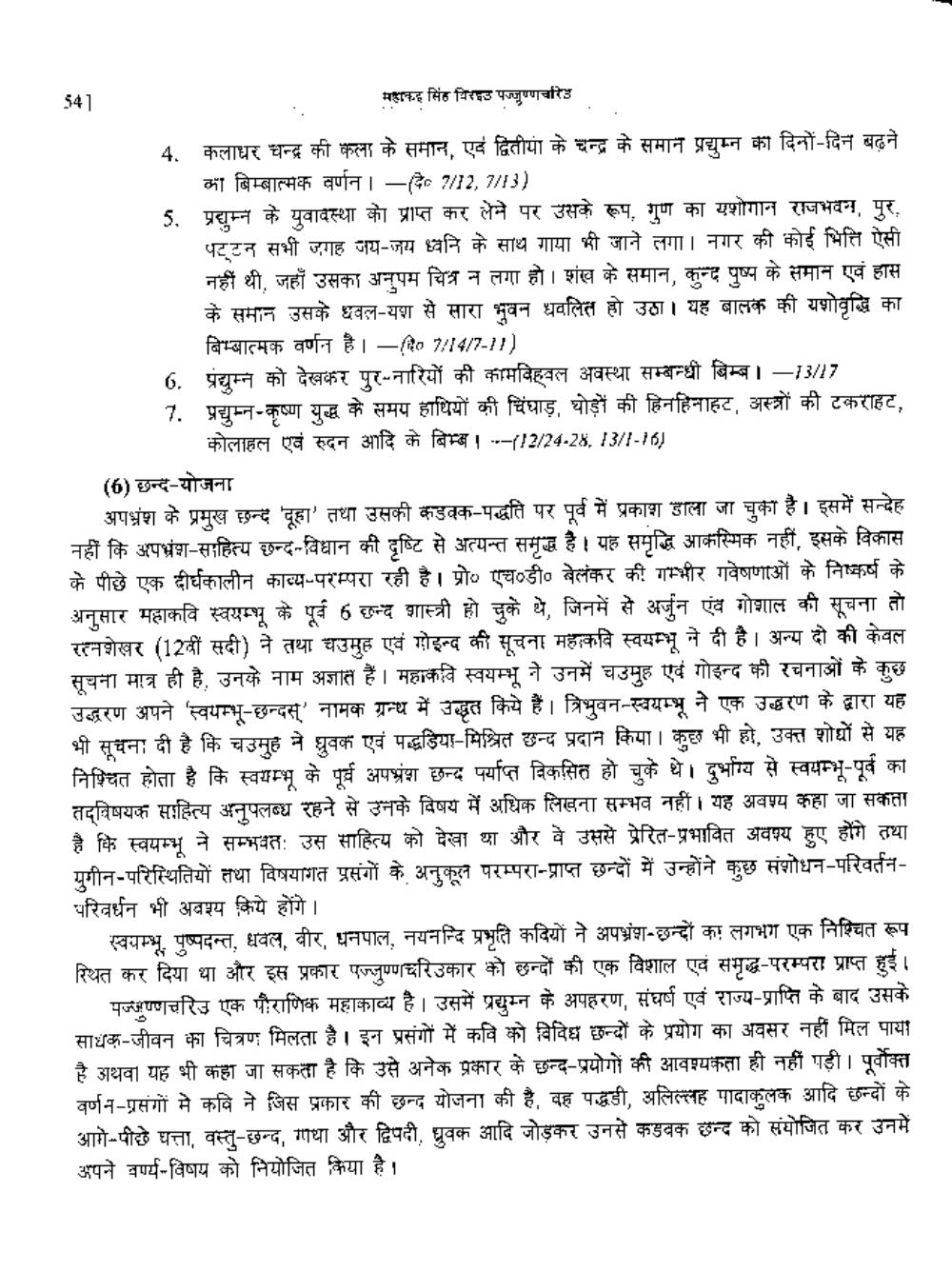________________
54]
महाकह सिंह विराउ पज्जुण्ण रेड
4. कलाधर चन्द्र की कला के समान, एवं द्वितीया के चन्द्र के समान प्रद्युम्न का दिनों-दिन बढ़ने
___ का बिम्बात्मक वर्णन। -(दै० 7/12, 7/13) 5, प्रद्युम्न के युवावस्था को प्राप्त कर लेने पर उसके रूप, गुण का यशोगान राजभवन, पुर,
पट्टन सभी जगह जय-जय ध्वनि के साथ गाया भी जाने लगा। नगर की कोई भित्ति ऐसी नहीं थी, जहाँ उसका अनुपम चित्र न लगा हो। शंख के समान, कुन्द पुष्प के समान एवं हास के समान उसके धवल-यश से सारा भुवन धवलित हो उठा। यह बालक की यशोवृद्धि का
बिम्बात्मक वर्णन है। -/07/14/7-11) 6. प्रद्युम्न को देखकर पुर-नारियों की कामविहबल अवस्था सम्बन्धी बिम्ब। -13/17 7. प्रद्युम्न-कृष्ण युद्ध के समय हाथियों की चिंघाड़, थोड़ों की हिनहिनाहट, अस्त्रों की टकराहट,
कोलाहल एवं रुदन आदि के बिम्ब । ---112/24.28. 13/1-16) (6) छन्द-योजना
अपभ्रंश के प्रमुख छन्द 'दूहा' तथा उसकी कडवक-पद्धति पर पूर्व में प्रकाश डाला जा चुका है। इसमें सन्देह नहीं कि अपभ्रंश-साहित्य छन्द-विधान की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध है। यह समृद्धि आकस्मिक नहीं, इसके विकास के पीछे एक दीर्घकालीन काव्य-परम्परा रही है। प्रो० एच०डी० बेलकर की गम्भीर गवेषणाओं के निष्कर्ष के अनुसार महाकवि स्वयम्भू के पूर्व 6 कुन्द शास्त्री हो चुके थे, जिनमें से अर्जुन एवं गोशाल की सूचना तो रत्नशेखर (12वीं सदी) ने तथा चउमुह एवं गोइन्द की सूचना महाकवि स्वयम्भू ने दी है। अन्य दो की केवल सूचना मात्र ही है, उनके नाम अज्ञात हैं। महाकवि स्वयम्भू ने उनमें चउमुह एवं गोइन्द की रचनाओं के कुछ उद्धरण अपने 'स्वयम्भू-छन्दस्' नामक ग्रन्थ में उद्धृत किये हैं। त्रिभुवन-स्वयम्भू ने एक उद्धरण के द्वारा यह भी सूचना दी है कि चउमुह ने युवक एवं पद्धडिया-मिश्रित छन्द प्रदान किया। कुछ भी हो, उक्त शोधों से यह निश्चित होता है कि स्वयम्भू के पूर्व अपभ्रंश छन्द पर्याप्त विकसित हो चुके थे। दुर्भाग्य से स्वयम्भू-पूर्व का तद्विषयक साहित्य अनुपलब्ध रहने से उनके विषय में अधिक लिखना सम्भव नहीं। यह अवश्य कहा जा सकता है कि स्वयम्भू ने सम्भवतः उस साहित्य को देखा था और वे उससे प्रेरित-प्रभावित अवश्य हुए होंगे तथा युगीन-परिस्थितियों तथा विषयागत प्रसंगों के अनुकूल परम्परा-प्राप्त छन्दों में उन्होंने कुछ संशोधन-परिवर्तनपरिवर्धन भी अवश्य किये होंगे।
स्वयम्भू, पुष्पदन्त, धवल, वीर, धनपाल, नयनन्दि प्रभृति कवियों ने अपभ्रंश-छन्दों का लगभग एक निश्चित रूप स्थित कर दिया था और इस प्रकार पज्जुण्णचरिउकार को छन्दों की एक विशाल एवं समृद्ध-परम्परा प्राप्त हुई।
पज्जपणचरिउ एक पौराणिक महाकाव्य है। उसमें प्रद्युम्न के अपहरण, संघर्ष एवं राज्य-प्राप्ति के बाद उसके साधक-जीवन का चित्रण मिलता है। इन प्रसंगों में कवि को विविध छन्दों के प्रयोग का अवसर नहीं मिल पाया है अथवा यह भी कहा जा सकता है कि उसे अनेक प्रकार के छन्द-प्रयोगों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पूर्वोक्त वर्णन-प्रसंगों मे कवि ने जिस प्रकार की छन्द योजना की है, वह पद्धडी, अलिल्लह पादाकुलक आदि छन्दों के आगे-पीछे घत्ता, वस्तु-छन्द, गणथा और द्विपदी, ध्रुवक आदि जोड़कर उनसे कडवक छन्द को संयोजित कर उनमें अपने वर्ण्य-विषय को नियोजित किया है।